(भाग-एक)
श्रीकृष्णेतिहासम् अर्थात श्रीकृष्ण का इतिहास प्रस्तुत करने वाला एक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित ग्रन्थ है।
-भागवत धर्म के संस्थापक भगवान श्रीकृष्ण एक अद्वितीय व अद्भुत महामानव भी थे जिनके चरित्र की समग्रता भूतकाल के गर्भ में समाहित है। आध्यात्मिक व पारलौकिक दृष्टिकोण से भारतीय माइथोलॉजी(पुराणशास्त्रों) में विष्णु के तीन स्वरूप मान्य हैं। इस विष्णु-त्रय में स्वयं श्रीकृष्ण स्वराट- विष्णु के रूप में सर्वोच्च भगवान बनकर प्रतिष्ठित हैं। यह उनका सर्वोच्च और समग्र रूप है। वह सुरक्षा, करुणा, कोमलता और प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं; कृष्ण का व्यक्तित्व बहु-आयामी है। वे सभी भारतीय धर्मों विशेषत: जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, आदि में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय व इष्ट हैं।
कृष्ण का जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष भारतीयों द्वारा चन्द्र-सौर भारतीय पाञ्चाङ्ग के अनुसार भाद्रमास कृष्णपक्षाष्टमी को मनाया जाता है। जो ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार अगस्त के अन्त या सितम्बर के प्रारम्भ में आता है। परन्तु जिन शास्त्रीय साक्ष्यों के आधार पर यह जन्म दिन अथवा जयन्ती का पर्व मनाया जाता है। उन्हीं साक्ष्यों में परस्पर इस तथ्य पर भेद है।
कुछ पुराण भाद्रपद मास की अपेक्षा श्रवणमास में भी कृष्ण जन्म का वर्णन करते हैं। इस विषय पर आगे यथाक्रम विस्तृत विश्लेषण किया जाऐगा।
कृष्ण का नाम और उनके पर्यायवाची शब्द पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के साहित्य और ग्रन्थों में भी पाए जाते हैं।
कृष्णवाद जैसी कुछ उप-परम्पराओं में, कृष्ण को स्वयं सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। ये उपपरम्पराऐं मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन के सन्दर्भ में विशेषत: उभर कर आयीं हैं।
कृष्ण-सम्बन्धित साहित्य ने भारत देश में भरतनाट्यम , कथकली , कुचिपुड़ी , ओडिसी और मणिपुरी नृत्य जैसी कई प्रदर्शन कलाओं को भी प्रेरित किया है।
वह श्रीकृष्ण सर्व-भारतीयों के आराध्य हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर विशेष रूप से पूजनीय व सांस्कृतिक चेतना भी हैं, जैसे उत्तर-प्रदेश में मथुरा- वृन्दावन , गुजरात में द्वारका और
जूनागढ़ ; तथा ओडिशा में जगन्नाथ , पश्चिम बंगाल के मायापुर में कृष्ण को मुख्य रूप से श्रीकृष्ण के रूप में ही जाना जाते है,
- यहीं पश्चिमीय बंगाल के मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु: का जन्म हुआ जो कृष्ण मत के प्रचारक व सन्त थे। मायापुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है, जिनका जन्म ईस्वी सन् (1486) में हुआ था। जिनका गौड़ीय वैष्णववाद के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व है, उनके अनुयायी उन्हें राधा के रूप में कृष्ण के एक विशेष अवतार मानते हैं।
महाराष्ट्र के पण्ढरपुर में विठोबा(विट्ठल) के रूप में श्रीकृष्ण की ही पूजा होती है।
- पहचान:भगवान विठोबा को विट्ठल और पाण्डुरङ्ग के नाम से भी जाना जाता है.
- स्वरूप:उन्हें आमतौर पर हिंदू देवता विष्णु या उनके अवतार कृष्ण का एक रूप माना जाता है.
- पूजा स्थल:उनकी पूजा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में की जाती है.
- प्रसिद्ध रूप:उन्हें अक्सर अपनी कमर पर हाथ रखे, ईंट पर खड़े एक काले युवा लड़के के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके साथ उनकी पत्नी रुक्मिणी खड़ी होती हैं.
विठ्ठल, विठोबा अर्थात पाण्डुरंग एक हिन्दू देवता हैं जिनकी पूजा मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, तथा आन्ध्र प्रदेश में होती हैं। उन्हें आम तौर पर भगवान विष्णु अथवा उनके अवतार, कृष्ण की अभिव्यक्ति माना जाता हैं। विठ्ठल अक्सर एक सावले युवा लड़के के रूप में चित्रित किए जाते है, एक ईंट पर खडे और दोनो हाथ कमर पर रखे; कभी-कभी उनकी पत्नी रखुमाई (ऋक्षमणी)- रुक्मिणी भी साथ होती हैं। विट्ठलस्वामी मन्दिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यह मन्दिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। हम्पी के समस्त मन्दिरों में यह सबसे ऊँचा है। माना जाता है कि राजा कृष्णदेव राय ने 'हज़ार राम' एवं 'विट्ठलस्वामी' नामक मंदिरों का निर्माण करवाया था।
विठोबा
- विट + ठल: यह सबसे आम व्याख्या है. कहा जाता है कि भगवान विष्णु (जिन्हें विठोबा भी कहते हैं) अपने भक्त पुंडलिक के माता-पिता की सेवा को देखते हुए एक ईंट पर खड़े हो गए थे. मराठी में ईंट को 'विट' कहते हैं और 'ठल' का अर्थ 'खड़े होना' है, जिससे यह नाम विट्ठल पड़ा.
- विष्णु का अपभ्रंश: कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मूल शब्द 'विष्णु' का ही विकृत रूप है. डॉ. आर. जी. भंडारकर के अनुसार, कन्नड़ में विष्णु शब्द का अपभ्रंश होकर 'बिट्टी' हुआ और इसी से 'विट्ठल' शब्द बना है.
- विट + स्थान: एक अन्य व्याख्या यह भी है कि यह शब्द संस्कृत के 'विष्णु' और 'थल' (स्थान या निवास) से बना है, जिसका अर्थ है "विष्णु का स्थान".
- भगवान विष्णु रुक्मिणी से नाराज़ होकर दिंडीवन पहुंचे, जहां उन्हें भक्त पुंडलिक मिले.
- पुंडलिक अपने माता-पिता की सेवा में लीन थे.
- पुंडलिक ने भगवान से ईंट पर खड़े होने के लिए कहा ताकि वे अपने माता-पिता की सेवा में कोई चूक न करें.
- भगवान विष्णु उनकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उसी ईंट पर खड़े हो गए, जिससे उन्हें 'विट्ठल' नाम मिला.
राजस्थान के नाथद्वारा में कृष्ण को मुख्य रूप से श्रीनाथजी के नाम से जाना जाता है. श्रीनाथजी, भगवान कृष्ण का सात वर्षीय बालक रूप है, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था. इस मंदिर को "श्रीनाथजी की हवेली" भी कहा जाता है, जो भगवान के निवास का प्रतीक है।
"श्रीकृष्ण के श्रीनाथ रूप की पुन: ठाकुर रूप और मन्दिर की हवेली रूप में प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक विवरण-
पुष्टिमार्ग के अनुयायी बताते हैं कि श्रीकृष्ण के इस स्वरूप का हाथ और चेहरा पहले गोवर्धन पहाड़ी से उभरा था और उसके बाद माधवेंद्र पुरी के आध्यात्मिक नेतृत्व में स्थानीय निवासियों (व्रजवासियों) ने गोपाल (कृष्ण) देवता की पूजा शुरू की। इन्हीं गोपाल देवता को बाद में श्रीनाथजी कहा गया। इस प्रकार, माधवेन्द्र पुरी को गोवर्धन के पास गोपाल देवता की खोज के लिए मान्यता दी जाती है, जिसे बाद में पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य द्वारा श्रीनाथजी के रूप में अनुकूलित और पूजित किया गया।
प्रारम्भ में, माधवेंद्र पुरी ने देवता के ऊपर उठे हुए हाथ और बाद में, चेहरे की पूजा की।
पुष्टिमार्ग साहित्य के अनुसार, श्रीनाथजी ने श्री वल्लभाचार्य को भारतीय विक्रम संवत 1549 में दर्शन दिए और वल्लभाचार्य को निर्देश दिया कि वे गोवर्धन पर्वत पर पूजा प्रारम्भ करें। वल्लभाचार्य ने उन देवता की पूजा के लिए व्यवस्था की, और इस परम्परा को उनके पुत्र विठ्ठलनाथजी ने आगे बढ़ाया।
श्री नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी की यह मूर्ति पहले आगरा और ग्वालियर में थी जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया तो वहाँ के महंत इस दिव्य मूर्ति को लेकर वृंदावन से वाया जयपुर, मारवाड़ पहुंचे। तत्कालीन महाराजा ने श्रीनाथ जी को चौपासनी में रुकवाया।
चौपासनी राजस्थान के जोधपुर शहर के पास एक क्षेत्र है, यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, जहाँ अतीत में श्रीनाथजी की मूर्ति भी कुछ समय के लिए विराजमान थी।
फिर जब तत्कालीन महाराजा पाटोदी(बाड़मेर) ठाकुर ने श्रीनाथ जी की सुरक्षा की दृष्टि से बीड़ा उठाया और वे श्रीनाथ जी को पाटोदी ले पधारे।
छ: माह तक श्रीनाथ जी पाटोदी (बाड़मेर) राजस्थान में ही बिराजे। तभी ऌये पाटोदी के ठाकुर भी कहलाने लगे इस तरह श्रीनाथ जी का पाटोदी से बहुत गहरा सम्बन्ध है। जब बात लीक हो गई तो महंत जी ने मेवाड़ का रुख किया। कोठारिया के ठाकुर और महाराणा राजसिंह जी मेवाड़ में अपने प्राणों पर खेल कर श्रीनाथ जी को नाथद्वारा में स्थापित कर दिया।
माना जाता है कि प्रतिमा ले जाते हुए रथ, यात्रा करते समय मेवाड़ के सिहाड़ गांव में कीचड़ में फंस गया था, और इसलिए मूर्ति की स्थापना मेवाड़ के तत्कालीन राणा की अनुमति के साथ एक मंदिर में की गई थी। धार्मिक मिथकों के अनुसार, नाथद्वारा में मंदिर का निर्माण 17 वीं शताब्दी में श्रीनाथजी द्वारा स्वयं चिन्हित किए गए स्थान पर किया गया था।
मंदिर को लोकप्रिय रूप देने के लिए से श्रीनाथजी की हवेली (श्रीनाथजी का घर) भी कहा जाता है। और श्रीनाथ जी को तभी से ठाकुर जी कहने की शुरुआत हुई। क्योंकि श्रीनाथ द्वारा में एक नियमित गृहस्थी की तरह इनके रथ की आवाजाही होती है। इस लिए यह नाथद्वारा उनका घर या हवेली है।
ठाकुर शब्द तुर्कों और ईरानियों के साथ भारत आया । ठाकुर का अर्थ पगड़ीधारी, भूखण्डका मालिक जागीरदार है। ठाकुर जी सम्बोधन का प्रयोग वस्तुत : स्वामी भाव को व्यक्त करने के निमित्त है । न कि जन-जाति विशेष के लिए । कृष्ण को ठाकुर सम्बोधन का क्षेत्र अथवा केन्द्र नाथद्वारा राजस्थान प्रमुखत: है। मन्दिरों में कृष्ण की पूजा ठाकुर जी की पूजा ही कहलाती है। यहाँ तक कि उनका मन्दिर भी हवेली कहा जाता है। विदित हो कि हवेली (Mansion) और तक्वुर (ठक्कुर) दौनों शब्दों की पैदायश ईरानी, तुर्की और आरमेनियन भाषाओं से है।
कालान्तरण में भारतीय समाज में ये शब्द रूढ़ हो गये । पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के देशभर में स्थित अन्य मन्दिरों में भी भगवान श्रीकृष्ण को अब ठाकुर जी कहने का परम्परा है।
- बाल रूप:श्रीनाथजी भगवान कृष्ण के 7 वर्ष की अवस्था के रूप में पूजे जाते हैं.
- गोवर्धनधारी:वे गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण के विग्रह हैं, और उन्हें गिरिराज धरण भी कहा जाता है.
- मन्दिर का महत्व:यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ भक्त श्रीनाथजी की सेवा करते हैं.
,भारत के कर्नाटक राज्य के उडुपी शहर में कृष्ण बाल रूप प्रतिष्ठित हैं यहाँ कृष्ण मठ को 13वीं सदी में वैष्णव संत श्री माधवाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। वे द्वैतवेदान्त सम्प्रदाय के संस्थापक थे।, तमिलनाडु में पार्थसारथी और केरल के अरनमुला में भगवान कृष्ण का नाम पार्थसारथी है. इस मंदिर को अरनमुला पार्थसारथी मंदिर कहा जाता है, जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा अर्जुन के सारथी के रूप में की जाती है, क्योंकि महाभारत में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी. और केरल के गुरुवायूर में श्रीकृष्ण को बाल रूप में ही पूजा जाता है।
गुरुवायूर के भगवान/पिता) को गुरुवायुरप्पन के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, यह विष्णु का एक रूप है जिसे मुख्य रूप से केरल । वह गुरुवयूर मंदिरी के पीठासीन देवता हैं, जिनकी पूजा उनके बाल रूप में कृष्ण के रूप में की जाती है, जिन्हें गुरुवयूर उन्नीकन्नन (गुरुवयूर का शाब्दिक 'छोटा कृष्ण') भी कहा जाता है।
गुरुवायूरप्पन रूप में
गुरुवायूरप्पन भगवान विष्णु का एक रूप हैं, जिनकी पूजा कृष्ण के बाल रूप में की जाती है और वह केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर मन्दिर के पीठासीन देवता हैं. उन्हें "गुरुवायूर का छोटा कृष्ण" भी कहा जाता है. इस मूर्ति की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा राजा सुतपा और रानी पृश्नि को दिए गए कृष्ण की मूर्ति से हुई है, जिसे वायु की सहायता से केरल में स्थापित किया गया
- देवता:वह भगवान विष्णु का ही एक रूप हैं.
- रूप:उनकी पूजा कृष्ण के बाल रूप में की जाती है, जिन्हें गुरुवायूर उन्नीकन्नन (छोटा कृष्ण) भी कहते हैं.
- स्थान:वह गुरुवायूर मंदिर के मुख्य देवता हैं, जो केरल, भारत में स्थित है.
- मूर्ति:यह मूर्ति एक विशेष प्रकार के पत्थर 'कृष्ण शिला' से बनी है, जिसे अत्यधिक आध्यात्मिक माना जाता है.
- उत्पत्ति:ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने द्वारिका में अपनी मूर्ति को उद्धार के लिए वायु देवता की मदद से केरल भेजा था, और उसी स्थान पर गुरुवायूरप्पन की स्थापना हुई, इसलिए इस जगह का नाम गुरु-वायु-उर पड़ा.
गुरुवायूरप्पन नाम "गुरु" (शिक्षक), "वायु" (पवन देवता), और "उर" (स्थान) से बना है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति को वायु देवता ने केरल में स्थापित किया था.
******************************
1960 के दशक से, कृष्ण की पूजा पश्चिमी दुनिया और अफ्रीका तक भी फैल गई है।
जिसका मुख्य कारण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) का कृष्ण भक्ति अभियान है।
नाम और विशेषण-
"कृष्ण" नाम की उत्पत्ति वैदिक भाषा की धातु कृष्= हलचालने" से हुई है। जिसका अर्थ है- हल चलाना/ कृषि करना।
कृष्ण एक विशेषण है जो मुख्य रूप से उनके कृषक पृष्ठभूमि को इंगित करता है। कृष्ण शब्द के अन्य अर्थ भी विकसित हुए हैं जैसे "काला", या "गहरा नीला" आदि है। वैसे तो कृष्ण ने अपने बहुमुखी व्यक्तित्व से जनमानस को आकर्षित भी किया था। इसलिए उनका कृष्ण होना सार्थक है। कृषि कार्य और गोपालन करने से त्वचा का रंग काला (श्यामल) हो जाने के कारण ही बाद में कृष्ण शब्द का अर्थ काला हो गया। श्याम शब्द कृष्ण के कायिक रञ्जना को दर्शाता है। कई कारणों से किसान काले होते हैं, जिसमें प्रमुख कारण है धूप में अधिक समय बिताना (जो मेलेनिन नामक पिगमेंट( रञ्जक) का उत्पादन बढ़ाता है), वंशानुगत कारण, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हाइपरपिगमेंटेशन, हार्मोनल बदलाव, पोषक तत्वों की कमी (विशेषकर विटामिन बी12), और अस्वस्थ जीवनशैली के कारण भी त्वचा का रंग श्यामल हो जाता है। किसान प्राय: धूप-छाँव की परवाह न करके दिन-रात महनत करता हैं।।
- सूर्य की किरणें:जब त्वचा पर सूरज की अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें पड़ती हैं, तो त्वचा में मेलेनिन हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है। मेलेनिन त्वचा को रंग देने वाला वर्णक(पिगमेंट)
- है, और इसका ज़्यादा उत्पादन त्वचा को काला बनाता है।
- स्थान-विषुवत रेखा के आस- पास या गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की त्वचा ज़्यादा काली होती है क्योंकि वहां धूप की तीव्रता अधिक होती है, जिससे शरीर ज़्यादा मेलेनिन हार्मोन सर्जित करता है।
- अन्य कारण-
- कुछ लोगों की त्वचा वंशानुगत रूप से काली होती है, जो उनकी आनुवंशिकी का परिणाम होता है। ऐसा होने के मूल में भी जलवायु सम्बन्धी गुणों का आनुवांशिक गुण बनकर परम्परागत रूप से सम्प्रेषित होना ही है।
कृष्ण के भाई संकर्षण हैं जो हल के आविष्कारक तथा कृषिविद्या के जनक हैं। दोंनो भाई कृषक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित हैं। जो पहले पशुपालन करते थे वही बाद में कृषि के भी करने वाले हुए।
श्रीकृष्ण के अन्य नामों में विष्णु नाम भी है।विष्णु के नाम के रूप में , कृष्ण को विष्णु सहस्रनाम में (57) वें नाम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ।विष्णु सहस्रनाम मुख्य रूप से महाकाव्य महाभारत के अनुशासन पर्व से उत्पन्न है। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, बाणों की शय्या पर लेटे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को भगवान विष्णु के इन एक हजार नामों के बारे में बताया था, जो उनके गुणों और शक्तियों का वर्णन करते हैं। अनुशासन पर्व के 149वें अध्याय में मिलता है,

भीष्म उवाच:
इतिदं कीर्तनियास्य केशवस्य महात्मनः।
नामनाम सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम्॥१।
योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वर: ।
नारसिंहवपु: श्रीमान् केशव: पुरुषोत्तम: ॥१६॥
अग्राह्य: शाश्वत: कृष्णो लोहिताक्ष: प्रतर्दन: ।
प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ॥२०।
महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवास: सतां गति: ।
अनिरुद्ध: सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पति: ॥३३॥
मरीचिर्दमनो हंस: सुपर्णो भुजगोत्तम: ।
हिरण्यनाभ: सुतपा: पद्मनाभ: प्रजापति: ॥३४॥
वेधा: स्वाङ्गोऽजित: कृष्णो द्दढ: सङ्कर्षणोऽच्युत:।
वरुणो वारुणो वृक्ष: पुष्कराक्षो महामना: ॥७२॥
इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मन: ।
नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् ॥१२१॥
य इदं श्रृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् ।
नाशुभं प्राप्नुयात्किञ्चित्सोऽमुत्रेह च मानव: ॥१२२॥
- महाभारत के अलावा, विष्णु सहस्रनाम के अन्य संस्करण पद्म पुराण, स्कन्द पुराण और गरुड़ पुराण में भी पाए जाते हैं।
उनके कृष्ण अथवा श्याम नाम के आधार पर, कृष्ण को अक्सर मूर्तियों में काले या नीले रंग के रूप में चित्रित किया जाता है। कृष्ण को कई अन्य नामों, विशेषणों और उपाधियों से भी जाना जाता है जो उनके कई संघों और गुणों को दर्शाते हैं। सबसे आम नामों में मोहन="सम्मोहन रखने वाला" हैं; गोविन्द गोपेन्द्र = गोपों का स्वामी", ? और गोपाल "'गो' के रक्षक। "
कृष्ण को वासुदेव-कृष्ण , मुरलीधर या चक्रधर भी कहा जा सकता है। मानद उपाधि "श्री"का प्रयोग अक्सर कृष्ण के नाम से पहले किया जाता है। कृष्ण के अन्य नाम-
"अच्युत , दामोदर , गोपाल , गोपीनाथ , गोविंद , केशव , माधव , राधा रमण , वासुदेव , कन्नन आदि-
जन्म:–मथुरा , शूरसेन (वर्तमान उत्तर प्रदेश , भारत)
देहावसान:–भालका , सौराष्ट्र (वर्तमान वेरावल , गुजरात , भारत)
अभिभावक:- नन्द यशोदा व वसुदेव देवकी।
जाति - गोप (आभीर) रोहिणी और वासुदेव की अन्य पत्नियाँ (सौतेली माताएँ)
भाई-बहन बलराम (सौतेले भाई)सुभद्रा (सौतेले बहन)योगमाया एकानंशा (पालक-बहन)
कृष्ण की अन्य सन्तानें व पत्नी के नाम-
राधा-रुक्मणी-सत्यभामा अन्य 6 प्रमुख रानियाँ-16,000 - 16,100 कनिष्ठ रानियाँ प्रमुख सन्तानें-प्रद्युम्न"साम्ब,भानु और कई अन्य ।
"श्रीकृष्ण के जन्म की यथार्थ तिथि निर्णय क्या है ?
सनातन धर्म में श्रीकृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। इन पूर्ण विष्णु को ही स्वराट विष्णु कहते हैं। विष्णु के तीन भेदों में यह सर्वोच्च स्वरूप है। भगवान विष्णु श्रीकृष्ण के रूप में द्वापर युग में अवतार लेते हैं। और धर्म की संस्थापना के लिए दुष्टों का संहार करते हैं। आम तौर पर श्रीकृष्ण के अवतरण या जन्म की तिथि भाद्रपद के कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि की अर्द्ध-रात्रि को माना जाता है । लेकिन इसको लेकर भी पुराणों में मतभेद है। जिस पर एक विश्लेषण यहाँ अपेक्षित है।
क्या श्रीकृष्ण का जन्म भादों के महीने में हुआ था ?
श्रीकृष्ण के चरित्र को लेकर सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रन्थों में महाभारत, देवीभागवत महापुराण और हरिवंश पुराण को माना जाता है । हरिवंश पुराण को महाभारत का अवशिष्ट ( बचा हुआ) भाग भी माना जाता है जिसमें भगवान विष्णु के सभी अवतारों विशेष कर भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और कार्यों का विस्तार से वर्णन है।
महाभारत में श्रीकृष्ण के जन्म की तिथि और उनके बाल्यकाल का कोई विवरण नहीं मिलता है श्रीमद्भावगत महापुराण के दशम स्कन्ध में अवश्य भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का विवरण मिलता है लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भगवान श्रीकृष्ण का जन्म किस महीने में हुआ था ,इसको लेकर श्रीमद्भभावगत महापुराण भी मौन है।
हरिवंश पुराण में भी श्रीकृष्ण के जन्म की कथा मिलती है।
- तिथि:भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि
- समय:मध्यरात्रि
- नक्षत्र:रोहिणी नक्षत्र
- अन्य शुभ योग: हरिवंशपुराण के अनुसार, उस समय अभिजित् नक्षत्र, जयन्ती नामक रात्रि और विजय नामक मुहूर्त था.
यह विवरण जन्माष्टमी के पर्व से मेल खाता है, जिसे इसी तिथि और समय के अनुसार मनाया जाता है. कृष्ण का जन्म एक शुभ लग्न में हुआ था, जिसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि थी और सभी ग्रह अपनी गति क्रम से ग्यारहवें स्थान में स्थित थे, जैसा कि हरिवंशपुराण में वर्णित है.
अभिजिन्नाम नक्षत्रं जयन्ती नाम शर्वरी ।
मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दनः ।१७।।
हरिवंशपुराण (विष्णुपर्व)अध्यायः(४)
लेकिन यहाँ भी ये नहीं बताया गया है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म किस महीने में हुआ था श्रीमद्भावत महापुराण में केवल ये बताया गया है कि श्रीकृष्ण का जन्म रात्रि के पहर में शुभ नक्षत्र था और ग्रह और तारे सभी शुभता के साथ स्थित थे। हरिवंश पुराण में भी यही कहा गया है कि श्रीकृष्ण का जन्म एक शुभ रात्रि में एक विशेष मूहूर्त में हुआ था । लेकिन इन दोनों ही ग्रन्थो में श्रीकृष्ण के जन्म का महीना नहीं बताया गया है ।
क्या श्रीकृष्ण का जन्म सावन के महीने में हुआ था ?
यद्यपि महाभारत श्रीकृष्ण के जन्म की घटना का कोई विवरण नही देता , श्रीमद्भावतम और महाभारत का खिल (परिशिष्ट) भाग हरिवंश पुराण में भी श्रीकृष्ण के जन्म के महीने का कोई श्लोक या विवरण नहीं मिलता , फिर भी आज के भारतीय भादों के महीने में ही श्रीकृष्ण का जन्म मनाते हैं।
लेकिन अगर कुछ और ग्रन्थो के श्लोकों को पढ़ा जाए तो उनमें ये कहा गया है कि सावन के महीने में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था।
श्रावणे मासि पक्षे च कृष्णेऽष्टम्यां प्रजापतेः।
नक्षत्रे वसुदेवस्य देवक्यां भगवान् हरिः१६/६५॥
सर्वलोकहितार्थाय भूमेर्भारावतारणम्।
कर्तुमाविरभूद्भूमौ मध्यरात्रे महामते।।१६/६६॥
(विश्वामित्रसंहिता, अध्याय – १६, श्लोक – ६५-६६)
पुराणों में श्रीकृष्ण के जन्म को लेकर मतभेद-
विश्वामित्र संहिता का ये श्लोक ये कहता है कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जब प्रजापति (ब्रह्मा) का नक्षत्र था, तब आधी रात को सभी लोकों का कल्याण करने के लिए और पृथ्वी का भार कम करने के लिए वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ ।६५-६६।
द्वापरे समनुप्राप्ते विरोधिवत्सरे शिवे।
श्रावणे चाष्टमी शुक्ला बुधरोहिणीसंयुता॥६३।
वज्रयोगे मध्यरात्रौ पूर्णः कृष्णो हरिः स्वयम्।
कंसस्य च वधार्थाय अर्जुनस्य हिताय च॥६४
(शक्तिसंगम महातन्त्र राज, छिन्नमस्ताखण्ड, पटल – 06, श्लोक – 63-64)
शक्ति संगम महातंत्र का ये श्लोक कहता है कि द्वापरयुग के आने पर विरोधी नामक सम्वत्सर में जब सावन के महीने के शुक्लपक्ष की अष्टमी की तिथि थी और वो दिन बुधवार का था और उस वक्त आधी रात को रोहिणी नक्षत्र का शुभ समय था उस वक्त वज्रयोग जैसे अति शुभ योग में आधी रात को ही स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु अवतार लेकर कंस का वध करने और अर्जुन का हित करने के लिए श्रीकृष्ण रुप में पधारे।
पद्मपुराण उत्तरखण्ड जो सभी पुराणों में प्राचीन व बृहद माना जाता है , उसमें में सावन के महीने में ही भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के बारे में श्लोक मिलते हैं। देखें निम्नलिखित श्लोकों को-
( हरिश्चन्द्रोवाच )
केनैव च विधानेन कस्मिनमासे च सा तिथि: ।कर्त्तव्या तन्ममाचक्ष्व अनुग्राह्योऽस्मि ते यदि।३१।
(सनत्कुमार- उवाच)
शृणुष्वावहितो राजनकथ्यमानं मया तव। श्रावण सत्य तु मासस्य कृष्णाष्टम्यां नराधिप।३२।
रोहिणी यदि लभ्येत जयन्ती नाम सा तिथि।भूयोभूयो महाराज भवेज्जन्मनि कीरणम्।३३।
सन्दर्भ- पद्मपुराण (उत्तरखण्डः)अध्यायः (३१)
पद्मपुराण उत्तरखण्ड के उपर्युक्त श्लोकों के अनुसार सावन के महीने की अष्टमी तिथि को रात्रि के समय और आकाश में रोहिणी नक्षत्र विराजमान था, उस पुण्य वेला में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था।
परन्तु पद्मपुराण ब्रह्मखण्ड अध्याय (१३) में वर्णन है कि
भाद्रेमास्यसिताष्टम्यां यस्यां जातो जनार्द्दनः ।
तदहं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने ।९।
पद्मपुराणम्/खण्डः ४ (ब्रह्मखण्डःअध्यायः (१३)
भगवान श्रीकृष्ण का जन्म किस तिथि को हुआ था ?
श्रीमद्भागवत महापुराण और हरिवंश पुराण भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की तिथि के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहते । श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से संबंधित दो श्लोक महत्वपूर्ण हैं –
अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः।
यर्हि एव अजनजन्मर्क्षं शान्तर्क्ष-ग्रहतारकम।।
(श्रीमद्भागवत पुराण, स्कन्ध (10) अध्याय (3), श्लोक (1)
इस श्लोक में शुकदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि – “अब समस्त शुभ गुणों से युक्त शुभ समय आया जब उसका जन्म होने वाला था जो अजन्मा (श्रीकृष्ण) है । इस काल में सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शान्त और सौम्य हो रहे थे।“
इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण का जब जन्म होता है तो इस समय के बारे में श्रीमद्भागवत महापुराण का ये श्लोक कुछ ऐसा कहता है –
(निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दन।) देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु: सर्वगुहाशय: आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशि इन्दुरिव पुष्कल:।। ८।
(श्रीमद्भागवत पुराण, स्कन्ध 10, अध्याय 3, श्लोक 8) श्रीमद्भागवत महापुराण के दसवें स्कन्ध के अध्याय 3 के श्लोक 8 में ये कहा गया है कि – “ उस रात में उन जनार्दन ( विष्णु) के जन्म का समय आया। चारों तरफ अन्धकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके ह्दय में विराजमान विष्णु देवरुपिणी देवकी के गर्भ से प्रगट हुए , जैसे पूर्व दिशा में सोलहों कलाओं से पूर्ण चन्द्रमा का उदय हुआ हो।“
स्पष्ट है कि श्रीमद्भागवत महापुराण में श्रीकृष्ण के न तो जन्म की तिथि बताई गई है और न ही उनके जन्म का नक्षत्र , लेकिन श्री हरिवंशपुराण श्रीकृष्ण के जन्म का नक्षत्र. मुहूर्त दोनों के बारे में बताता है –
अभिजिन्नाम नक्षत्रं जयन्ती नाम शर्वरी।
मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दनः॥
(हरिवंशपुराण, विष्णुपर्व, अध्याय – 4 – श्लोक – 17)
हरिवंश पुराण के इस श्लोक के अनुसार जब भगवान् जनार्दन (विष्णु) का अवतार हो रहा था, उस नक्षत्र का नाम अभिजित्, रात्रि का नाम जयन्ती और मुहूर्त का नाम विजय था। लेकिन आश्चर्य की बात यहां भी यही है कि श्रीकृष्ण के जन्म की तिथि नहीं बताई गई है और न ही महीना बताया गया है ।
यद्यपि हमनें इस लेख में विश्वामित्र संहिता और पद्मपुराण उत्तरखण्ड" ब्रह्मपुराण" विष्णु पुराण" और कुछ ग्रन्थों के अनुसार ये दिखाया है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म सावन के महीने में अष्टमी की तिथि को ही हुआ था।
ये हो सकता है कि महीने और पक्षो में कुछ हजार सालो में परिवर्तन होता रहता हो और इसलिए ये भ्रम आज भी बना हुआ है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म आखिरकार किसी तिथि और किस महीने हुआ था। -
ब्रह्मपुराण अवतार प्रयोजन वर्णन-
"व्यास उवाच"
श्रृणुध्वं मुनिशार्दूलाः प्रवक्ष्यामि समासतः। अवतारं हरेश्चात्र भारावतरणेच्छया।।१८१.१।।
यदा यदा त्वधर्मस्य वृद्धिर्भवति भो द्विजाः। धर्मश्च ह्रासमभ्योति तदा देवो जनार्दनः॥१८१.२ ।।
अवतारं करोत्यत्र द्विधा कृत्वाऽऽत्मनस्तनुम्।साधूनां रक्षणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च॥१८१.३।
दुष्टानां निग्रहार्थाय अन्येषां च सुरद्विषाम्।प्रजानां रक्षणार्थाय जायतेऽसौ युगे युगे।।१८१.४ ।।
पुरा किल मही विप्रा भूरिभारावपीडिता। जगाम धरणी मेरौ समाजे त्रिदिवौकसाम्।।१८१.५।
सब्रह्मकान्सुरान्सर्वान्प्रणित्याथ मेदिनी।कथयामास तत्सर्वं खेदात्करुणभाषिणी।।१८१.६।।
धरण्युवाच
अग्निः सुवर्णस्य गुरुर्गवां सूर्योऽपरो गुरुः।ममाप्यखिललोकानां वन्द्यो नारायणो गुरुः।। १८१.७ ।।
तत्सांप्रतमिमे दैत्याः कालनेमिपुरोगमाः। मर्त्यलोकं समागम्य बाधन्तेऽहर्निशं प्रजाः।। १८१.८ ।।
कालनेमिर्हतो योऽसौ विष्णुना प्रभविष्णुना।उग्रसेनसुतः कंसः संभूतः सुमहासुरः।।१८१.९ ।।
अरिष्टो धेनुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा।सुन्दोऽसुरस्तथाऽत्युग्रो वाणश्चापि बलेः सुतः।। १८१.१० ।।
तथाऽन्ये च महावीर्या नृपाणां भवनेषु ये। समुत्पन्ना दुरात्मानस्तान्न संख्यातुमुत्सहे।। १८१.११ ।।
अक्षौहिण्यो हि बहुला दिव्यमूर्तिधृताः सुराः।महाबलानां दृप्तानां दैत्येन्द्राणां ममोपरि।। १८१.१२ ।।
तद्भूरिभारपीडार्ता न शक्नोम्यमरेश्वराः।विभर्तुमात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः।। १८१.१३ ।।
क्रियतां तन्महाभागा मम भारावतारणम्। यथा रसातलं नाहं गच्छेयमतिविह्वला।।१८१.१४।।
व्यास उवाच
इत्याकर्ण्य धरावाक्यमशेषैस्त्रिदशैस्ततः।भुवो भारावतारार्थं ब्रह्मा प्राह च चोदितः।। १८१.१५ ।।
ब्रह्मोवाच
यदाह वसुधा सर्वं सत्यमेतद्दिवौकसः। अहं भवो भवन्तश्च सर्वं नारायणात्मकम्।।१८१.१६ ।।
विभूतयस्यु यास्तस्य तासामेव परस्परम्। आधिक्यं न्यूनता बाध्यबाधकत्वेन वर्तते।। १८१.१७ ।।
तदागच्छत गच्छामः क्षीराब्धेस्तटमुत्तमम्।तत्राऽऽराध्य हरिं तस्मै सर्वं विज्ञापयाम वै।। १८१.१८ ।।
सर्वदैव जगत्यर्थे स सर्वात्मा जगन्मयः।स्वल्पांशेनावतीर्योर्व्यां धर्मस्य कुरुते स्थितिम्।। १८१.१९ ।।
व्यास उवाच
इत्युक्त्वा प्रययौ तत्र सह देवैः पितामहः।समाहितमना भूत्वा तुष्टा गरुडध्वजम्।। १८१.२०।
ब्रह्मोवाच
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रमूर्ते, सहस्रबाहो बहुवक्त्रपाद। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्तिविनाशसंस्थानपराप्रमेय।।१८१.२१ ।।
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं च बृहत्प्रमाणं गरीयसामप्यतिगौरवात्मन्।प्रधानबुद्धीन्द्रियवाक्प्रधानमूला परात्मन्भगवन्प्रसीद।।१८१.२२ ।।
एषा मही देव महीप्रसूतैर्महासुरैः पीडितशैलबन्धा।परायणं त्वां जगतामुपैति, भारावतारार्थमपारपारम्।।१८१.२३ ।।
एते वयं वृत्ररिपुस्तथाऽयं, नासत्यदस्रौ वरुणस्तथैषः। इमे च रुद्रा वसवः ससूर्याः, समीरणाग्निप्रमुखास्तथाऽन्ये।। १८१.२४ ।।
सुराः समस्ताः सुरनाथ कार्यमेभिर्मया यच्च तदीश सर्वम्। आज्ञापयाऽऽज्ञां प्रतिपालयन्तस्तवैव तिष्ठाम सदाऽस्तदोषाः।।१८१.२५।।
व्यास उवाच
एवं संस्तूयमानस्तु भगवान्परमेश्वरः।उज्जहाराऽऽत्मनः केशौ सितकृष्णौ द्विजोत्तमाः।। १८१.२६ ।।
उवाच च सुरानेतै मत्केशौ वसुधातले। अवतीर्य भुवो भारक्लेशहानिं करिष्यतः।। १८१.२७ ।।
सुराश्च सकलाः स्वांशैरवतीर्य महीतले। कुर्वन्तु युद्धमुन्मत्तैः पूर्वोत्पन्नैर्महासुरैः।।१८१.२८।।
ततः क्षयमशेषास्ते दैतेया धरणीतले। प्रयास्यन्ति न संदेहो नानायुधविचूर्णिताः।। १८१.२९ ।।
वसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा। तस्या गर्भोऽष्टमोऽयं तु मत्केशो भविता सुराः।। १८१.३०।।
अवतीर्य च तत्रायं कंसं घातयिता भुवि।कालनेमिसमुद्भूतमित्युक्त्वाऽन्तर्दधे हरिः।। १८१.३१ ।।
अदृश्याय ततस्तेऽपि प्रणिपत्य महात्मने। मेरुपृष्ठं सुरा जग्मुरवतेरुश्च भूतले।। १८१.३२ ।।
कंसाय चाष्टमो गर्भो देवक्या धरणीतले।भविष्यतीत्याचचक्षे भगवान्नारदो मुनिः।। १८१.३३ ।।
कंसोऽपि तदुपश्रुत्य नारदात्कुपितस्ततः। देवकीं वसुदेवं च गृहे गुप्तावधारयत्।। १८१.३४ ।
जातं जातं च कंसाय तेनैवोक्तं यथा पुरा। तथैव वसुदेवोऽपि पुत्रमर्पितवान्द्विजाः।। १८१.३५ ।।
हिरण्यकशिपोः पुत्राः षड्गर्भा इति विश्रुताः।विष्णुप्रयुक्ता तान्निद्रा क्रमाद्गर्भे न्ययोजयत्।। १८१.३६ ।।
योगनिद्रा महामाया वैष्णवी मोहितं यया। अविद्यया जगत्सर्वं तामाह भगवन्हरिः।१८१.३७।
विष्णुरुवाच
गच्छ निद्रे ममाऽऽदेशात्पातालतलसंश्रयान्।एकैकश्येन षड्गर्भन्देवकीजठरे नय।१८१.३८ ।।
हतेषु तेषु कंसेन शेषाख्योऽशस्ततोऽनघः।अंशांसेनोदरे तस्याः सप्तमं संभविष्यति।। १८१.३९ ।।
गोकुले वसुदेवस्य भाराया वै रोहिणी स्थिता।तस्याः प्रसूतिसमये गर्भो नेयस्त्वयोदरम्।। १८१.४० ।।
सप्तमो भोजराजस्य भयाद्रोधोपरोधतः। देवक्याः पतितो गर्भ इति लोको वदिष्यति।। १८१.४१ ।।
गर्भसंकर्षणात्सोऽथ लोके संकर्षणेति वै।संज्ञामवाप्स्यते वरीः श्वेताद्रिशिखरोपमः।। १८१.४२ ।।
ततोऽहं संभविष्यामि देवकीजठरे शुभे। गर्भे त्वया यशोदाया गन्तव्यमविलम्बितम्।। १८१.४३ ।।
प्रावृट्काले च नभसि कृष्णाष्टम्यामहं निशि।उत्पत्स्यामि नवम्यां च प्रसूतिं त्वमवाप्स्यसि।। १८१.४४ ।।
यशोदाशयने मां तु देवक्यास्त्वामनिन्दिते।मच्छक्तिप्रेरितमतिर्वसुदेवो नयिष्यति।१८१.४५।।
कंसश्च त्वामुपादाय देवि शैलशिलातले।प्रक्षेप्स्यत्यन्तरिक्षे च त्वं स्थानं समवाप्स्यसि।। १८१.४६ ।।
ततस्त्वां शतधा शक्रः प्रणम्य मम गौरवात्।प्रणिपातानतशिरा भगिनीत्वे ग्रहीष्यति।। १८१.४७ ।।
ततः शुम्भनिशुम्भादीन्हत्वा दैत्यान्सहस्रशः।स्थानैरनेकैः पृथिवीमसेषां मण्डयिष्यसि।। १८१.४८ ।।
त्वं भूतिः संनतिः कीर्तिः कान्तिर्वै पृथिवी धृतिः।लज्जापुष्टिरुषा च काचिदन्या त्वमेव सा।। १८१.४९ ।।
ये त्वामार्येति दुर्गेति वेदगर्भेऽम्बिकेति च। भद्रेति भद्रकालीति क्षेम्या क्षेमंकरीति च।। १८१.५० ।।
प्रातश्चैवापराह्णे च स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः। तेषां हि वाञ्छितं सर्वं मत्प्रसादाद्भविष्यति।। १८१.५१ ।।
सुरामांसोपहारैस्तु भक्ष्यभोज्यैश्च पूजिता।नृणामशेषकामांस्त्वं प्रसन्नायां प्रदास्यसि।। १८१.५२ ।।
ते सर्वे सर्वदा भद्रा मत्प्रसादादसंशयम्। असंदिग्धं भविष्यन्ति गच्छ देवि यथोदितम्।। १८१.५३ ।।
इति श्रीमहापुराणे(ब्रह्मपुराणे) आदिब्राह्मे हरेरंशावतारनिरूपणं नामैकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः।।१८१ ।।
अनुवाद:-
अध्याय 72(182) - हरि के अवतार
व्यास ने कहा :
हे श्रेष्ठ मुनियों, सुनो, मैं तुम्हें संक्षेप में उन अवतारों का वर्णन करूँगा जो पृथ्वी का भार हरने के लिए भगवान श्रीहरि ने धारण किये थे।1।
हे ब्राह्मणो, जब-जब पाप बढ़ता है और पुण्य क्षीण होता है, तब-तब भगवान विष्णु सज्जनों की रक्षा, पुण्य की स्थापना और दुष्टों तथा देव- शत्रुओं का दमन करने के लिए अपने शरीर को दो भागों में विभाजित करके अवतार लेते हैं। वे प्रजा की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में जन्म लेते हैं ।2-4।
हे ब्राह्मणों ! पूर्वकाल में पृथ्वी अत्यधिक भार से पीड़ित हो गई थी। पृथ्वी स्वर्गवासियों की सभा में गई। ब्रह्मा सहित देवताओं को प्रणाम करके पृथ्वी ने दुःखी होकर सब कुछ कह सुनाया।5-6।
पृथ्वी ने कहा
अग्नि देवताओं के गुरु हैं, सूर्य गौओं के गुरु हैं, तथा नारायण मेरे तथा अन्य लोगों द्वारा नमस्कार किये जाने योग्य लोगों के गुरु हैं।7।
अब कालनेमि के अनुयायी दैत्य इस मृत्युलोक में आ गए हैं। वे दिन-रात प्रजा को कष्ट पहुँचाते हैं।8।
वह असुर कालनेमि, जो सर्वशक्तिमान विष्णु द्वारा मारा गया था, अब महान असुर कंस और उग्रसेन के पुत्र के रूप में जन्म ले रहा है ।9।
. अरिष्ट , धेनुका , केशिन , प्रलम्ब , नरक , सुन्द , बाण , बलि का भयंकर पुत्र आदि कई अन्य अत्यंत शक्तिशाली असुर हैं । ये राजाओं के लोकों में उत्पन्न दुष्ट आत्माएँ हैं। मैं उन सभी की गणना करने का प्रयास नहीं कर सकका हूँ।10-11।
हे दिव्य रूप धारण करने वाले देवो ! मुझ पर बहुत सी अक्षौहिणी (अत्यंत बलवान अभिमानी दैत्यों की विशाल सेना) आक्रमण कर रही हैं।12।
हे अमर प्राणियों के स्वामियों, उनके अत्यधिक भार से व्यथित और पीडित होकर मैं स्वयं को स्थिर नहीं कर पा रही हूँ। हे परम धन्यों, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर से यह अतिरिक्त भार हटा दें, अन्यथा मैं मोहवश अधोलोक में डूब जाऊँगी।13-14।
व्यास ने कहा :
पृथ्वी के ये शब्द सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा से पृथ्वी का भार हटाने का अनुरोध किया।15।
ब्रह्मा ने कहा :
हे स्वर्गवासियों! पृथ्वी जो कुछ कहती है, वही सत्य है। तुम सब, मैं और हर - हम सभी नारायण की उत्कृष्ट और मनोहर शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों में दूसरों को रोकने और उनके द्वारा बाधित होने की श्रेष्ठता और हीनता की भावना है। इसलिए आओ। हम क्षीरसागर के उत्तम तट पर जाएँगे। वहाँ हम हरि को प्रसन्न करेंगे और उन्हें सब कुछ बताएँगे।16-18।
. वह प्रभु सबका आत्मा है । वह ब्रह्मांड के समान है। वह सदैव आपके हित के लिए कार्य करेगा। अपने एक छोटे से अंश के साथ वह पृथ्वी पर जन्म लेगा और सद्गुणों की स्थापना करेगा।19।
व्यास ने कहा : ऐसा कहकर ब्रह्माजी देवताओं के साथ चले गए। उन्होंने पूर्ण एकाग्रता से गरुड़देव की स्तुति की ।20।
ब्रह्मा ने कहा :
हे हजार रूपों वाले प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है; हे हजार भुजाओं वाले, हे अनेक भुजाओं और अनेक पैरों वाले, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, हे ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार में लगे हुए प्रभु, हे अज्ञेय।21।
. हे प्रभु, आप सूक्ष्मतम प्राणियों में भी सूक्ष्मतम हैं; आपका आकार महान है, आप सबसे भारी से भी भारी हैं। हे प्रभु, प्रधान , ब्रह्माण्डीय बुद्धि और इन्द्रियों से युक्त, हे प्रमुख लोकों के समान प्रभु, आप प्रसन्न हों।22।
हे प्रभु, पृथ्वी पर उत्पन्न हुए पराक्रमी असुरों के कारण यह पृथ्वी अत्यंत पीड़ित है। यह दुःख के भारी भार से व्यथित है। इस भार को दूर करने के लिए यह आपके पास आई है, जो लोकों के परम आश्रय हैं, तथा आपसे बढ़कर कोई अन्य उद्धारक नहीं है।23।
. हे देवराज! हम सभी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं - वृत्र , नासत्य और अश्विन का संहार करने वाले इन्द्र , वरुण , रुद्र , वसु , सूर्य, वायु , अग्नि और देवता। हे देव! इन सबको और मुझे क्या करना चाहिए, इसकी आज्ञा दीजिए। हम दोषों से बचने के लिए भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे ।24-25।
व्यास ने कहा :
. हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार स्तुति करने पर, महाप्रभु ने अपने सिर से दो बाल उखाड़े, एक श्वेत और दूसरा काला। फिर उन्होंने देवताओं से इस प्रकार कहा, "मेरे ये दो बाल अत्यधिक भार से व्यथित पृथ्वी पर अवतार लेंगे।"26-27।
सभी देवता पृथ्वी पर अवतार लें। वे पहले से ही उत्पन्न हुए शक्तिशाली अभिमानी असुरों से युद्ध करें।28
फिर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पृथ्वी पर जितने भी असुर हैं, उन सबका नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों द्वारा चूर्ण-चूर्ण करके नाश कर दिया जाएगा।29।
हे अमर ! मेरा यह बाल (केश) वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से आठवें बच्चे के रूप में जन्म लेगा , जो देवों के समान है।30।
पृथ्वी पर जन्म लेकर यह कालनेमि के कंस-वर का वध करेगा। ऐसा कहकर श्रीहरि वहीं अन्तर्धान हो गये।3।
तब उन देवताओं ने उन महान भगवान को प्रणाम किया जो अदृश्य हो गए, मेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर उतर आए।32।
नारद मुनि ने कंस से कहा - "पृथ्वी पर उत्पन्न देवकी के गर्भ से आठवाँ बालक तुम्हारा वध करेगा।33।
34. नारद से यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी और वसुदेव को उनके ही घर में बंदी बनाकर उनके कुएँ की रखवाली करने लगा।34।
हे ब्राह्मणों! जब भी कोई पुत्र उत्पन्न होता तो वसुदेव तुरन्त उस पुत्र को कंस को सौंप देते थे, जैसा कि उन्होंने स्वयं पहले ही उसे बताया था।35।
हिरण्यकशिपु के पुत्र गर्भस्थ शिशु के रूप में विख्यात हुए। विष्णु द्वारा प्रेरित होकर उनकी योगनिद्रा ने उन्हें क्रमशः देवकी के गर्भ से जोड़ दिया।36।
भगवान विष्णु की इस योगनिद्रा को महामाया और अविद्या भी कहते हैं । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उनसे मोहित है।37।
[ नोट : ब्रह्मपुराण के कुछ संस्करणों में यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।
"भगवान हरि ने उससे कहा :
हे निद्रा ! यहाँ से जाओ। मेरे कहने पर इन (हिरण्यकशिपु के) बालकों को, जो इस समय पाताल लोक में हैं, एक-एक करके देवकी के गर्भ में ले जाओ।38।
जब वे कंस द्वारा मारे जाएँगे, तो मेरा पापरहित अंश शेष, एक छोटे से अंश के रूप में देवकी के गर्भ में सातवाँ बालक बनेगा।39।
अहीरों की बस्ती में वसुदेव की एक और पत्नी रोहिणी है । देवकी के गर्भ में बच्चा पैदा होने पर उसे रोहिणी के गर्भ में ले जाना चाहिए। तब लोग कहेंगे कि कंस के भय और कारावास की कठोरता के कारण देवकी के गर्भ में सातवें बच्चे का गर्भपात हो गया।40-41।
चूँकि गर्भस्थ शिशु को खींच लिया गया है, अतः संसार में मेरु शिखर के समान वीर बालक संकर्षण का जन्म होगा।42।
तब मैं देवकी के शुभ गर्भ से जन्म लूँगा। तुम भी अविलम्ब यशोदा के गर्भ में जाओ।43।
मैं वर्षा ऋतु में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि में जन्म लूँगा । तुम्हारा जन्म नवमी तिथि को होगा।44।
हे आनन्दिते, मेरी शक्ति से प्रेरित होकर वसुदेव मुझे यशोदा के शयन-शयन-स्थल पर ले जाएंगे और तुम्हें देवकी के शयन-स्थल पर।45।
हे भद्रे , कंस तुम्हें पकड़कर एक चट्टान पर पटक देगा। तत्पश्चात तुम आकाश में निवास करोगी।46।
इन्द्र मेरे प्रति आदरपूर्वक सौ बार तुम्हें प्रणाम करेगा; सिर झुकाकर तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करेगा।47।
तत्पश्चात् तुम हजारों दैत्यों का वध करोगे और विभिन्न धामों से सम्पूर्ण पृथ्वी को सुशोभित करोगे।48।
आप निम्नलिखित देवियों के समान हैं:— भूति (अस्तित्व), सन्नति (नमस्कार), कीर्ति (यश), कांति (तेज), पृथ्वी (पृथ्वी), धृति (साहस), लज्जा (शर्म), पुष्टि (पोषण), उमा तथा अन्य देवियाँ, चाहे वे कोई भी हों।49।
यदि भक्तगण प्रातःकाल और मध्याह्न में अपने स्वरूप को झुकाकर आपकी स्तुति करें और आपको आर्या , दुर्गा , वेदगर्भा , अम्बिका , भद्रा , भद्रकाली , क्षेम्या और क्षेमकारी कहकर सम्बोधित करें, तो मेरी कृपा से उन्हें जो कुछ भी चाहिए होगा।50-51।
.मदिरा, मांस, अन्य उपहारों और विविध खाद्य पदार्थों से पूजित होकर आप प्रसन्न होंगी और मनुष्यों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करेंगी।52।
निःसंदेह, मेरी कृपा से उन सबका सदैव कल्याण होगा। इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हे भद्र महिला, आप पहले बताए गए तरीके से जाएँ।53।
__________________________________
"प्रावृट्काले च 'नभसि' कृष्णाष्टम्यामहं निशि।उत्पत्स्यामि नवम्यां तु प्रसूतिं त्वमवाप्स्यसि ।।
अर्थात– वर्षाऋतु में नभस् (श्रावण) मास की अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूँगा और तुम (योगमाया) नवमी को उत्पन्न होगी।
टिप्पणी- नभस्य और नभस् जो पृथक शब्द हैं।और दोनो का ही अर्थ भिन्न भिन्न है।
नभस्य -भाद्रपदमासे नभःशब्दे उदाहरण । “प्रथमा च द्वितीया च नभस्ये मासि निग्दिता” वसिष्ठः। “अथ नभस्य इव त्रिदशायुषम्” रघुवंश महाकाव्य- नभस्य शब्द का अर्थ भाद्रपद मास है और विष्णु पुराण में इसका प्रयोग न हेकर नभस्- नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। नभस् का सप्तमी एक वचन अधिकरण कारक- रूप हुआ नभसि-
नभस्- श्रावणे मासि पु० अमरः कोश । बाहुल्येन मेघसम्बन्धात्तस्य तथात्वम् । “नभोनभस्यत्वमलम्भितद्दृशौ” नैषधीय चरितं “नभाश्च नभस्यश्च वार्षिकावृतू” यजुर्वेद- १४।१५ ।
यहाँ यह बात विचारणीय है कि श्रीकृष्ण का जन्म वर्षा ऋतु के नभस् अर्थात् (सावन) श्रावण मास में हुआ था। भाद्रपद मास में नहीं। भाद्रपद की परम्परा क्यों और कैसे बनी ये बुद्धिजीवियों की चिन्ता का विषय होना चाहिए।
अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'Notable Horoscopes' के प्रथम पृष्ठ पर डॉ वी बी रामन ने उनकी जन्म तिथि अमान्त श्रावण अष्टमी को ( १९ जुलाई ३२२८ बीसी ) बताई है।
हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व 4/17 में कहा है कि-
अभिजिन्नाम नक्षत्रं जयन्ती नाम शर्वरी । मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दनः ।।
अर्थात – जब योगेश्वर श्रीकृष्ण प्रकट हुए उस समय अभिजित् नामक 'नक्षत्र' था, जयन्ती नाम की रात्रि थी और विजय नामक विशिष्ट मुहूर्त था
पद्मपुराण उत्तरखण्ड (31/32) में कहा गया है कि
सनत्कुमार उवाच-
शृणुष्वावहितो राजन्कथ्यमानं मया तव।श्रावणस्य तु मासस्य कृष्णाष्टम्यां नराधिप।३२।
रोहिणी यदि लभ्येत जयंती नाम सा तिथिः भू योभूयो महाराज भवेज्जन्मनि कारणम्।३३।
अर्थात – हे राजन, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो उस तिथि को जयन्ती तिथि कहा जाता है।
उपर्युक्त सभी प्रमाणों से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी वर्षा ऋतु के श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही सिद्ध होती है।
ज्ञातव्य है कि यजुर्वेद १४ /१५ के अनुसार नभस्च नभस्यश्च वार्षिकावृतु, अर्थात् श्रावण (प्रथम) और भाद्रपद (दूसरा), ये दो महीने वर्षा ऋतु के होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दक्षिणायन/वर्षा ऋतु/श्रावण सङ्क्रान्ति से सम्बद्ध सौरमास से जुड़े चान्द्रमास की निशीथ व्यापिनी अष्टमी को ही होती है।
दैनिक पञ्चाङ्ग से जुड़े सन्देश में निम्न लिखित अंश प्रतिदिन अनुदानित हैं -
सूर्य व चन्द्र के भोगांशों देशान्तर (Longitudes) से हम सौर एवं चान्द्रमासों तथा आज की तिथि का और पुनः दी हुई क्रान्ति (Declination of the Sun) से वापस सूर्य भोगांश के सत्य का परीक्षण कर सकते हैं। इसी से होगा पञ्चागों के झूठ और सच के दूध का दूध और पानी का पानी समस्त पञ्चाङ्ग निर्माता और ज्योतिर्विदजन ही नहीं हमारे सभी पाठक मित्र भी कृपया इस गुरुमन्त्र को अपनी स्मरण में गाण्ठ बान्ध कर रख लें-- समीचिना क्रान्ति: सङ्क्रान्ति:।।
अस्तु, सिद्धान्त सम्मत क्रान्ति सिद्ध सङ्क्रान्तियों के अनुसार (देखें ऋग्वेद १/१५५/०६) तो बृहस्पतिवार, १७ जुलाई २०२५ को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि सिद्ध होती है जो कि आज भूतकाल का विषय बन चुकी है।
___________
अब ब्रह्मपुराण के समान ही विष्णुपुराण और भागवतपुराण से समान श्लोक उद्धृत कर निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं।
श्रीपराशर उवाच
एवं संस्तूयमानस्तु भगवान्परमेश्वरः ।
उज्जहारात्मनः केशौ सितकृष्णौ महामुने॥ ५,१.६०॥
उवाच च सुरानेतौ मत्केशौ वसुधातले ।
अवतीर्य भुवो भारक्लेशहानिं करिष्यतः॥ ५,१.६१॥
विशेष-भूमेः सुरेतरवरूथविमर्दितायाः।क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः। जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः। कर्माणि चाऽऽत्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥२६॥
श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कन्ध अध्याय (7) द्वितीय स्कन्ध: सप्तम अध्यायः (7) श्लोक 26- का हिन्दी अनुवाद:
भगवान् के लीलावतारों की कथा:-जिस समय झुण्ड-के-झुण्ड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे उस समय उसका भार उतारने के लिये भगवान् अपने सफ़ेद और काले केश से बलराम और श्रीकृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिलकुल नहीं समझ सकेंगे ।26।
श्लोक का संदर्भ:यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान कृष्ण, अपने पूर्ण विस्तार सहित, पृथ्वी पर संकट को समाप्त करने के लिए प्रकट हुए।
"सितकृष्णकेशः" शब्द का प्रयोग यहाँ कृष्ण के (श्वेत)और '(काले') 'सुन्दर' केशों के लिए किया गया है, जो उनकी उपस्थिति का वर्णन करता है
यह दर्शाता है कि भगवान कृष्ण (जिन्हें अक्सर कृष्ण वर्ण का माना जाता है) के आने से पृथ्वी पर सुख-शांति स्थापित होगी।
पुन: विष्णु पुराण से उद्धृत क्रमश: श्लोक-
सुराश्च सकलाःस्वांशैरवतीर्य महीतले ।
कुर्वन्तु युद्धमुन्मत्तैः पूर्वोत्पन्नैर्महासुरैः ॥५,१.६२॥
ततः क्षयमशेषास्ते दैतेया धरमीतले ।
प्रयास्यन्ति न संदेहो मद्दृपातविचूर्णिताः॥ ५,१.६३॥
वसुदेवस्य या पत्नी देवकी देवतोपमा ।
तत्रायमष्टमो गर्भो मत्केशो भविता सुराः ॥ ५,१.६४ ॥
अवतीर्य च तत्रायं कंसं घातयिता भुवि ।
कालनेमीं समुद्भूतमित्युक्त्वान्तर्दधे हरिः ॥ ५,१.६५ ॥
अदृश्याय ततस्तस्मै प्रणिपत्य महामुने ।
मेरुपृष्ठं सुरा जग्मुरवतेरुश्च भूतले ॥ ५,१.६६ ॥
कंसाय चाष्टमो गर्भो देवक्या धरणीधरः ।
भविष्यतीत्याच चक्षे भगवान्नारदो मुनिः ॥ ५,१.६७ ॥
कंसोऽपि तदुपश्रुत्य नारदात्कुपितस्ततः ।
देवकीं वसुदेवं च गृहे गुप्तावधारयत् ॥ ५,१.६८ ॥
वसुदेवेन कंसाय तेनैवोक्तं यथा पुरा ।
तथैव वसुदेवोऽपि पुत्रमर्पितवान् द्विज ॥ ५,१.६९॥
हिरण्यकशिपोः पुत्राःषड्गर्भा इति विश्रुताः ।
विष्णुप्रयुक्ता स्तान्निद्राक्रमाद्गर्भानयोजयत् ॥ ५,१.७० ॥
योगनिद्रा महामाया वैष्णवी मोहितं यया ।
अविद्यया जगत्सर्वं तामाह भगवान्हरिः ॥५,१.७१॥
श्रीभगवानुवाच
निद्रे गच्छ ममादेशात्पातालातलसंश्रयान् ।
एकैकत्वेन षड्गर्भान्देवकीजठरं नय ॥ ५,१.७२ ॥
हतेषु तेषु कंसेन शेषाख्योंशस्ततो मम ।
अंशांशोनादरे तस्याःसप्तमः संभविष्यति ॥ ५,१.७३ ॥
गोकुले वसुदेवस्य भार्यान्या रोहिणी स्थिता ।
तस्याःस सम्भूतिसमं देवि नेयस्त्वयोदरम् ॥ ५,१.७४ ॥
सप्तमो भोजराजस्य भयाद्रोधोपरोधतः ।
देवक्याः पितितो गर्भ इति लोको वदिष्यति ॥ ५,१.७५ ॥
गर्भसंकर्षणात्सोऽथ लोके संकर्षणेति वै ।
संज्ञामवाप्स्यते वीरः श्वेताद्रिशिखरोपमः ॥ ५,१.७६ ॥
ततोऽहं संभविष्यामि देवकीजठरे शुभे ।
भर्गं त्वया यशोदाया गन्तव्यमविलंबितम् ॥ ५,१.७७ ॥
*****
प्रावृट्काले च नभसि कृष्णाष्टम्यामहं निशि ।
उत्पत्स्यामि नवम्यां तु प्रसूतिं त्वमवाप्स्यसि ॥ ५,१.७८ ॥
यशोदाशयने मां तु देवक्यास्त्वामनिन्दिते ।
मच्छक्तिप्रोरितमतिर्वसुदेवो नयिष्यति ॥५,१.७९ ॥
कंसश्च त्वामुपादाय देवि शैलशिलातले ।
प्रक्षेप्स्यत्यन्तारिक्षे च संस्थानं त्वमवाप्स्यसि ॥ ५,१.८० ॥
ततस्त्वां शतदृक्छक्रः प्रणम्य मम गौरवात् ।
प्रणिपातानतशिरा भगिनीत्वे ग्रहीष्यति ॥५,१.८१।
त्वं च शुंभनिशुंभादीन्हत्वा दैत्यान्सहस्रशः ।
स्थानैरनेकैः पृथिवीमशेषां मण्डयिष्यसि ॥ ५,१.८२ ॥
त्वं भूतिः सन्नतिः क्षान्तिः कान्तिर्द्यौः पृथिवी धृतिः
लज्जापुष्टी रुषा या तु काचिदन्या त्वमेव सा ॥ ५,१.८३ ॥
ये त्वामार्येति दुर्गेति वेदगर्भांबिकेति च ।
भद्रेति भद्रकालीति क्षेमदा भग्यदेति च ॥ ५,१.८४॥
प्रातश्चैवापराह्ने च स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः ।
तेषां हि प्रार्थितं सर्वं मत्प्रसादाद्भविष्यति ॥ ५,१.८५ ॥
सुरामांसोपहरैश्च भक्ष्यभोज्यैश्च पूजिता ।
नॄणामशेषसामांस्त्वं प्रसन्ना संप्रदास्यसि ॥ ५,१.८६ ॥
ते सर्वे सर्वदा भद्रे मत्प्रसादादसंशयम् ।
असंदिग्धा भविष्यन्ति गच्छ देवि यथोदितम् ।
इति विष्णुमहापुराणे पञ्चमांशे प्रथमोऽध्यायः (१)
***************
अनुवाद:-
श्री पराशर जी बोले ;- हे महामुने ! इस प्रकार स्तुति किये जानेपर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े ॥ ५ ९॥
******************************
और देवताओं से बोले-मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथिवी के भाररूप कष्ट को दूर करेंगे ॥ ६० ॥
सब देवगण अपने-अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें।६१॥
तब मेरे दृष्टिपात से दलित होकर पृथिवी तलपर सम्पूर्ण दैत्यगण निस्सन्देह क्षीण हो जाएँगे ॥६२।।
वसुदेवजी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है उसके आठवें गर्भ से मेरा यह (श्याम ) केश अवतार लेगा ॥६३॥
और इस प्रकार वहाँ अवतार लेकर यह कालनेमि का अवतार कंस का वध करेगा।' ऐसा कहकर श्रीहरि अन्तर्धान हो गये ॥६४॥
हे महामुने ! भगवान के अदृश्य हो जानेपर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गये और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए ॥ ६५ ॥
इसी समय भगवान नारदजी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के आठवें गर्भ में भगवान धरणी धर जन्म लेंगे ॥६६॥
नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया ॥ ६७ ॥
द्विज ! वसुदेव जी भी, जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपना प्रत्येक पुत्र कंस को सौंपते रहे ॥६८ ॥
*********************************
ऐसा सुना जाता है कि ये छः गर्भ पहले हिरण्य कशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योगनिद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही ।।६९॥
*******
विशेष- परन्तु देवीभागवतपुरण के अनुसार ये छै: पुत्र अदिति के थे। और सातवाँ बलराम रूप शेषनाग कद्रु के पुत्र थे। परन्तु अदिति रूप देवकी के छ: स्थापित पुत्र और सप्तम गर्भविस्थापित पुत्र बलराम थे।
(जाता विनश्येरंस्तव पुत्रास्तु सप्त वै" - देवी भागवतमहापुराण)
अत: देवीभागवत पुराण का वर्णन सत्य तथा तर्कसंगत है। जबकि विष्णु पुराण और ब्रह्मपुराण का वर्णन प्रक्षेप है।
जिस अविद्या-रूपिणी से सम्पूर्ण जगत् मोहित हो रहा है, वह योगनिद्रा भगवान विष्णु के महामाया है उससे भगवान श्री हरि ने कहा--॥ ७०॥
श्रीभगवान् बोले - हे निद्रे ! जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित छः गर्भ को एक-एक करके देवकी की कुक्षि में स्थापित कर दे॥७१।।
कंस द्वारा उन सबके मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश देवकी के सातवें गर्भ में स्थित होगा ॥७२॥
हे देवि ! गोकुल में वसुदेवजी की जो रोहिणी नामकी दूसरी भार्या रहती है उसके उदर में उस सातवें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े ॥७३॥
उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बन्द होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का सातवाँ गर्भ गिर गया ॥७४॥
वह श्वेत शैलशिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किये जाने के कारण संसार में 'सङ्गर्षण' नाम से प्रसिद्ध होगा॥ ७५॥
तदनन्तर, हे शुभे ! देवकी के आठवें गर्भ में मैं स्थित होऊँगा । उस समय तू भी तुरन्त ही यशोदा के गर्भ में चली जाना ॥७६॥
********
वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात्रि के समय मैं जन्म लूंगा और तू नवमी को उत्पन्न होगी। ७७ ॥
हे अनिन्दिते ! उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयनगृह में ले जाएंगे ॥७८॥
तब, हे देवि ! कंस तुझे पकड़कर पर्वत-शिलापर पटक देगा; उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जायगी ॥ ७९ ।।
उस समय मेरे गौरव से सहस्रनयन इन्द्र शिर झुकाकर प्रणाम करनेके अनन्तर तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा॥ ८० ॥
तू भी शुम्भ, निशुम्भ आदि ,सहस्र दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी॥८१॥
तू ही भूति, सन्नति, क्षान्ति और कन्ति है; तू ही आकाश, पृथिवी, धृति, लज्जा, पुष्टि और उषा है; इनके अतिरिक्त संसारमें और भी जो कोई शक्ति है वह सब तू ही है॥ ८२॥
जो लोग प्रातः काल और सायंकाल में अत्यन्त नम्रतापूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अम्बिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे उनकी समस्त कामनाएँ मेरी कृपा से पूर्ण हो जायँगी ॥८३-८४ ॥
*********
मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थो द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी ॥८५॥
*****
तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएँ मेरी कृपा से निस्सन्देह पूर्ण होंगी। हे देवि ! अब तू मेरे बतलाये हुए स्थानको जा ॥८६॥
ऊपर कही हुई कहानी विष्णुमहापुराण के पञ्चमांश प्रथमोऽध्याय में तथा ब्रह्मा के विधि-विधानों पर केन्द्रित ब्रह्मपुराण( महापुराण) के (181) वें अध्याय में उल्लिखित है। दोनों पाठ एक दूसरे की नकल हैं। यह यज्ञ मूलक कर्मकाण्डों के समर्थ पुरोहितो द्वारा आरोपित हैं । यह सभी क्षेपक ही है।
*********************************
स्कन्द पुराणकार भीराधा जी के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उन्हें आदि शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करता है। देखे निम्नलिखित श्लोकों को-
श्रीकृष्णस्य मनश्चंद्रो राधास्यप्रभयान्वितः ।।तद्विहारवनं गोभिर्मण्डयन्रोचते सदा ।।५।।
कृष्णचन्द्रः सदा पूर्णस्तस्य षोडश याः कलाः ।।चित्सहस्रप्रभाभिन्ना अत्रास्ते तत्स्वरूपता ।। ६ ।।
एवं वज्रस्तु राजेन्द्र प्रपन्नभयभञ्जकः।।श्रीकृष्णदक्षिणे पादे स्थानमेतस्य वर्तते ।।७।।
अवतारेऽत्र कृष्णेन योगमायाऽति भाविता ।।तद्बलेनात्मविस्मृत्या सीदन्त्येते न संशयः ।। ८।।
श्लोकार्थ -
श्रीकृष्ण का मनरूपी चन्द्रमा राधा के मुख की प्रभारूप चाँदनी से युक्त हो उनकी लीलाभूमि वृन्दावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है ।।५।।
श्रीकृष्णचन्द्र नित्य परिपूर्ण हैं, प्राकृत चन्द्रमा की भाँति उनमें वृद्धि और क्षयरूप विकार नहीं होते। उनकी जो सोलह कलाएँ हैं, उनसे सहस्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं; इससे उनके सहस्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त, नित्य परिपूर्ण श्रीकृष्ण इस व्रजभूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं; इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अन्तर नहीं है ।।६।।
राजेन्द्र परीक्षित् ! इस प्रकार विचार करने पर सभी व्रजवासी गोप भगवान् के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करनेवाले जो ये वज्रनाभ हैं, इनका स्थान श्रीकृष्ण के दाहिने चरण में है ।।७।।
इस अवतार में भगवान् श्रीकृष्ण ने इन सबको अपनी योगमाया से अभिभूत कर लिया है, उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गये हैं और इसी कारण सदा दुःखी रहते हैं। यह बात निस्सन्देह ऐसी ही है ।।८।।
___________________
श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे परीक्षिदुद्धवसंवादे श्रीभागवतमाहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः।।३।।
इसके अति आगम ग्रन्थों में कृष्ण यामलतन्त्र के निम्नलिखित श्लोक विचारणीय हैं।
📚: वृषभानुपुराद्याता क्रीडार्थं राधिका स्वयम्।। पारावारेति विख्यातं स्थानं तस्मात् समागता:।।५४।।
कृष्ण यामल तन्त्र-📚
बिम्बाधरेण मुरली कररी विलासी।मायूरपिच्छपरिलाञ्छित चारचूड:।आभीरबालककुलेन विहारकारी।। राधापतिर्मम पुनर्भविताऽनुकूल:।।१५८।
कृष्ण यामल तन्त्र-📚
📚: एक: कृष्णो द्विधाभूतो मुमुक्षुभजनैषिणो:। उपकाराय शुद्धात्मा वेदविद्भि: स गीयते। मुक्तोब्रृह्मपदंयाति तदंगं ज्योतिरुत्तमम्।।८/२६ ख –८/२७ क।(कृष्ण यामल तन्त्र)
प्रकाशन काल में कुछ द्वेषवादी पुरोहितों नें भी ग्रन्थों में छेड़ाखानी की और कुछ जोड़ा कुछ तोड़ा और कुछ मरोड़ा है। अत: पुराण जो कृष्ण द्वैपायन व्यास की रचना बताए जाते परस्पर कहीं कहीं विरोधाभास लिए हुए हैं।
†श्रीकृष्ण जन्माष्टमी †
देवी भागवत पुराण के कुछ श्लोकों में कृष्ण के जन्म वर्णन है। वसुदेव और नन्द दोनों सजातीय एक ही परिवार के व्यक्ति थे।
पद संख्या (231) से (240) तक / तुलसीदास विनयपत्रिका /
बायों दियो बिभव कुरूपति को, भोजन जाइ बिदुर-घर कीन्हो।3।
व्याख्या:
"भविष्यपुराण-(उत्तरपर्व)अध्याय-(55)
सिंहराशिगते सूर्ये गगने जलदाकुले ।
मासि भाद्रपदेऽष्टम्यां कृष्णपक्षेऽर्धरात्रके ।
वृषराशिस्थिते चन्द्रे नक्षत्रे रोहिणीयुते ॥१४॥
वसुदेवेन देवक्यामहं जातो जनाः स्वयम् ।।
एवमेतत्समाख्यातं लोके जन्माष्टमीव्रतम् ।।१५।।
बंगाल के चैतन्य महाप्रभु द्वारा संचारित गौड़ीय सम्प्रदाय के अनुयायी सन्तों की मान्यता है कि जिस समय कारागार में श्रीवसुदेव-देवकी के सम्मुख चतुर्भुजरूप में भगवान् प्रकट हुए थे, उसी समय नन्दबाबा के घर पर भी यशोदानन्दन के रूप में द्विभुजरूप में भगवान प्रकट हुए थे।
एक: कृष्णो द्विधाभूतो मुमुक्षुभजनैषिणो:। उपकाराय शुद्धात्मा वेदविद्भि: स गीयते। मुक्तोब्रृह्मपदंयाति तदंगं ज्योतिरुत्तमम्।।८/२६ ख –८/२७ क।(कृष्ण यामल तन्त्र)
और यशोदा माता ने जुड़वाँ रूप में दो सन्तानों को जन्म दिया था पुत्र का नाम गोविन्द और पुत्री का नाम अम्बिका था।
नन्दपत्न्यां यशोदायां मिथुनं सञ्जायत: । गोविन्दाख्यः पुमान् कन्या साम्बिका च मथुरां गता ।।५।
(कृष्ण यामल तन्त्र)
विदित हो कि भगवान का द्विभुजधारी गोप रूप गोलोक का शाश्वत रूप है। जबकि चतुर्भुज रूप वैकुण्ठ वासी विष्णु रूप है। इसी लिए भगवान पृथ्वी पर गोपों के यहाँ ही गोप रूप में अवतरण करते हैं।
वे नन्द के पुत्र रूप में भी जन्म लेते हैं और वसुदेव के पुत्र रूप में भी जन्म लेते है।
श्रीमद्भागवत, दशमस्कन्ध के पञ्चम अध्याय के प्रथम श्लोक में वर्णन आया है--
नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्नादो महामनाः।
- जब नन्द के पुत्र का जन्म हुआ। यहाँ आत्मज शब्द नन्द और कृष्ण के रक्त व आनुवांशिक सम्बन्ध को सूचित करता है।
- जाताह्लादो महामनाःमहान मन वाले नन्द आनन्दित हुए।
- आहूय विप्रान् वेदज्ञान्:उन्होंने वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर।
- स्नातः शुचिरलङ्कृतः:उन्होंने स्नान किया, शुद्ध हुए और अलंकार धारण किए।
- नन्द ने तत्पश्चात विधिवत जातकर्मादि संस्कार करवाए और पितृ-देवताओं का पूजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को अलंकरणों से युक्त दस लाख गायें और सात रत्न तथा रेशमी वस्त्रों से युक्त तिलाद्रि (तिलों से भरे पर्वत) दान किए।
श्रीनन्दजी के आत्मज स्वयं से उत्पन्न (पुत्र) होने पर उन महामना को परमाह्लाद हुआ।'
श्रीनन्दजी के यहाँ भगवान् पुत्ररूप में जन्म न लेते तो शुकदेव जी 'आत्मज उत्पन्ने' पुत्र पैदा हुआ पद न कहकर 'स्वात्मजं मत्वा' ' अपना पुत्र मानकर ' वाक्यपद कहते। जो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। अत: व्याकरण की दृष्टि से भी कृष्ण गोविन्द नाम से नन्द के पुत्र हैं।
*********
कृष्ण यामल तन्त्र नामक ग्रन्थ में वर्णन है कि नन्द की पत्नी यशोदा के जुड़वां सन्तानें हुई एक लड़का हुआ और एक लड़की । लड़के का नाम गोविन्द और लड़की का नाम अम्बिका रखा गया जो मथुरा को चली गयी।५।
नन्दपत्न्यां यशोदायां मिथुनं सञ्जायत: । गोविन्दाख्यः पुमान् कन्या साम्बिका च मथुरां गता ।।५।
(कृष्ण यामल तन्त्र)
इतना ही नहीं विष्णु यामल में वर्णन है कि वसुदेव द्वारा ले जाए ग॒ए वासुदेव कृष्ण निश्चय ही नन्द पुत्र की आत्मा में विलीन हो गयी जैसे मेघों में बिजली समा जाती है।
वसुदेव: समानीतो वासुदेवोऽखिलात्मनि लीनो नन्दसुते राजन् ! घने सौदामिनी यथा।।६।
अनुवाद:-वसुदेव द्वारा लाये गये वासुदेव श्रीकृष्ण स्वयं नन्द पुत्र में लीन हो गये जैसे बिजली मेघों में विलीन हो जाती है।६।
(विष्णु यामल-तत्र)
इन महानुभावों का कहना है कि श्रीवसुदेव-देवकी की भक्ति ऐश्वर्यमिश्रित वात्सल्यमयी थी और श्रीनन्दयशोदा की भक्ति ऐश्वर्यगन्धशून्य विशुद्ध वात्सल्यमयी।
इसी से वसुदेव-देवकी के सामने भगवान् शंख-चक्र-गदापद्मधारी चतुर्भुज अद्भुत बालक के रूप में आविर्भूत हुए। भगवान् के इस ऐश्वर्यमय रूप को देखकर उन्होंने समझा कि श्रीभगवान् नारायण हमारे पुत्ररूप में प्रकट हुए हैं; अतएव उन्होंने हाथ जोड़कर इनकी स्तुति की और भगवान ने भी पूर्व-जन्मों की स्मृति दिलाकर अपने साक्षात् भगवान् होने का परिचय दिया।
इसमें ऐश्वर्य प्रत्यक्ष है। तदनन्तर वात्सल्य-भाव का उदय होनेपर कंस के भयसे उन्होंने भगवान्से बार-बार चतुर्भुजरूप को छिपाकर द्विभुज साधारण शिशु बनने के लिये अनुरोध किया।
इससे यह सिद्ध है कि श्रीवसुदेव-देवकी का वात्सल्य-प्रेम-ऐश्वर्यमिश्रित था और भगवान् का ऐश्वर्यमय चतुर्भुजरूप ही उनका आराध्य था तथा वे उसको पुत्ररूप में प्राप्त करना तथा देखना चाहते थे।
परन्तु इसके विपरीत श्रीनन्द-यशोदा का वात्सल्य-प्रेम विशुद्ध था, उसमें ऐश्वर्य-ज्ञान का तनिक भी सम्बन्ध नहीं था; इससे उनके सामने भगवान् द्विभुज प्राकृत बालक के रूप में ही आविर्भूत हुए और उन्होंने कोई स्तुति-प्रार्थना भी नहीं की। यह द्विभुज रूप ही गोलोक का गोप रूप है। इसी रूप को
पुत्र समझकर गोद में उठा लिया और नवजात बालक के कल्याणार्थ जातकर्मादि करवाये।
***
नन्दपत्नयां यशोदायां मिथुन: समपद्यत:। गोविन्दाख्यः पुमान् कन्या साम्बिका मथुरां गता॥
यह प्रसिद्ध ही है कि भगवान् उसी रूप में भक्त के सामने प्रकट होते हैं, जो रूप भक्त के मन में होता है। श्रीभागवत में श्रीब्रह्माजी ने कहा है--
त्वं भक्तियोगपरिभावितहृत्सरोज ।
आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम् ।
यद् यद् धिया ते उरुगाय विभावयन्ति ।
तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥११॥
(भागवतपुराण-३/९/११)
भगवन् ! आपके भक्त जिस स्वरूप की निरन्तर भावना करते हैं, आप आप उसी रूप में प्रकट होकर भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं।'
श्रीमद्भागवत में जो यह स्पष्ट वर्णन नहीं आया है--इसका कारण यह बताया जाता है कि श्रीशुकदेवजी भक्तराज परीक्षित् को कथा सुना रहे थे। परीक्षित् का सम्बन्ध वसुदेवजी से था। अतः उन्हें विशेष आनन्द देने के लिये शुकदेवजी ने नन्दालय में भी भगवान् के प्रकट होने का स्पष्ट वर्णन नहीं किया; परन्तु उनका प्रेमपूर्ण हृदय माना नहीं और इस श्लोक में उनके श्रीमुखसे “नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने ' के रूप में रहस्य प्रकट हो ही गया।
श्रीमद्भागवतमें और भी संकेत है--कंस ने जब गोकुल से लायी हुई यशोदा की कन्या को देवकी की कन्या समझकर उसे मारने के लिये शिलापर पटकना चाहा, तब वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गयी और देवीरूप से प्रकट हुई । उस समय भागवत में उसके लिये 'अदृश्यतानुजा विष्णो: ' अर्थात् 'कंस ने भगवान्की अनुजा (छोटी बहिन)-को देखा '-यों लिखा है। पर यदि भगवान् श्रीकृष्ण केवल श्रीदेवकी के पुत्र होते तो यशोदा की कन्या को भगवान् की 'अनुजा' कहना युक्तियुक्त तथा सत्य न होता किन्तु परमानन्दघनविग्रह भक्तवाञ्छाकल्पत भक्तवाञ्छाकल्पतरु श्रीभगवान् जिस समय कंस-कारागार में वसुदेव-आत्मजरूप में प्रकट हुए थे, ठीक उसी समय गोकुल में नन्दात्मज के रूप में भी वही भगवान् प्रकट हुए थे तथा उसी के थोड़ी देर बाद योगमाया कन्या के रूप में प्रकट हुई थीं।
___________________
श्रीहरिवंश में आया है-
गर्भकाले त्वसम्पूर्णे अष्टमे मासि ते स्त्रियौ। देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तदा ।११।
हरिवंशपुराण विष्णुपर्व अध्याय (4)
अर्थात् गर्भकाल पूरा होने के पहले ही आठवें महीने में 'देवकी और यशोदा दोनों ने एक ही साथ प्रसव किया था।'
इस तथ्य पर यह कहा जा सकता है कि “जिस समय देवकी जी के भगवान् पुत्ररूप में प्रकट हुए, उसी समय यशोदाजी के योगमाया प्रकट हुईं।'
पर ऐसा कहना बनता नहीं; क्योंकि श्रीमद्भागवत (१०। ३। ४७) -में यह स्पष्ट उल्लेख है कि “' श्रीभगवान् से प्रेरित वसुदेवजी ने पुत्र को गोद में लेकर कारागार से बाहर निकलने की इच्छा की, उस समय “योगमाया ' प्रकट हुईं।'
अतएव कारागार में भगवान का और गोकुल में योगमाया का प्राकट्य आगे-पीछे हुआ, एक ही समय नहीं हुआ था। इस तथ्य पर भी यह कहा जा सकता है कि गोकुलमें ' भगवान् प्रकट हुए ! इसमें स्पष्ट प्रमाण क्या है ? तो इसके समाधान में ' श्रीकृष्णयामल तन्त्र' नामक ग्रन्थ का कहना है कि नन्द पत्नी यशोदा के यमज( जुड़वाँ) संतान हुई थी; पहले एक पुत्र हुआ, तदनन्तर एक कन्या हुई पुत्र साक्षात् श्रीगोविन्द थे और कन्या थी स्वयं अम्बिका (योगमाया)।
यशोदा की इस कन्या को ही वसुदेवजी मथुरा ले गये थे-
इस स्पष्टोक्ति से योगमायाको 'श्रीकृष्ण की अनुजा'(छोटी बहिन) कहा जाना भी सार्थक हो गया।
इस विषय पर फिर कहा जा सकता है--' श्रीवसुदेव जी जब शिशु श्रीकृष्ण को लेकर गोकुल गये, तब वहाँ उन्हें केवल शिशु बालिका ही क्यों दिखायी दी, बालक क्यों नहीं दिखायी दिया ? और बालक भी था तो फिर वह बालक कहाँ गया ? वहाँ दो बालक होने चाहिये।'
इस शंका का समाधान यह है कि इनके वहाँ पहुँचते ही उसी क्षण इन वसुदेव बालक उस नन्दबालक में विलीन हो गया। इन्हें पता ही नहीं लगा कि वहाँ कोई बालक और भी था। वरिष्ठ महानुभावों ने यहाँ तक माना है कि जिस समय कंस के कारागार में देवकी ने यह प्रबल इच्छा की कि श्रीभगवान् के चतुर्भुजरूप का गोपन हो जाय, उसी समय यशोदा हृदयस्थ भगवान् का द्विभुज बालकरूप उस चतुर्भुजरूप को छिपाकर देवकी के सामने आविर्भूत हो गया (यदा स्वाविर्भूतचतुर्भुजरूपाच्छादनाय श्रीदेवकीच्छाजायत, तदा यशोदाहदयस्थद्विभुजरूपस्य तद्रूपाच्छादनपूर्वकाविर्भावस्तत्रासीदिति गम्यते--'वैष्णवतोषिणी')।
यशोदा के यहाँ प्रकट भगवान् वहाँ से तुरन्त यहाँ आकर प्रकट हो गये और उनमें भगवान् का शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुजरूप तुरन्त वैसे ही विलीन हो गया, जैसे बादल में बिजली विलीन हो जाती है-
वसुदेवसुतः श्रीमान् वासुदेवोऽखिलात्मनि। लीनो नन्दसुते राजन ! घने सौदामनी यथा॥ 6। (श्रीकृष्णयामल तन्त्र )
देवक्यां देवरूपिण्यां. विष्णु: सर्वगुहाशयः। आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः॥ भागवत पुराण-(१०। ३। ८)
यहाँ 'देवकी' शब्द 'देहली-दीपक' न्याय से श्रीदेवकीजी और श्रीयशोदाजी दोनोंका ही वाचक है; क्योंकि यशोदाजीका भी दूसरा नाम 'देवकी' था।
श्रीहरिवंशपुराण में आया है-
द्वे नाम्नी नन्दभार्याया यशोदा देवकीति च। अतः सख्यमभूत्तस्या देवक्या शौरिजायया॥अनुवाद:-“नन्दभार्या यशोदा के यशोदा और देवकी-दो नाम थे, इसीलिये उनका नामसाम्य के कारण वसुदेव-पत्नी देवकी से सख्यभाव था।'
इस वाक्य से भी यह कहा जा सकता है कि सांकेतिक भाषा में श्रीशुकदेवजीने दोनों जगह भगवान् के प्राकट्य की बात कह दी। एक अस्पष्ट संकेत और भी है-
यशोदा नन्दपत्नी च जातं॑ परमबुध्यत। न तल्लिड्रं परिश्रान्तना निद्रयापगतस्मृतिः॥
(श्रीमद्भागवत पुराण- १०। ३। ५३)
नन्दपत्नी यशोदा को यह तो ज्ञात हुआ कि संतान हुई है; परंतु श्रम और निद्रा (भगवत्प्रेरित स्वजनमोहिनी माया)-के कारण अचेत होने से वे यह न जान सकीं कि पुत्र है या कन्या! इससे भी नन्दालय में भगवान् के प्राकट्य का संकेत है। महानुभावों का कहना है कि भगवान् के दो रूप हैं--'ऐश्वर्य सम्पन्न' और 'ब्राह्म सम्पन्न। 'ऐश्वर्य' मायायुक्त है और “ब्राह्म' स्वरूप मायातीत है। अचिन्त्यानन्त-अतुलनीय-कल्याण-गुणगणसम्पन्न स्वमायाविशिष्ट ' ऐश्वर्य' रूप के द्वारा इस विश्वब्रह्माण्ड का सृजन-पालन आदि होता है। भगवान्का शुद्ध ब्रह्मस्वरूप उत्पादन-पालनादि लीलाओं से रहित, केवल आनन्दप्रेममय है। अत: वसुदेवजी के यहाँ जिस रूप का प्राकट्य हुआ था, वह “ऐश्वर्य"' रूप था और “नन्दात्मज' रूप से ब्रह्मस्वरूप गोलोक रूप से भगवान् अवतरित हुए थे। श्रीवसुदेवजीके यहाँ आविर्भूत 'ऐश्वर्य ' रूप और नन्दात्मज ब्राह्मस्वरूप में ब्राह्मस्वरूप गोपनरूप से गोपांगनाओं के साथ ब्रजमण्डल में रह गया। यही “वृन्दावन परित्यज्य पादमेक॑ न गच्छति' का रहस्य है।
यद्यपि श्रीभागवतमें इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है तथा यह क्लिष्ट कल्पना-सी भी है, तथापि महानुभावोंके उपर्युक्त विवेचनके अनुसार श्रीभगवान् “नन्दात्मज' रूपमें भी अवतीर्ण हुए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
भारत के विभिन्न राज्यों में श्रीकृष्ण के नाम-
कृष्ण की आमतौर पर पूजा इस प्रकार की जाती है:
- कन्हैय्या/ बांकेबिहारी /ठाकुरजी/कान्हा/कुंजबिहारी/ राधा रमण / राधावल्लभ /किसना/किशन : उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश
- जगन्नाथ : ओडिशा
- विठोबा : महाराष्ट्र
- श्रीनाथजी : राजस्थान
- गुरुवायूरप्पन / कन्नन : केरल
- द्वारकाधीश /रणछोड़ : गुजरात
- मायोन/पार्थसारथी/कन्नन : तमिलनाडु
- कृष्णय्या: कर्नाटक
ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत-
कृष्ण की परंपरा प्राचीन भारत के कई स्वतंत्र देवताओं का एक समामेलन प्रतीत होती है, जिनमें से सबसे पहले वासुदेव को प्रमाणित किया गया है । वासुदेव वृष्णि जनजाति के एक नायक-देवता थे , जो वृष्णि नायकों से संबंधित थे , जिनकी पूजा 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पाणिनी के लेखन में और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से हेलियोडोरस के साथ पुरालेख में प्रमाणित है। स्तम्भ ] एक समय में, ऐसा माना जाता है कि वृष्णियों की जनजाति यादवों/अभीरों की जनजाति के साथ मिल गई थी, जिनके अपने नायक-देवता का नाम कृष्ण था। वासुदेव और कृष्ण मिलकर एक देवता बन गए, जो इसमें प्रकट होता है महाभारत , और उन्हें महाभारत और भगवद गीता में विष्णु के साथ पहचाना जाने लगा। चौथी शताब्दी ईस्वी के आसपास, एक अन्य परंपरा, मवेशियों के रक्षक, आभीरों के गोपाल-कृष्ण का पंथ
प्रारम्म्भिक पुरालेखीय स्रोत
सिक्के पर चित्रण (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व)

180 ईसा पूर्व के आसपास, इंडो-ग्रीक राजा अगाथोकल्स ने देवताओं की छवियों वाले कुछ सिक्के ( अफगानिस्तान के ऐ-खानौम में खोजे गए) जारी किए थे, जिन्हें अब भारत में वैष्णव कल्पना से संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवता संकर्षण प्रतीत होते हैं - गदा गदा और हल के गुणों वाले बलराम , और शंख (शंख) और सुदर्शन चक्र के गुणों वाले वासुदेव-कृष्ण। बोपराची के अनुसार, देवता के शीर्ष पर स्थित शिरस्त्राण वास्तव में शीर्ष पर अर्ध-चंद्र छत्र ( छत्र ) के साथ एक शाफ्ट का गलत चित्रण है।
शिलालेख

हेलियोडोरस स्तंभ , ब्राह्मी लिपि शिलालेख वाला एक पत्थर का स्तंभ, बेसनगर ( विदिशा , मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश ) में औपनिवेशिक युग के पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया था। शिलालेख के आंतरिक साक्ष्य के आधार पर, यह 125 और 100 ईसा पूर्व के बीच का बताया गया है और अब इसे हेलियोडोरस के नाम से जाना जाता है - एक इंडो-ग्रीक जिसने एक क्षेत्रीय भारतीय राजा, काशीपुत्र भागभद्र के लिए ग्रीक राजा एंटियालसिडास के राजदूत के रूप में कार्य किया था । हेलियोडोरस स्तंभ शिलालेख " वासुदेव" को हेलियोडोरस का एक निजी धार्मिक समर्पण है", एक प्रारंभिक देवता और भारतीय परंपरा में कृष्ण का दूसरा नाम। इसमें कहा गया है कि स्तंभ का निर्माण " भगवत हेलियोडोरस" द्वारा किया गया था और यह एक " गरुड़ स्तंभ" है (दोनों विष्णु-कृष्ण-संबंधित शब्द हैं)। इसके अतिरिक्त, शिलालेख में महाभारत के अध्याय 11.7 से एक कृष्ण-संबंधित श्लोक शामिल है जिसमें कहा गया है कि अमरता और स्वर्ग का मार्ग सही ढंग से तीन गुणों का जीवन जीना है: आत्म- संयम ( दमः ), उदारता ( कागः या त्याग ), और सतर्कता ( प्रमादः) ) पुरातत्वविदों द्वारा 1960 के दशक में हेलियोडोरस स्तंभ स्थल की पूरी तरह से खुदाई की गई थी। इस प्रयास से एक गर्भगृह, मंडप और सात अतिरिक्त स्तंभों के साथ एक बहुत बड़े प्राचीन अण्डाकार मंदिर परिसर की ईंट की नींव का पता चला । हेलियोडोरस स्तंभ शिलालेख और मंदिर प्राचीन भारत में कृष्ण-वासुदेव भक्ति और वैष्णववाद के सबसे पहले ज्ञात साक्ष्यों में से हैं।

हेलियोडोरस शिलालेख पृथक साक्ष्य नहीं है। हाथीबाड़ा घोसुंडी शिलालेख , जो राजस्थान राज्य में स्थित हैं और आधुनिक पद्धति द्वारा पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, संकर्षण और वासुदेव का उल्लेख करते हैं, यह भी उल्लेख करते हैं कि संरचना सर्वोच्च देवता नारायण के सहयोग से उनकी पूजा के लिए बनाई गई थी । ये चार शिलालेख सबसे पुराने ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से कुछ होने के कारण उल्लेखनीय हैं।
उत्तर प्रदेश के मथुरा-वृंदावन पुरातात्विक स्थल पर पाए गए एक मोरा पत्थर के स्लैब पर , जो अब मथुरा संग्रहालय में रखा गया है , उस पर ब्राह्मी शिलालेख है। यह पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व का है और इसमें पांच वृष्णि नायकों का उल्लेख है , जिन्हें संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न , अनिरुद्ध और साम्ब के नाम से जाना जाता है ।
वासुदेव के लिए शिलालेखीय रिकॉर्ड दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अगाथोकल्स और हेलियोडोरस स्तंभ के सिक्के के साथ शुरू होता है, लेकिन कृष्ण का नाम पुरालेख में बाद में दिखाई देता है। अफगानिस्तान की सीमा के पास, उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में पहली शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्द्ध के चिलास II
पुरातात्विक स्थल पर , पास में कई बौद्ध छवियों के साथ, दो पुरुष उत्कीर्ण हैं। दोनों पुरुषों में से बड़े ने अपने दोनों हाथों में हल और गदा पकड़ रखी थी।
कलाकृति के साथ खरोष्ठी लिपि में एक शिलालेख भी है, जिसे विद्वानों ने राम-कृष्ण के रूप में परिभाषित किया है , और दो भाइयों, बलराम और कृष्ण के एक प्राचीन चित्रण के रूप में व्याख्या की गई है।
"The first known depiction of the life of Krishna himself comes relatively late, with a relief found in Mathura, and dated to the 1st–2nd century CE. This fragment seems to show Vasudeva, Krishna's father, carrying baby Krishna in a basket across the Yamuna. The relief shows at one end a seven-hooded Naga crossing a river, where a makara crocodile is thrashing around, and at the other end a person seemingly holding a basket over his head.
Gita

एक व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण के विस्तृत विवरण वाला सबसे पहला ग्रंथ महाकाव्य महाभारत है , जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। कृष्ण महाकाव्य की कई मुख्य कहानियों के केंद्र में हैं। महाकाव्य की छठी पुस्तक ( भीष्म पर्व ) के अठारह अध्याय जो भगवद गीता का निर्माण करते हैं, उनमें युद्ध के मैदान पर अर्जुन को कृष्ण की सलाह शामिल है ।
हरिवंश पुराण भी महाभारत का खिलभाग है। जिसमें कृष्ण के आभीर( गोप ) जाति में जन्म लेने का वर्णन है।
प्राचीन काल में जब भगवद गीता की रचना की गई थी, तब कृष्ण को व्यापक रूप से एक व्यक्तिगत देवता के बजाय विष्णु के अवतार के रूप में देखा जाता था, फिर भी वह बेहद शक्तिशाली थे और विष्णु के अलावा ब्रह्मांड में लगभग सभी चीजें "किसी न किसी तरह कृष्ण के शरीर में मौजूद थीं" "
हरिवंश पुराण जो , महाभारत के बाद के परिशिष्ट में , कृष्ण के बचपन और युवावस्था का विस्तृत संस्करण शामिल है।
अन्य स्रोत

छान्दोग्य उपनिषद , जिसकी रचना ईसा पूर्व 8वीं और 6वीं शताब्दी के बीच हुई मानी जाती है, प्राचीन भारत में कृष्ण के संबंध में अटकलों का एक अन्य स्रोत रहा है।
छान्दोग्योपनिषद-श्लोक (III.xvii.6) में कृष्णाय देवकीपुत्राय में कृष्ण का उल्लेख अंगिरसा परिवार के ऋषि घोर के छात्र के रूप में किया गया है। कुछ विद्वानों द्वारा घोरा की पहचान जैन धर्म के बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ से की जाती है । यह वाक्यांश, जिसका अर्थ है " देवकी के पुत्र कृष्ण के लिए", मैक्स मुलर जैसे विद्वानों द्वारा कृष्ण के बारे में दंतकथाओं और वैदिक विद्या के संभावित स्रोत के रूप में उल्लेख किया गया है।
यास्क का निरुक्त , छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास एक व्युत्पत्ति शास्त्रीय शब्दकोश प्रकाशित हुआ है, जिसमें अक्रूर के पास मौजूद श्यामंतक रत्न का संदर्भ है , जो कृष्ण के बारे में प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं का एक रूप है। शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय-आरण्यक कृष्ण अपने वृषि उत्पत्ति से बेकार हैं।
प्राचीन वैयाकरण पाणिनि (संभवतः 5 वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे ) द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में , वासुदेव और अर्जुन को , पूजा के प्राप्तकर्ता के रूप में, एक ही सूत्र में एक साथ सन्दर्भित किया गया है ।

मेगस्थनीज , एक यूनानी नृवंशविज्ञानी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम के राजदूत, ने अपने प्रसिद्ध काम इंडिका में हेराक्लीज़ का संदर्भ दिया था । यह पाठ अब इतिहास में खो गया है, लेकिन बाद के यूनानियों जैसे एरियन , डायोडोरस और स्ट्रैबो द्वारा माध्यमिक साहित्य में उद्धृत किया गया था । इन ग्रंथों के अनुसार, मेगस्थनीज ने उल्लेख किया है कि भारत की सौरसेनोई जनजाति, जो हेराक्लीज़ की पूजा करती थी, के पास मेथोरा और क्लेइसोबोरा नाम के दो प्रमुख शहर थे, और जोबारेस नाम की एक नौगम्य नदी थी। एडविन ब्रायंट के अनुसार भारतीय धर्मों के एक प्रोफेसर, जो कृष्ण पर अपने प्रकाशनों के लिए जाने जाते हैं, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि सौरसेनोई यदु वंश की एक शाखा, शूरसेनस को संदर्भित करता है, जिससे कृष्ण संबंधित थे"। ब्रायंट का कहना है कि हेराक्लीज़ शब्द संभवतः हरि-कृष्ण का ग्रीक ध्वन्यात्मक समकक्ष है, जैसे कि मथुरा का मेथोरा, कृष्णपुरा का क्लीसोबोरा और जमुना का जोबारेस । बाद में, जब सिकंदर महान ने उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में अपना अभियान शुरू किया, तो उसके सहयोगियों को याद आया कि पोरस के सैनिक हेराक्लीज़ की एक छवि ले जा रहे थे।
बौद्ध पाली सिद्धान्त और घट-जातक (नंबर 454) में वासुदेव और बलदेव के भक्तों का विवादास्पद उल्लेख है। इन ग्रंथों में कई विशिष्टताएँ हैं और ये कृष्ण कथाओं का विकृत और भ्रमित संस्करण हो सकते हैं।
जैन धर्म के ग्रंथों में भी तीर्थंकरों के बारे में अपनी किंवदंतियों में, कई विशिष्टताओं और विभिन्न संस्करणों के साथ, इन कहानियों का उल्लेख किया गया है । प्राचीन बौद्ध और जैन साहित्य में कृष्ण से संबंधित किंवदंतियों के इस समावेश से पता चलता है कि प्राचीन भारत की गैर-हिंदू परंपराओं द्वारा देखे गए धार्मिक परिदृश्य में कृष्ण धर्मशास्त्र अस्तित्व में था और महत्वपूर्ण था ।
थेरवाद (बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा में पाली ग्रन्थों में वासुदेव शब्द है।
घट जातक (संख्या 454) में बताया गया है कि जब वसुदेव के पुत्र की मृत्यु हो गई और वसुदेव निराशा में डूब गए, तो उनके भाई घटपंडित ने पागलपन का नाटक करके उन्हें होश में लाया।
वासुदेव के मंत्री रोहिणीय थे। वासुदेव को (जि.4.84; जि.6.421 में उन्हें कन्ह कहा गया है) कान्हा और फिर केशव कहकर संबोधित किया गया है। विद्वान बताते हैं (जि.4.84) कि उन्हें कन्ह्यानगोत्त के होने के कारण कन्ह्या कहा जाता था, और केशव इसलिए क्योंकि उनके केश सुंदर थे (केशसोभानतय)। हालाँकि, ये नाम इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं (देखें अंधकवेन्हुदासपुत्त, संख्या 1) कि वासुदेव की कथा कृष्ण की कथा से जुड़ी थी।
महाउम्मग्ग जातक (ज.वि.421) में वर्णित है कि राजा शिवि की माता जाम्बवती, वासुदेव कान्हा की पत्नी थीं। विद्वान इस वासुदेव की पहचान अंधकवेन्हुदासपुत्त के ज्येष्ठ पुत्र से करते हैं और कहते हैं कि जाम्बवती एक चण्डाली थीं। वासुदेव उनके अद्भुत सौंदर्य के कारण उन पर मोहित हो गए और उनकी जाति के विपरीत उनसे विवाह कर लिया। उनका पुत्र शिवि था, जो बाद में द्वारावती में अपने पिता के सिंहासन पर बैठा।
वासुदेव की पहचान सारिपुत्त से की जाती है। जे.iv.89.
वासुदेववत्तिका। संभवतः वासुदेव (कृष्ण) के अनुयायी; उनका उल्लेख बलदेववत्तिका और अन्य के साथ समानब्रह्मणवत्तशुद्धिका की सूची में किया गया है।
-जैन ग्रन्थों में श्रीकृष्ण-
वसुदेव कृष्ण के पिता हैं: श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों स्रोतों के अनुसार वे नौवें वासुदेव ("हिंसक नायक") हैं । चूँकि वे चक्रवर्ती (सार्वभौमिक सम्राट) की आधी शक्ति रखते हैं , इसलिए उन्हें अर्धचक्रीण भी कहा जाता है। जैन किंवदंतियों में ऐसे नौ वासुदेवों का वर्णन है जो आमतौर पर अपने "कोमल" जुड़वां बलदेवों के साथ प्रकट होते हैं। इन जुड़वां नायकों की किंवदंतियों में आमतौर पर उनके विरोधी समकक्ष प्रतिवासुदेव (प्रतिनायक) शामिल होते हैं।
राजा वासुदेव, रानी देवकी और उनके पुत्र कृष्ण की कहानियाँ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित ("तिरसठ महान व्यक्तियों का जीवन") जैसे ग्रंथों में वर्णित हैं , जो हेमचंद्र द्वारा बारहवीं शताब्दी में रचित श्वेताम्बर ग्रंथ है।
वासुदेव (वासुदेव) (या विष्णु, नारायण) नौ "नायकों" के समूह और विरोधी प्रतिवासुदेवों (या प्रतिविष्णु, प्रतिनारायण) के समकक्ष को संदर्भित करता है, जिसका उल्लेख श्वेतांबर और दिगंबर दोनों साहित्य में किया गया है। - प्रत्येक अर्ध काल चक्र में, बलभद्र (सौम्य नायक), वासुदेव (हिंसक नायक) और प्रतिवासुदेव (प्रतिनायक) के 9 समूह होते हैं। हिंदू पुराणों के विपरीत, जैन पुराणों में बलभद्र और नारायण नाम केवल बलराम और कृष्ण तक ही सीमित नहीं हैं। इसके बजाय वे शक्तिशाली सौतेले भाइयों के दो अलग-अलग वर्गों के नाम के रूप में कार्य करते हैं, जो जैन ब्रह्माण्ड विज्ञान के प्रत्येक अर्ध काल चक्र में नौ बार प्रकट होते हैं और संयुक्त रूप से आधे चक्रवर्ती के रूप में आधी पृथ्वी पर शासन करते हैं। अंततः नारायण द्वारा प्रतिनारायण को उसके अधर्म और अनैतिकता के कारण मार दिया जाता है।
प्राचीन संस्कृत व्याकरणविद् पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में बाद के भारतीय ग्रंथों में पाए जाने वाले कृष्ण और उनके सहयोगियों के कई संदर्भ दिए हैं। पाणिनि के श्लोक 3.1.26 पर अपनी टिप्पणी में, उन्होंने कंसवध या "कंस की हत्या" शब्द का भी उपयोग किया है , जो कृष्ण से जुड़ी किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
पुराणों
कई पुराण , ज्यादातर गुप्त काल (4-5वीं शताब्दी ईस्वी) के दौरान संकलित हैं जिनमें कृष्ण की जीवन कहानी या उसके कुछ मुख्य अंश बताये गये हैं। दो पुराणों, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी का सबसे विस्तृत वर्णन है, लेकिन भागवत और विष्णु पुराण की वर्तमान प्रतियों से बहुत से श्लोक निकालकर प्रक्षिप्त श्लोक संलग्न कर दिए गये हैं। और अन्य ग्रन्थों में कृष्ण की जीवन कहानियाँ अलग-अलग हैं, और उनमें महत्वपूर्ण विसंगतियाँ हैं। सम्भवत ये बाद में जोड़े गये प्रक्षिप्त अंश हैं।
[ आभीर जाति को यदि शब्द व्युत्पत्ति के हिसाब से देखा जाय तो- अभीर शब्द में 'अण्' तद्धित प्रत्यय करने पर आभीर समूह वाची रूप बनता है। अर्थात् आभीर शब्द अभीर शब्द का ही बहुवचन है। 'परन्तु परवर्ती संस्कृत कोश कारों नें आभीरों की गोपालन वृत्ति और उनकी वीरता प्रवृत्ति को दृष्टि-गत करते हुए अभीर और आभीर शब्दों की दो तरह से भिन्न-भिन्न व्युत्पत्तियाँ कर दीं। जैसे-
ईसा पूर्व पाँचवी सदी में कोशकार अमरसिंह ने अपने कोश अमरकोश में अहीरों की प्रवृत्ति वीरता (निडरता) को केन्द्रित करके आभीर शब्द की व्युत्पत्ति की है। नीचे देखें।
आ= समन्तात् + भी=भीयं (भयम्) + र= राति ददाति शत्रुणां हृत्सु = जो चारो तरफ से शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करता है वह आभीर कहलाता है।
किन्तु वहीं पर अमरसिंह के परवर्ती शब्द कोशकार- तारानाथ नें अपने ग्रन्थ वाचस्पत्यम् में अभीर- जाति की शब्द व्युत्पत्ति को उनकी वृत्ति यानी व्यवसाय के आधार पर गोपालन को केन्द्रित करके ही सुनिश्चित किया है। नींचे देखें।
"अभिमुखी कृत्य ईरयति गा- इति अभीर = जो सामने मुख करके चारो-ओर से गायें चराता है या उन्हें घेरता है।
अगर देखा जाय तो उपर्युक्त दोनों शब्दकोश में जो अभीर शब्द की व्युत्पत्ति को बताया गया है उनमें बहुत अन्तर नहीं है। क्योंकि एक नें अहीरों की वीरता मूलक प्रवृत्ति (aptitude ) को आधार मानकर शब्द व्युत्पत्ति को दर्शाया है तो वहीं दूसरे नें अहीर जाति को गोपालन वृत्ति अथवा (व्यवसाय) (profation) को आधार मानकर शब्द व्युत्पत्ति को दर्शाया है।
अहीर शब्द के लिए दूसरी जानकारी यह है कि- आभीर का तद्भव रूप आहीर होता है। अब यहाँ पर तद्भव और तत्सम शब्द को जानना आवश्यक हो जाता है। तो इस सम्बन्ध में सर्वविदित है कि - संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिन्दी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं।
ऐसे शब्द, जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिन्दी में आये हैं,वे 'तद्भव' कहलाते हैं। अर्थात- तद्भव शब्द का मतलब है, जो शब्द संस्कृत से आए हैं, लेकिन उनमें कुछ बदलाव के बाद हिन्दी में प्रयोग होने लगे हैं। जैसे आभीर संस्कृत का शब्द है, किन्तु कालान्तरण में बदलाव हुआ और आभीर शब्द हिन्दी में आहीर शब्द के रूप में प्रयुक्त होने लगा। ऐसे ही तद्भव शब्द के और भी
उदाहरण है जैसे- दूध, दही, अहीर, रतन, बरस, भगत, थन, घर इत्यादि।
किन्तु यहाँ पर हमें अहीर और आभीर, शब्द के बारे में ही विशेष जानकारी देना है कि इनका प्रयोग हिन्दी और संस्कृत ग्रन्थों में कब, कहाँ और कैसे एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है।
तो इस सम्बन्ध में सबसे पहले अहीर शब्द के विषय में जानेंगे कि हिन्दी ग्रन्थों में इसका प्रयोग कब और कैसे हुआ। इसके बाद संस्कृत ग्रन्थों में जानेंगे कि आभीर शब्द का प्रयोग गोप, अहीर और यादवों के लिए कहाँ-कहाँ प्रयुक्त हुआ।
अहीर शब्द का प्रयोग हिन्दी पद्य साहित्यों में कवियों द्वारा बहुतायत रुप से किया गया है। जैसे-
अहीर शब्द का रसखान कवि अपनी रचनाओं में खूब प्रयोग किए हैं-
"सेष, गनेस, महेस, दिनेस, सुरेसहु जाहि निरंतर गावैं।
जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावैं।
नारद से सुक ब्यास रहैं पचि हारे तऊ पुनि पार न पावैं।
ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भरि छाछ पै नाच नचावैं।।8।।
इसी ग्रन्थ "सुजानरसखान" में अन्यत्र भी रसखान श्रीकृष्ण को अहीर लिखते हैं ।
देस बदेस के देखे नरेसन रीझ की कोऊ न बूझ करैगो।
तातें तिन्हैं तजि जानि गिरयौ गुन सौगुन गाँठि परैगो।
बाँसुरीबारो बड़ो रिझवार है स्याम जु नैसुक ढार ढरैगौ।
लाड़लौ छैल वही तौ अहीर को पीर हमारे हिये की हरैगौ।।18।
बाँकी धरै कलगी सिर ऊपर बाँसुरी-तान कटै रस बीर के।
कुंडल कान लसैं रसखानि विलोकन तीर अनंग तुनीर के।
डारि ठगौरी गयौ चित चोरि लिए है सबैं सुख सोखि सरीर के।
जात चलावन मो अबला यह कौन कला है भला वे अहीर के।।88।।
_____
इसी तरह से भगवान श्रीकृष्ण की श्रद्धा में सदैव लीन रहने वाले कवि इशरदास रोहडिया (चारण), जिनका जन्म विक्रम संवत- (1515) में राजस्थान के भादरेस गांँव में हुआ था। जिन्होंने (500) साल पहले दो ग्रन्थ "हरिरस" और "देवयान" लिखे। जिसमें ईशरदासजी द्वारा रचित "हरिरस" के एक दोहे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कृष्ण भगवान का जन्म अहीर (यादव) कुल में हुआ था।
नारायण नारायणा! तारण तरण अहीर। हूँ चारण हरिगुण चवां, सागर भरियो क्षीर।। ५८।
अर्थात् - अहीर जाति में अवतार लेने वाले हे नारायण (श्रीकृष्ण) ! आप जगत के तारण तरण (उद्धारक) हो, मैं चारण आप श्रीहरि के गुणों का वर्णन करता हूँ, जो कि सागर गुणों के क्षीर से भरा हुआ है।५८।
और श्रीकृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी ने भी श्रीकृष्ण को अहीर कहते हुए उनका स्तवन किया है। सूरसागर के दशमस्कन्ध-(पृष्ठ ४७९) में लिखा है-
चातकी बूंद भई हो हेरत हेरत रही हिराइ ।८१॥जैतश्री॥
सखीरी काके मीत अहीर । काहे को भरि भरि ढारति हो इन नैन राह के नीर।।
आपुन पियत पियावत दुहि दुहिं इन धेनुनके क्षीर। निशि वासर छिन नहिं विसरतहै जो यमुना के तीर।। ॥
मेरे हियरे दौं लागति है जारत तनु की चीर । सूरदास प्रभु दुखित जानिकै छांडि गए वे पीर ।।८२॥
सूरसागर.पृष्ठ/
(४७९)
दशमस्कन्ध-१०
ये उपर्युक्त सभी उदाहरण श्रीकृष्ण के अहीर जाति का होने के हैं जो हिन्दी साहित्यिक ग्रन्थों में प्रयुक्त हुए सन्दर्भ प्रस्तुत करते हैं। अब हम लोग आभीर शब्द को जानेंगे जो प्राकृत भाषा के आहीर का तत्सम रूप है, वह संस्कृत ग्रन्थों में कहाँ-कहाँ प्रयुक्त हुआ हैं। इसके साथ ही आभीर (अहीर) शब्द के पर्यायवाची शब्द - गोप, गोपाल और यादव को भी जानेंगे कि पौराणिक ग्रन्थों में अभीर के ही अर्थ में कैसे प्रयुक्त हुए हैं।
सबसे पहले हम गर्गसंहिता के विश्वजितखण्ड के अध्याय -(७) के श्लोक संख्या- (१४) को लेते हैं जिसमें में भगवान श्रीकृष्ण और नन्दबाबा सहित पूरे अहीर समाज के लिए आभीर शब्द का प्रयोग शिशुपाल उस समय करता है जब सन्धि का प्रस्ताव लेकर उद्धव जी शिशुपाल के यहाँ जाते हैं। किन्तु वह प्रस्ताव को ठुकराते हुए उद्धव जी से श्रीकृष्ण के बारे में कहता है कि-
आभीरस्यापि नन्दस्य पूर्वं पुत्रः प्रकीर्तितः।वसुदेवो मन्यते तं मत्पुत्तोऽयं गतत्रपः।।१४।
प्रद्युम्नं तस्तुतं जित्वा सबलं यादवैः सह।कुशस्थलीं गमिश्यामि महीं कर्तुमयादवीम्।। १६।
अनुवाद -
• वह (श्रीकृष्ण) पहले नन्द नामक अहीर का भी बेटा कहा जाता था। उसी को वसुदेव लाज- हया छोड़कर अपना पुत्र मानने लगे हैं।१४।
• मैं उसके पुत्र प्रद्युम्न को यादवों तथा सेना सहित जीत कर भूमण्डल को यादवों से शून्य कर देने के लिए कुशस्थली पर चढ़ाई करूँगा।१६।
उपर्युक्त दोनो श्लोक को यदि देखा जाए तो इसमें भगवान श्रीकृष्ण सहित सम्पूर्ण अहीर अथवा यादव समाज के लिए ही आभीर शब्द का प्रयोग किया गया है किसी अन्य के लिए नहीं।
इसी तरह से आभीर शूरमाओं का वर्णन महाभारत के द्रोणपर्व के अध्याय- (२०) के श्लोक - (६) और (७) में मिलता है जो शूरसेन देश से सम्बन्धित थे।
भूतशर्मा क्षेमशर्मा करकाक्षश्च वीर्यवान्।कलिङ्गाः सिंहलाः प्राच्याः शूराभीरा दशेरकाः।।६।
यवनकाम्भोजास्तथा हंसपथाश्च ये। शूरसेनाश्च दरन्दा मद्रकेकयाः।।७।
अर्थ:- भूतशर्मा , क्षेमशर्मा पराक्रमी कारकाश , कलिंग सिंहल पराच्य (शूर के वंशज शूरवीर आभीर) और दशेरक।६।
अनुवाद - शक यवन ,काम्बोज, हंस -पथ नाम वाले देशों के निवासी और शूरसेन प्रदेश के अभीर (अहीर) दरद, मद्र, केकय ,तथा एवं हाथी सवार घुड़सवार रथी और पैदल सैनिकों के समूह उत्तम कवच धारण करने उस व्यूह के गरुड़ ग्रीवा भाग में खड़े थे।६-७।
इसी तरह से विष्णुपुराण द्वित्तीयाँश के तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या- (१६-१७ और १८ ) में अन्य जातियों के साथ-साथ शूर आभीरों का भी वर्णन मिलता है-
"तथापरान्ताः ग्रीवायांसौराष्ट्राः शूराभीरास्तथार्ब्बुदाः। कारूषा माल्यवांश्चैव पारिपात्रनिवासिनः ।१६।
सौवीरा-सैन्धवा हूणाः शाल्वाः शाकलवासिनः। मद्रारामास्तथाम्बष्ठाः पारसीकादयस्तथा ।१७।
आसां पिबन्ति सलिलं वसन्ति सरितां सदा ।समीपतो महाभागा हृष्टपुष्टजनाकुलाः ।। १८।
अनुवाद - पुण्ड्र, कलिंग, मगध, और दाक्षिणात्य लोग, अपरान्त देशवासी, सौराष्ट्रगण, शूर आभीर और अर्बुदगण, कारूष,मालव और पारियात्रनिवासी, सौवीर, सैन्धव, हूण, साल्व, और कोशल देश वासी तथा माद्र,आराम, अम्बष्ठ, और पारसी गण रहते हैं।१७-१७।
हे महाभाग ! वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। उनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हृष्ट-पुष्ट रहते हैं।१८।
▪ इसी तरह से महाभारत के उद्योगपर्व के सेनोद्योग नामक उपपर्व के सप्तम अध्याय में श्लोक संख्या- (१८) और (१९) पर गोपों (अहीरों) को अजेय योद्धा के रूप में वर्णन है-
"मत्सहननं तुल्यानां ,गोपानाम् अर्बुदं महत् । नारायणा इति ख्याता: सर्वे संग्रामयोधिन:।१८।
अनुवाद - मेरे पास दस करोड़ गोपों (आभीरों) की विशाल सेना है, जो सबके सब मेरे जैसे ही बलिष्ठ शरीर वाले हैं। उन सबकी 'नारायण' संज्ञा है। वे सभी युद्ध में डटकर मुकाबला करने वाले हैं।।१८।।
इसी तरह से जब भगवान श्रीकृष्ण ने इन्द्र की पूजा बन्द करवा दी, तब इसकी सूचना जब इन्द्र को मिली तो वह क्रोध से तिलमिला उठा और भगवान श्रीकृष्ण सहित समस्त अहीर समाज को जो कुछ कहा उसका वर्णन श्रीमद्भागवत पुराण के दशम स्कन्ध के अध्याय -(२५ )के श्लोक - (३) से( ५) में मिलता है। जिसमें इन्द्र ने अपने दूतों से कहा कि-
अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां काननौकसाम्
कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनम्।।३।
वाचालं बालिशं स्तब्धमज्ञं पण्डितमानिनम्।
कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा मे चक्रुरप्रियम्।। ५।
अनुवाद- ओह, इन जंगली ग्वालों (गोपों ) का इतना घमण्ड ! सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला।३।
• कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है। फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। ५।
उपर्युक्त दो श्लोकों में यदि देखा जाए- तो इनमें गोप शब्द आया है जो अहीर तथा यादव शब्द का पर्यायवाची शब्द है।
इसी तरह से संस्कृत श्लोकों में अहीरों के लिए गोपाल शब्द का प्रयोग भागवत पुराण स्कन्ध दशम के अध्याय- (६१) के श्लोक (३५) में मिलता है। जिसमें द्यूत- क्रीडा) जूवा खेलते समय रुक्मि बलराम जी को कहता है कि -
नैवाक्षकोविदा यूयं गोपाला वनगोचरा:।
अक्षैर्दीव्यन्ति राजनो बाणैश्च नभवादृशा।।३४।
अनुवाद - बलराम जी आखिर आप लोग वन- वन भटकने वाले गोपाल (ग्वाले) ही तो ठहरे! आप पासा खेलना क्या जाने ? पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं।
इस श्लोक को यदि देखा जाए तो इसमें बलराम जी के लिए गोपाल शब्द का प्रयोग किया गया है जो एक साथ- गोप, ग्वाल, अहीर और यादव समाज के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इसलिए गर्गसंहिता के अनुवाद कर्ता, अनुवाद करते हुए गोपाल शब्द को ग्वाल के रूप में लिखते हैं।
इसी तरह से भगवान श्रीकृष्ण को एक ही प्रसंग में एक ही स्थान पर यदुवंश शिरोमणि और गोप (ग्वाला) दोनों शब्दों से सम्बोधित युधिष्ठिर के राजशूय यज्ञ के दरम्यान उस समय किया गया।
वासुदेवेति मां ब्रूत न तु गोपं यदूत्तमम् ।
एकोऽहं वासुदेवो हि हत्वा तं गोपदारकम् ।। १भविष्यपर्व- अध्या!य91 )
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
(१)- भारतीय समाज में पञ्च-प्रथा की संकल्पना और अहीरों का पृथक वर्ण-
[क]- पञ्चमवर्ण वर्ण की उत्पत्ति-
देखा जाए तो प्राचीन भारतीय समाज में पञ्च-पञ्चायत और पञ्चजन जैसे शब्द सामाजिक व्यवस्था में पाँच वर्णों की मान्यता व उनके निर्णयों पर आधारित पञ्च- प्रथा के ही सूचक दिग्दर्शक थे। जो परम्परागत रूप से आज भी ग्रामीण समाज में पञ्चों द्वारा की गयी पञ्चायतों के रूप में प्रचलित व विद्यमान हैं।
जिसे भारत की पञ्चायत राज प्रणाली में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्योंकि भारत में पञ्चायत राज प्रणाली, भारतीय समाज में पारम्परिक रूप से ग्राम संस्थाओं पर ही आधारित है।
ग्राम पञ्चायत, गाँव की मन्त्रिपरिषद का काम करती है। जिनके सदस्यों का चुनाव जनता करती है और इस जनता मे सभी पाँचों वर्णों के प्रतिनिधि पञ्च के रूप में उपस्थित व अनुमोदित होकर अपना निष्पक्ष निर्णय देते हैं।
इस तरह की संकल्पना हमारे समाज में पूर्व काल से ही रही है। जिसकी पुष्टि- सर्वप्रथम ऋग्वेद से होती है जिसमें बताया गया है कि- पञ्चकृष्टी और पञ्चजन शब्द पाँच वर्णों के प्रतिनिधि व पञ्चों के रूपान्तरण थे।
"आ दधिक्राः शवसा पञ्चकृष्टीः सूर्य इव ज्योतिषापस्ततान।
सहस्रसाः शतसा वाज्यर्वा पृणक्तु मध्वा समिमा वचांसि ॥१०॥ ऋग्वेद ४/३८/१०
तदद्य वाचः प्रथमं मसीय येनासुराँ अभि देवा असाम।
ऊर्जाद उत यज्ञियास: पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम् ॥ ऋग्वेद-१०.५३.४।
पदों का अर्थ-
(अद्य) = आज (तद् वाचः प्रथमम्) = उस प्रथम वाणी को (मसीय) = हृदयस्थरूपेण उच्चारण करता हूँ। (येन) = जिससे (देवाः) = और देवगण (असुरान्) = आसुरों को (अभि असाम) = अभिभव करते हैं।
(ऊर्जादः) = पौष्टिक (शक्तिवर्धक) अन्नों का सेवन करने वाले (उत) = और (यज्ञियासः) = यज्ञशील (पञ्चजना:) = पाँच वर्ण (जाति) ! (मम होत्रम्) = मेरे हवन को (जुषध्वम्) = प्रीतिपूर्वक सेवन करो।
उपर्युक्त ऋचाओं में पञ्च' पञ्चकृष्टी' और पञ्च जन' जैसे पद पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
ऋग्वेद में पञ्चजन: और पञ्चकृष्टी संज्ञा पद बताते हैं कि समाज में पाँच प्रकार के व्यक्ति थे जिनका समाज में वर्चस्व होता था। ऋग्वेद में उल्लिखित पञ्चजना: शब्द पाँच जातियों के प्रतिनिधियों का ही वाचक है।
श्लोक:
ब्राह्मण क्षत्त्रिय वैश्य शूद्राश्चतस्रो जातयो यथा।
तथा स्वतन्त्रा जातिरेका आभीरा च तस्या वर्ण अस्मिन् विश्वे वैष्णवाभिधा।।
(ब्रह्मवैवर्तपुराण, ब्रह्मखण्ड, एकादश अध्याय, सात्वतीय टीका)
सारांश (टीका के अनुसार)
यह श्लोक ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखण्ड से लिया गया है, जिसमें चातुर्यवर्ण्य व्यवस्था के अतिरिक्त पाँवे वैष्णव वर्ण की महत्ता को भी दर्शाया गया है। श्लोक में कहा गया है कि जैसे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं, वैसे ही विश्व में वैष्णव नाम का एक स्वतन्त्र और सर्वोच्च वर्ण है।
इस वैष्णव वर्ण के अन्तर्गत आभीर /आहीर ( यादव अथवा गोप जाति को एक स्वतन्त्र और विशेष जाति के रूप में उल्लेखित किया गया है, जो गोप (आभीर) जाति भगवान स्वराट्- विष्णु से उत्पन्न होकर उनकी सनातन भक्ति में ही लीन रहती है। वह वर्ण से वैष्णव है।
विस्तृत व्याख्या व भावार्थ:-
यह श्लोक भारतीय दर्शन और सामाजिक संरचना में ब्रह्मा की चातुर्यवर्ण्य व्यवस्था के साथ-साथ स्वराट्- विष्णु से उत्पन्न एक अन्य वर्ण वैष्णव की सार्वभौमिकता , प्राचीनता और उसकी सर्वोपरिता को स्थापित करता है।
शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था को समाज के कार्यों को सुचारु व व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बनाया गया था, जिसमें प्रत्येक वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र) की अपनी विशिष्ट भूमिका थी।
एक अन्य वर्ण वैष्णव इन सबसे पृथक और सर्वोच्च था।
समाज में प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था के प्रतिनिधित्व के लिए पञ्चायत व्यवस्था भी कायम थी। जो समवेत रूप से सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए सम्मति व निर्णय पारित करती थी।
पञ्च शब्द समाज के पाँच वर्णों के प्रतिनिधीयों को स्वयं में अन्तर्निहित किए हुए है।
वैदिक ऋचाओं में बहुतायत से पञ्चजना, और पञ्चकृष्टय: जैसे पद पाँच वर्णों से सम्बन्धित पञ्चायत व्यवस्था की प्राचीनता को अभिव्यक्त करते है।
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📚: १२वीं सदी के गुजरात के जैन धर्माचार्य व विद्वान हेमचन्द्र सूरी ने अपने ग्रन्थ द्वाश्रय(
महाकाव्य के द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सर्गों में 'आभीर' और 'आहीर' दोनों शब्दों का प्रयोग. संस्कृत और प्राकृत में सर्वप्रथम समानार्थक रूप से किया है,
यद्यपि उनके द्वारा किया गया प्रयोग एक-दूसरे के पर्याय के रूप में था, जिससे यह पता चलता है कि वे एक ही समुदाय को दर्शाते थे।
आभीर और अहीर का सम्बन्ध:
अहीर शब्द मूल रूप से 'आभीर' शब्द का विकृत प्राकृत रूप है, और कुछ इतिहासकार इसे निडर व्यक्ति के रूप में भी परिभाषित करते हैं।
कुछ लोग आभीरों को कृष्ण के वंशज मानते हैं, जिन्हें यदुवंशी अहीर कहा जाता है।
- द्वयाश्रय काव्य क्या है ?
- यह प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध महाकाव्य 'कुमारपाल-चरित' का दूसरा नाम है।
- इसे आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी प्राकृत व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए १२वीं सदी में रचा था।
- यह महाकाव्य २० सर्गों का है, जिसमें पहले ४ सर्गों में राजा कुमारपाल के जीवन का वर्णन है और बाकी सर्गों में जैन धर्म की मान्यताओं का वर्णन है।
- आभीर कौन थे?
- आहीरों को प्राचीन काल के आभीर जाति के रूप में जाना जाता है, जिसमें यादव वंश का प्रादुर्भाव होता है।
- वे भारतीय उपमहाद्वीप के एक योद्धा-पशुपालक और कृषक समुदाय के सदस्य थे और स्वयं को यदुवंशी कहते हैं।
- द्वयाश्रय काव्य में आभीरों का सन्दर्भ:
- यह काव्य गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल से सम्बन्धित है।
- काव्य में 'वनथली के चूड़ासमा राजकुमार गृहरिपु' का उल्लेख है, जिसे समानार्थक रूप से यादव और आभीर कहा गया है, जो अभीरों के यादवों से सघन सम्बन्ध की पुष्टि करता है।
- द्वयाश्रय काव्य के माध्यम से यह भी पता चलता है कि मूलराज ने सौराष्ट्र के आभीरों के साथ भी सम्बन्ध स्थापित किए थे, जैसा कि किसी दानपत्र से प्रमाणित होता है।
द्वयाश्रय काव्य में आभीरों का उल्लेख एक ऐतिहासिक सन्दर्भ में मिलता है, जिसमें आभीर के लिए प्राकृत भाषा में आहीर शब्द का प्रयोग समानान्तर रूप से हुआ है। और सौराष्ट्र व गुजरात के आभीरों के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है।
- आभीर का संस्कृत रूप: संस्कृत में 'आभीर' शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत और पुराणों में मिलता है।
- प्राकृत का प्रभाव: प्राकृत भाषा के विकास के दौरान, संस्कृत के कई शब्द अपभ्रंश होकर सरल रूप ले लेते थे। इसी प्रक्रिया के तहत 'आभीर' शब्द 'अहीर' में बदल गया।
- तद्भव परिवर्तन: यह एक तद्भव परिवर्तन है, जिसमें एक शब्द संस्कृत से प्राकृत और फिर अन्य स्थानीय भाषाओं में बदलते हुए नया रूप धारण करता है।
- महाभारत और पुराणों में आभीरों का उल्लेख एक गोपालन और युद्धप्रिय जाति के रूप में मिलता है।
- समय के साथ, यह नाम बदलकर "अहीर" हो गया और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में इन लोगों को अहीर, ग्वाला और यादव के नाम से भी जाना जाने लगा, जो सभी गोपालन के पारम्परिक पेशे से जुड़े हैं।
अन्य धर्मों में भी कृष्ण की मान्यता ब्राह्मण धर्म से बाहर- जैन" बौद्ध जातक और बहाई धर्म तक (भाग प्रथम) में हमने संक्षेप में उल्लेख किया -
"बौद्ध धर्म के ग्रन्थों में कृष्ण का अस्तित्व-
अभीर,आभीर, अवर, अफर, अबीर आयर, आयबेरिया, तथा वीर नाम से अहीरों की प्राचीन विभिन्न संस्कृतियों में उपस्थिति -
आहिर आदिमजाति माना जाता है इनको इजरायल में अबीर। अफ्रीका में अफर । तुर्की में अवर। आयरलैंड अथवी आयरिश में आबेरिय । । चीन में "सु" नाम से शोधकर्ताओं ने पहचान किया।
परन्तु इनका मुख्य रूप से हर सभ्यता के साथ तो जिक्र है ही अब्राहमिक( यहूदी ) धर्म और भारतीय धर्म में भी समान जिक्र है। दोनों मुख्य धर्मो के ग्रन्थ को देखा जाय तो समानता है।
यादव की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार ययाति से यदु और यदु से यादव वंश की उत्पत्ति हुई । परन्तु प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदु वंश किस जाति में उत्पन्न हुआ। भारतीय पुराणों में विशेषत: पद्मपुराण सृष्टि खण्ड में आभीर जाति को सत्युग के प्रारम्भ में उपस्थित माना है । भारतीय पुराणों के अनुसार सभी चारों युगों में आभीर जाति उपस्थित रही है।
यहूदीयों की उत्पत्ति बाइबिल के सृष्टि खण्ड ( जेनेसिस ) अनुसार याकूब से यहूदा और यहूदा से यहूदीयों की उत्पत्ति हुई है।
याकूब इजराएल के नीम से भी जानी जाती है। याकूब से जैकब और हाकि़म जैसे शब्द विकसित हुए। याकूव ही ययाति है।
अब ये यादव यहुदी हैं अथवा यहूदी यादव हैं तो सवाल उठता है ये अहीर कौन है?
हिब्रू बाइबिल में अबीर शब्द शक्तिशाली अथवा बहादुर का विशेषण है।
- ** ईश्वर के लिए विशेषण:** यह ईश्वर की शक्ति और दृढ़ता को व्यक्त करने के लिए एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है।
- "अबीर याकूब": जेनेसिस 49:24 में, यह "याकूब का बल" (Mighty One of Jacob) के रूप में आता है, जो ईश्वर को याकूब के संरक्षक और रक्षक के रूप में दर्शाता है।
- ** काव्यात्मक प्रयोग**: इसका उपयोग अक्सर काव्य पंक्तियों में किया जाता है, जो ईश्वर की ताकत और उसकी शक्ति को दर्शाती है।
- उत्पत्ति 49:24: "परन्तु उसका धनुष बना रहा और उसका बाण दृढ़ रहा; उसके हाथों की कलाइयाँ मेरे अबीर-याकूब के हाथों के कारण मज़बूत हो गईं..."।
- भजन 132:2, 5: ईश्वर का उल्लेख "अबीर" के रूप में भी किया जाता है।
- यशायाह 49:26: ईश्वर की अपनी लोगों पर विजय और बचाव का वर्णन करने के लिए।
यहुदह् को ही यदु कहा गया ...
हिब्रू बाइबिल में यदु के समान यहुदह् शब्द की व्युत्पत्ति
मूलक अर्थ है " जिसके लिए यज्ञ की जाये"
और यदु शब्द यज् --यज्ञ करणे
धातु से व्युत्पन्न वैदिक शब्द है ।
इज़राएल में आज भी अबीर यहूदीयों का एक वर्ग है ।
जो अपनी वीरता तथा युद्ध कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है ।
कहीं पर " आ समन्तात् भीयं राति ददाति इति आभीर :
इस प्रकार आभीर शब्द की व्युत्पत्ति-की है , जो
अहीर जाति के भयप्रद रूप का प्रकाशन करती है ।
अर्थात् सर्वत्र भय उत्पन्न करने वाला आभीर है ।
यह सत्य है कि अहीरों ने दास होने की अपेक्षा दस्यु होना उचित समझा ...
- प्राचीन भारतीय संदर्भ:यहूदी धर्म का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत पैगंबर इब्राहिम ने की थी, और उनके पोते याकूब (जिन्हें इजराइल भी कहा जाता है) ने 12 यहूदी कबीलों का गठन किया था, जिनमें से एक "अबीर" कबीला था। यहूदी धर्म के ऐतिहासिक ग्रंथ, 'तनख', में इस बात का उल्लेख है कि यह कबीला भारत की प्राचीन अहीर जाति से उत्पन्न हुआ था।
- प्रमाण और शोध:कुछ शोधकर्ताओं ने "अबीर" कबीले के इस संबंध में प्राचीन भारत के "अहीर" वंश से होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- समान नामकरण:"यहूदी अबीर कबीला" के रूप में, यहूदी धर्म से जुड़ा "अबीर" कबीला भारत के प्राचीन अहीर कबीले से जुड़ा हुआ है, जो आज भी भारत में कई क्षेत्रों में रहते हैं।
- सांस्कृतिक और भाषाई जुड़ाव:यहूदी धर्म के अनुयायियों के बीच "अबीर" का विशेष स्थान है क्योंकि यह उनकी प्राचीन जड़ों और उनके ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा हुआ है।
यहूदीयों की हिब्रू बाइबिल के सृष्टि-खण्ड नामक अध्याय Genesis 49: 24 पर ---
अहीर शब्द को जीवित ईश्वर का वाचक बताया है।
----------------------------------------------------------
___The name Abir is one of The titles of the living god for some reason it,s usually translated for some reason all god,s
in Isaiah 1:24 we find four names of
The lord in rapid succession as Isaiah
Reports " Therefore Adon - YHWH - Saboath and Abir ---- Israel declares...
------------------ ---------------------
Abir (अभीर )---The name reflects protection more than strength although one obviously -- has to be Strong To be any good at protecting still although all modern translations universally translate this name whith ---- Mighty One , it is probably best translated whith --- Protector --रक्षक ।
हिब्रू बाइबिल में तथा यहूदीयों की परम्पराओं में ईश्वर के पाँच नाम प्रसिद्ध हैं :----
(१)----अबीर (२)----अदॉन (३)---सबॉथ (४)--याह्व्ह् तथा (५)----(इलॉही)
-------------------------------------------------------------------
हिब्रू भाषा मे अबीर (अभीर) शब्द के बहुत ऊँचे अर्थ हैं- अर्थात् जो रक्षक है, सर्व-शक्ति सम्पन्न है
इज़राएल देश में याकूब अथवा इज़राएल-- ( एल का सामना करने वाला )को अबीर
का विशेषण दिया था ।
इज़राएल एक फ़रिश्ता है जो भारतीय पुराणों में यम के समान है ।
जिसे भारतीय पुराणों में ययाति कहा है ।
ययाति यम का भी विशेषण है।
समानता के और भी स्तर हैं जैसे- हिब्रू बाइबिल में ईसा मसीह की बिलादत (जन्म) भी गौओं के सानिध्य में ही हुई ...
ईसा का नाम (कृष्ट) है जो कृष्ण के चरित्र का भी साम्य है।
ईसा के गुरु ऐञ्जीलस ( Angelus)/Angel हैं जिन्हें हिब्रू परम्पराओं ने फ़रिश्ता माना है ।
तो कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु घोर- आंगीरस हैं ।जिन्हें सप्तर्षियों गिना जाता है।
तो ये समझना जरूरी है। कि यदु तो व्यक्ति थे जिनके वंश को यादव नाम से जाना थे उनकी जाति क्या थी ? इसका जवाब प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में जैसा कि वर्णन है ऋग्वेद के दशम मण्डल के (62) में सूक्त मन्त्र में 👇
उत दासा परिविषे स्मद्दिष्टी (स्मत् दिष्टी गोपरीणसा यदुस्तुर्वश् च मामहे।१०।
अर्थात् यदु और तुर्वशु नामक जो दास हैं गोओं से परिपूर्ण है अर्थात् चारो ओर से घिरे हुए हैं हम सब उनकी स्तुति करते हैं।१०।
यहाँ यदु को गोप ही बताया गया है। यादव ही अभीर है यदु के बाद इनको यादव भी कहा जाने लगा था इस कारण ही सभी शोधकार्ता यहूदी यादव को एक ही मानते हैं। क्यों की इनके उत्त्पति में तो समानता है ही संस्कृति में भी व्यवस्था में अत्यधिक समानता है। यहाँ तक की वैवाहिक परम्पराओं और प्रवृत्तियों में भी गजब की आश्चर्जनक समानता है।
बदले की भावना ये अपने दुश्मन को छोड़ते नही जातिवादी कट्टरता इनको रक्तशुद्धता में परिबद्ध करती है।
यानी यादव यहूदी वही हो सकता है जिसके माता पिता दोनों यादव हो बरना मामला गड़बड़ समझो समाज से बाहर कर देते है। जैसे यहां यादवों का योद्धा कबीला अहीर है वैसे ही यहूदियों का योद्धा कबीला अबीर है। जिसने पश्चिमी एशिया में जूडो -कराटे का व्यवहारिक ज्ञान दिया।
"मिश्र के यहूदीयों का एक विशेषण कॉप्ट(गुप्त)-
गोप और अंग्रेज़ी कॉप(Cop) शब्दों की एक रूपता-
- कॉप्टिक (Coptic)शब्द मिस्र के ईसाई समुदाय को संदर्भित करता है, जो प्राचीन मिस्रवासियों के वंशज हैं।
- यह शब्द ग्रीक शब्द "एजिप्टियोस" से आया है, जिसका अर्थ "मिस्रवासी" है, जिसे बाद में अरबों ने इसे "क़ुबत" कर दिया।
- पशु-मुद्रा प्राचीन समाजों में, विनिमय के माध्यम के रूप में सीधे पशुओं का इस्तेमाल होता था। लोग अपनी ज़रूरतों के अनुसार मवेशी, गाय या भैंस जैसी चीज़ों का आदान-प्रदान करते थे।
- पशुओं का महत्व:पशुधन को धन और संपत्ति का एक महत्वपूर्ण रूप माना जाता था। यह वित्तीय सुरक्षा और विनिमय का एक प्रारंभिक तरीका पशु ही थे ।
- ** धातु मुद्रा की ओर विकास:** धीरे-धीरे, धातु मुद्रा का विकास हुआ, जो पशुधन की तुलना में अधिक सुविधाजनक और टिकाऊ थी। धातु मुद्रा का प्रचलन बढ़ने के साथ ही पशु-मुद्रा समाप्त होने लगी परन्तु उनके लिए नामित शब्द रूढ हो गये।
- आधुनिक पैसे का विकास:धातु मुद्रा से हुआ, जो पैसे के एक महत्वपूर्ण विकासवादी क्रम का हिस्सा है।
- लैटिन/पुरानी फ्रेंच से उत्पत्ति:'फीस' (Fee) शब्द की उत्पत्ति पुरानी फ्रेंच शब्द 'fée' या लैटिन शब्द 'feudum' से हुई है, जिसका अर्थ किसी अधिकार या विशेषाधिकार के बदले भुगतान किया जाने वाला शुल्क था।
- सामंती व्यवस्था:प्रारंभिक सामंती व्यवस्था में, 'फीस' शब्द का उपयोग भूमि के स्वामित्व या सामंती व्यवस्था के तहत प्राप्त होने वाले पदों के लिए किया जाता था। सेवा के बदले दी जाने वाली भुगतान को भी फीस कहा जाता था।
- पृष्ठभूमि:जब मूसा पर्वत सिनाई पर परमेश्वर से मिलने के लिए गए, तब इस्राएलियों ने मूसा के पीछे छूटने के कारण सोने का बछड़ा बनाने और उसकी पूजा करने का निर्णय लिया।
- आराधना:इस्राएलियों ने सोने के इस बछड़े की पूजा की, जिसे परमेश्वर की पूजा के बजाय एक मूर्तिकला के रूप में देखा गया, जिससे ईश्वर के साथ उनका विश्वास और भरोसा कमज़ोर हुआ।
- बाइबिल का चित्रण:निर्गमन की पुस्तक में इस घटना को मूर्तिपूजा का एक उदाहरण के रूप में वर्णित किया गया है और इसे 'पाप' माना गया है।
एक लाल बछिया, या हिब्रू में जिसे "पराह अदुमाह", कहते है बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुनने में लगता है—एक छोटी मादा गाय जो पूरी तरह से लाल होती है। लेकिन हम यहाँ किसी भी लाल गाय की बात नहीं कर रहे हैं। यहूदी परम्परा के अनुसार, इस बछिया को कुछ खास मानदण्डों पर खरा उतरना होता है:
- यह पूरी तरह से लाल होना चाहिए (बहुत ही चुनिंदा बातें!)
- इसमें कोई दोष नहीं हो सकता
- इसका उपयोग कभी भी श्रम के लिए नहीं किया गया होगा (काम करने वाली बछियाओं की अनुमति नहीं है!)
ये आवश्यकताएं सीधे बाइबल से आती हैं, विशेष रूप से गिनती 19:1-2 , जिसमें ईश्वर द्वारा कहा गया है:
“अदोन( ईश्वर) ने मूसा और हारून से कहा, 'यह तोरा( धर्म संहिता )की विधि है, जिसकी आज्ञा अदोन ने दी है: इस्राएलियों से कहो कि वे तुम्हारे पास एक निर्दोष लाल बछिया ले आएं, जिस पर कोई दोष न हो और जिस पर कभी कोई जूआ न रखा गया हो।'”
इन सभी मानदंडों पर खरी उतरने वाली गाय मिलना लगभग उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई मिलना—अगर वह सुई भी पूरी तरह लाल हो और उससे कभी कुछ सिलने में इस्तेमाल न किया गया हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जब कोई संभावित उम्मीदवार सामने आता है तो लोग उत्साहित हो जाते हैं!
भारत-यूरोपीय देवताओं वरुण , मित्र और इंद्र और यम को किसके राज्य में मान्यता दी गई थी। यह पूर्वोत्तर सीरिया में मितन्नीयों( जिसे वेद में मितज्ञु) कहा गया है। यहीं पूर्वोत्तर सीरिया( सामदेश) दूसरी सहस्राब्दी की तीसरी तिमाही में हुर्रियन आबादी पर एक इंडो-आर्यन अभिजात वर्ग का शासन था। उनके मुख्य देवताओं के नाम और सामान्य चरित्र से परे हुर्रियनों के धर्म के बारे में बहुत कम जानकारी है: तेशुब( अशुतोष) , एक तूफान देवता, और उसकी पत्नी हेपत( हेमवती); उनका बेटा, शर्रुमा( स्कन्द), का विवरण है। एक तूफान देवता भी; मेसोपोटामियन ईशर( स्त्री) के साथ पहचानी जाने वाली देवी शौशका; और कुसुख और शिमेगी, चंद्र और सौर देवता , क्रमशः तथा इनसे सम्बन्धित हुरियन पौराणिक कथाओं को हित्ती संस्करणों के माध्यम से ही जाना जाता है।
सैमेटिक "हैमेटिक और यूरोपीय संस्कृतियों में "मनु" की उपस्थिति-
____________
मनु के विषय में विश्व के सभी धर्म - मतावलम्बी अपने अपने पूर्वाग्रह से ग्रस्त ही हैं ।
भारतीय सन्दर्भों में किसी ने "मनु" की अवधारणा अयोध्या के आदि- पुरुष के रूप में है। तो किसी ने सुमेर और बैबीलॉन ( मेसोपाटामिया ) की संस्कृतियों में "नूह" के रूप में की है । परन्तु अयोध्या का स्थान निर्धारण अनिश्चित है। किसी ने मनु को हिमालय का अधिवासी कहा है ! परन्तु हिमालय पर्वतीय प्रदेश है जो यूरोपीय संस्कृति का संकेत करता है।
____________________________________
"परन्तु सत्य के निर्णय निश्पक्षता के सम धरातल पर होते हैं न कि पूर्वाग्रह के ऊबड़ खाबड़ स्थलों पर ". और हम मनु के ऐतिहासिक तथ्यों पर एक निष्पक्ष पहल करेंगे-
विश्व की सभी महान संस्कृतियों में "मनु" का वर्णन मानव सभ्यता के उद्भासक के रूप में किसी न किसी प्रकार अवश्य हुआ है !
परन्तु भारतीय संस्कृति में यह मान्यता अधिक प्रबल तथा पूर्णत्व को प्राप्त है। अत: इस विवरण में भारतीय सन्दर्भों को उद्धृत करते हुए अन्य संस्कृतियों से भी तथ्य उद्धृत किए गये हैं।
👇
1- प्रथम सांस्कृतिक वर्णन:–"भारतीय पुराणों में मनु का वर्णन:–👇
पुराणों में वर्णित है कि मनु ब्रह्मा के पुत्र हैं ;
जो मनुष्यों के मूल पुरुष माने जाते हैं।
विशेष—वेदों में मनु को यज्ञों का आदिप्रवर्तक लिखा है। ऋग्वेद में कण्व और अत्रि को यज्ञ प्रवर्तन में मनु का सहायक लिखा है।
शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि मनु एक बार जलाशय में हाथ धो रहे थे; उसी समय उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आई।
उसने मनु सें अपनी रक्षा की प्रार्थना की और कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए;
मैं अपकी भी रक्षा करुँगी। उसने मनु से एक आनेवाली बाढ़ की बात कही और उन्हें एक नाव बनाने के लिये कहा।
मनु ने उस मछली की रक्षा की; पर वह मछली थोड़े ही दिनों में बहुत बड़ी हो गई।
जब बाढ़ आई, मनु अपनी नाव पर बैठकर पानी पर चले और अपनी नाव उस मछली की आड़ ( श्रृंग) में बाँध दी। मछली उत्तर को चली और हिमालय पर्वत की चोटी पर उनकी नाव उसने पहूँचा दी। वहाँ मनु ने अपनी नाव बाँध दी।
उस बड़े ओघ (जल-प्रलय )से अकेले मनु ही बचे थे। उन्हीं से फिर मनुष्य जाति की वृद्धि हुई। दूसरी कथा के अनुसार-
ऐतरेय ब्राह्यण में मनु के अपने पुत्रों में अपनी सम्पत्ति का विभाग करने का वर्णन मिलता है। उसमें यह भी लिखा है कि उन्होंने हरिवंश पुराण के अनुसार वैवस्वत मनु के एक पुत्र "नाभागारिष्ठ" को अपनी संपत्ति का भागी नहीं बनाया था।
निघण्टु में 'मनु' शब्द का पाठ "द्युस्थान देवगणों में है ; और वाजसनेयी संहिता में मनु को प्रजापति लिखा है। पुराणों और सूर्यसिद्धान्त आदि ज्योतिष के ग्रन्थों के अनुसार एक कल्प में चौदह मनुओं का अधिकार होता है और उनके उस अधिकारकाल को मन्वन्तर (मनु-अन्तर) कहते हैं।
चौदह मनुओं के नाम ये हैं—(१)स्वायम्। (२)स्वारोचिष्। (३) उत्तम। (४) तामस। (५) रवत। (६) चाक्षुष। (७) वैवस्वत। (८) सावर्णि। (९) दक्षसावर्णि। (१०) ब्रह्मसावर्णि। (११) धमसावर्णि। (१२) रुद्रसावर्णि। (१३) देवसावर्णि और(१४) इन्द्रसावर्णि।
वर्तमान मन्वन्तर वैवस्वत मनु का है।
मनुस्मृति मनु को विराट् का पुत्र लिखा है और मनु से दस प्रजापतिया की उत्पत्ति हुई यह वर्णन है।
--जो सुमेरियन माइथॉलॉजी से संग्रहीत है-
"संस्कृत भाषा में मनु शब्द की व्युत्पत्ति !
मन्यते इति मनु। ( मन् + इति उ:) मनु: “ शॄस्वृस्निहीति । “ उणादि सूत्र १ । ११ ।
ब्रह्मणः पुत्त्रः । स च प्रजापतिर्धर्म्मशास्त्रवक्ता च ।
इति लिङ्गादिसंग्रहे अमरः ॥ ब्रह्मा का पुत्र धर्मशास्त्र का वक्ता मनुष्यों का पूर्वज । इति शब्द- रत्नावली ॥
(यथा ऋग्वेदे । ८। ४७। ४।“ मनोर्विश्वस्य घेदिम आदित्याराय ईशतेऽनेहसो व ऊतयः सु ऊतयो व ऊतयः ॥ ऋगवेद 8/47/4“ मनोर्भव: मनुष्य: ।
इति तद्भाष्ये सायणः ॥
वस्तुत
मनु सुमेरियन संस्कृतियों में विकसित माइथॉलॉजीकल की अवधारणा है ।
____________________________________
इसी आधार पर काल्पनिक रूप से ब्राह्मण समाज द्वारा वर्ण-व्यवस्था का समाज पर आरोपण कर दिया गया , जो वैचारिक रूप से तो सम्यक् था परन्तु व्यवहारिक रूप में कभी यथावत् परिणति नहीं हुआ।
वर्ण व्यवस्था जाति अथवा जन्म के आधार पर दोष-पूर्ण व अवैज्ञानिक ही थी ।
इसी वर्ण-व्यवस्था को ईश्वरीय विधान सिद्ध करने के लिए काल्पनिक रूप से ब्राह्मण - समाज ने मनु-स्मृति की रचना की ।
जिसमें तथ्य समायोजन इस प्रकार किया गया कि स्थूल दृष्टि से कोई बात नैतिक रूप से मिथ्या प्रतीत न हो ।
वर्तमान में मनु के नाम से नामित स्मृति ग्रन्थ( धर्म-शास्त्र) पुष्यमित्र सुंग के अनुयायी सुमित भार्गव (ई०पू०१८४-४८ ) के समकालिक है ।
यह पुष्य-मित्र सुंग केे निर्देशन में ब्राह्मण समाज द्वारा 'मनु' की रचना मान्य कर दी गयी ।
लगभग चौथी शताब्दी में नारद स्मृति के लेखक को मनुस्मृति के लेखक का नाम ज्ञात था । नारद स्मृति कार के अनुसार ' सुमति भार्गव ' नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मनुसंहिता की रचना की ।इस प्रकार मनु नाम ‘सुमति भार्गव' का छद्म नाम था और वह ही इसके वास्तविक रचयिता थे”( अम्बेडकर वाड्मय , भाग 7 , पृ० 151 ) ।
— “मनु के काल - निर्धारण के प्रसंग में डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक में सन्दर्भ देते हुए बताया था कि मनुस्मृति का लेखन ईसवी पूर्व 185 , अर्थात पुष्यमित्र की क्रान्ति के बाद सुमति भार्गव के हाथों हुआ था ।” ( वही , भाग 7 , पृ० 116 )
____________________________________
परन्तु मनु भारतीय धरा की विरासत नहीं थे ।
और ना हि अयोध्या उनकी जन्म भूमि थी। यह भी सत्य है क्योंकि भारत में अयोध्या का स्थान अनिश्चित ही है।
वर्तमान में अयोध्या भी थाईलेण्ड बैंकॉक में "एजोडिया" के रूप में है ।
रामनगरी अयोध्या (Ayodhya) की तरह एक और आयोध्या थाइलैंड (Thailand) में भी बसती है। थाइलैंड एक ऐसा देश है जहां पर राम को सांस्कृतिक धरोहर की तरह माना जाता है। यहाँ पर कई प्राचीनकाल राममंदिर हैं और एक शहर है 'अयुत्थया' (Ayutthaya, Thailand) जो स्थानीय भाषा में अयोध्या का समानार्थी है।
सुमेरियन सभ्यताओं में भी अयोध्या को एजेडे "Agede" नाम से वर्णन किया है। जिसे सुमेरियन इतिहास में "अक्काद" रूप में वर्णन किया गया है। यहीं सूर्य वंशी राजा सगर का शासन था । जिन्हें सारगॉन नाम से जाना जता है। मनु को भी सगर की पूर्वज माना जाता है। सगर अयोध्या के एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। ईरान, मध्य एशिया, बर्मा, थाईलैंड, इण्डोनेशिया, वियतनाम, कम्बोडिया, चीन, जापान और यहां तक कि फिलीपींस में भी मनु की पौराणिक कथाऐं लोकप्रिय थीं।
विद्वान ब्रिटिश संस्कृतिकर्मी, जे. एल. ब्रॉकिंगटन "राम" को विश्व साहित्य का एक उत्कृष्ट शब्द मानते हैं।
यद्यपि वाल्मीकि रामायण महाकाव्य का कोई प्राचीन इतिहास नहीं है। यह बौद्ध काल के बाद की रचना है। फिर भी इसके पात्र का प्रभाव सुमेरियन और ईरानीयों की प्राचीनत्तम संस्कृतियों में देखा जा सकता है।
राम के वर्णन की विश्वव्यापीयता का अर्थ है कि राम एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति रहे होंगे। इतिहास और मिथकों पर औपनिवेशिक हमला सभी महान धार्मिक साहित्यों का अभिन्न अंग है। लेकिन स्पष्ट रूप से एक ऐतिहासिक पात्र के बिना रामायण कभी भी विश्व की श्रेण्य-साहित्यिक रचना नहीं बन पाएगी।
राम, मेडियनस और ईरानीयों के एक नायक भी हैं । जहाँ मित्र, अहुरा मज़्दा आदि जैसे सामान्य देवताओं को वरीयता दी गई है। टी• क्यूइलर यंग, एक प्रख्यात सांस्कृतिक ईरानी विद्वान जिन्होंने कैम्ब्रिज में प्राचीन इतिहास और प्रारम्भिक विश्वकोश में ईरान के इतिहास और पुरातत्व पर लिखा है:-👇
वह उप-महाद्वीप के बाहर प्रारम्भिक भारतीयों और ईरानीयों को सन्दर्भों की विवेचना करते हैं ।
💐 राम ’पूर्व-इस्लामी ईरान में एक पवित्र नाम था; जैसे आर्य "राम-एनना" दारा-प्रथम के प्रारम्भिक पूर्वजों में से थे।
जिसका सोने की टैबलेट( शील या मौहर पुरानी फ़ारसी में एक प्रारम्भिक दस्तावेज़ है;
राम जोरास्ट्रियन कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण नाम है; "रेमियश" राम और वायु को समर्पित है। संभवतः हनुमान की एक प्रतिध्वनि; भी है। कई राम-नाम पर्सेपोलिस (ईरानी शहर) में पाए जाते हैं।
राम बजरंग फार्स की एक कुर्दिश जनजाति का नाम भी है। राम-नामों के साथ कई सासैनियन शहर: राम अर्धशीर, राम होर्मुज़, राम पेरोज़, रेमा और रुमागम -जैसे नाम प्राप्त होते हैं ।
राम-शहरिस्तान सूरों की प्रसिद्ध राजधानी थी। राम-अल्ला यूफ्रेट्स (फरात) पर एक शहर है और यह फिलिस्तीन में भी है।
_____________________________________
"उच्च प्रामाणिक सुमेरियन राजा-सूची में राम सिन और भरत (बरत-सिन) सौभाग्य से प्राप्त होते हैं।
उच्च प्रामाणिक सुमेरियन राजा-सूची में राम सिन और भरत (बरत-सिन) सौभाग्य से प्राप्त होते हैं।सुमेरियन इतिहास का एक अध्ययन राम का एक बहुत ही ज्वलन्त चित्र प्रदान करता है।
उच्च प्रामाणिक सुमेरियन राजा-सूची में भरत (वरद) warad सिन और रामसिन(रिमसिन )जैसे पवित्र नाम दिखाई देते हैं।
____________________________________
राम मेसोपोटामिया वर्तमान (ईराक और ईरान)के सबसे लम्बे समय तक शासन करने वाले सम्राट थे। जिन्होंने 60 वर्षों तक शासन किया।
भरत सिन ने 12 वर्षों तक शासन किया (1834-1822 ई.पू.) का समय
जैसा कि बौद्धों के दशरथ जातक में कहा गया है। जातक का कथन है, "साठ बार सौ, और दस हज़ार से अधिक, सभी को बताया, / प्रबल सशस्त्र राम ने"
केवल इसका मतलब है कि राम ने साठ वर्षों तक शासन किया, जो अश्शूरियों (असुरों) के आंकड़ों से बिल्कुल सहमत हैं।
_____________________________________
अयोध्या सरगोन की राजधानी अगड( अवध) (अजेय) हो सकती है ।
जिसकी पहचान अभी तक नहीं हुई है।
यह संभव है कि एजेड (Agade) (अयोध्या)डेर या हारुत के पास हरयु या सरयू नदी के पास थी।👇
सीर दरिया का साम्य सरयू से है ।
सिर दरिया) मध्य एशिया की एक बड़ी नदी है। यह २,२१२ किलोमीटर लम्बी नदी किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़बेकिस्तान और काज़ाख़स्तान के देशों से निकलती है। आमू दरिया और सिर दरिया को मध्य एशिया की दो सब से महत्वपूर्ण नदियाँ माना जाता है, हालांकि आमू दरिया में सिर दरिया से कहीं ज़्यादा पानी बहता है।
इतिहास लेखक डी. पी. मिश्रा जैसे विद्वान इस बात से अवगत थे कि राम हेरात क्षेत्र से हो सकते हैं।
प्रख्यात भाषाविद् "सुकुमार सेन" ने यह भी कहा कि राम ईरानीयों के धर्म ग्रन्थ अवेस्ता में एक पवित्र नाम है।
_____________________________________
सुमेरियन माइथॉलॉजी में "दूर्मा" नाम धर्म की प्रतिध्वनि है ।
सुमेरियन माइथॉलॉजी के मितानियन ( वैदिक रूप) मितज्ञु राजाओं का तुसरत नाम दशरथ की प्रतिध्वनि प्रतीत होता है। मितज्ञुओं का वर्णन ऋग्वेद में हुआ है । ये बाइबिल के मितन्नी ही हैं। Mitanni वैदिक ऋचाओं में (मितज्ञु)
"उत स्या नः सरस्वती जुषाणोप श्रवत्सुभगा यज्ञे अस्मिन् ।
मितज्ञुभिर्नमस्यैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥४॥ ऋग्वेद7/95/4
सायण-भाष्य-उत अपि च "जुषाणा प्रीयमाणा "सुभगा शोभनधना “स्या सा “सरस्वती “नः अस्माकम् “अस्मिन् “यज्ञे “उप “श्रवत् । अस्मदीयाः स्तुतीरुपशृणोतु । कीदृशी सा। “मितज्ञुभिः प्रह्वैर्जानुभिः “नमस्यैः नमस्कारैर्देवैः “इयाना उपगम्यमाना । चिच्छब्दश्चार्थे । “युजा नित्ययुक्तेन “राया धनेन च संगता “सखिभ्यः "उत्तरा उत्कृष्टतरा । ईदृश्यस्मदीयाः स्तुतीरुपशृणोत्वित्यन्वयः
वैदिक पात्र मितज्ञुओं का वर्णन अन्य संस्कृतियों में"
तथा ऋग्वेद में अन्यत्र भी मितज्ञु जाति का वर्णन है ।"
"स वह्निभिरृक्वभिर्गोषु शश्वन्मितज्ञुभिः पुरुकृत्वा जिगाय । पुरः पुरोहा सखिभिः सखीयन्दृळ्हा रुरोज कविभिः कविः सन्॥३॥(ऋग्वेद 6/32/3)
सायण ने उपर्युक्त दौनों भाष्यों में मितज्ञु शब्द का अर्थ "छोटे घुटनों वाले" किया है । जो सत्य नहीं क्योंकि सायण को इतिहास की ज्ञान नहीं था।
मिश्तानी (मिथानी क्यूनिफॉर्म कूर उरुमी Ta-e-an-i), मित्तानी Mitanni ), जिसे मिस्र के ग्रंथों में अश्शुरियन( असुरों) के समकालीन व सहवर्ती भी कह गया है।
उत्तरी सीरिया में एक (Hurrian)
(सुर-भाषा ) बोलने वाला और सीसिस्तान के दक्षिण पूर्व अनातोलिया राज्य था।
1500-1300 ईसा पूर्व मितन्नी (मितज्ञु) एक हज़ारों अमोरिथ- एमॉराइट (मरुतों) को बाबुल के विनाश के बाद एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई ।
और असीरी (अशरियन राजाओं) की एक श्रृंखला ने मेसोपोटामिया में एक शक्ति निर्वाध रूप में बनायी।
मित्तानी साम्राज्य
1500-1300 ईसा पूर्व, सीरिया से उत्तरी सीरिया और दक्षिण-पूर्व एनाटोलिया में स्थित साम्राज्य
मित्तानी साम्राज्य यह सा्म्राज्य कई सदियों तक (१६०० -१२०० ईपू) पश्चिम एशिया में राज करता रहा। इस वंश के सम्राटों के संस्कृत नाम थे। विद्वान समझते हैं कि यह लोग महाभारत के पश्चात भारत से वहां प्रवासी बने। कुछ विद्वान समझते हैं कि यह लोग वेद की (मैत्रायणीय) शाखा के प्रतिनिधि हैं।
कुछ भी हो यहूदियों के ग्रन्थों में भी इनका वर्ण "सिन्नार (सिनाई पर्वत" के रहने वालों के रूप में हुआ है।
मिद्यान ( हिब्रू : מדין , Miḏyān ; अरबी : مدين , Maḏyān ; " नाम का अर्थ है :: संघर्ष, निर्णय ") अब्राहम के पुत्र का चौथा पुत्र और :: केतुराह का पुत्र था । वह मिद्यानी लोगों ( हिब्रू : מדיןים , Miḏyānīm ) के पूर्वज हैं, जिन्हें हाउस ऑफ़ इज़राइल के इतिहास में दो महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई थीं । मीदिया उत्तर-पश्चिमी ईरान का एक क्षेत्र है,
बाइबल मिद्यानियों की वंशावली के बारे में और अधिक विवरण नहीं देती है। (बाइबिल-उत्पत्ति 25:2,4 )
यूसुफ
यूसुफ के ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे गड्ढ़े में फेंकने के बाद , उसे मिद्यानियों के व्यापारियों को बेच दिया, जो उसे वे दास के रूप में बेचने के लिए मिस्र ले गए।
मूसा
2473 ईसापूर्व पूर्वाह्न की सर्दियों में, मूसा मिस्र से भागकर मिद्यानी देश चले गये। वहाँ उसकी मित्रता एक मिद्यानी याजक से हुई जिसका नाम :: जेथ्रो था । इस जेथ्रो की सात बेटियाँ थीं, जिनमें सिप्पोरा बड़ी थी , जिनसे मूसा ने विवाह किया था। वर्षों बाद, किन के वंशज क़ेनियों ने स्वयं को इस्राएलियों से जोड़ लिया। ( न्यायियों 1:16 )
परन्तु जब इस्राएली जंगल में भटक रहे थे, तब मिद्यानियों ने "मोआबियों" के साथ मिलकर इस्राएलियों को नष्ट करने का प्रयास किया था। प्रतिशोध में, पीनहास ने मिद्यानियों को कुचलने के लिए 12,000 पुरुषों की एक सेना का नेतृत्व किया।
गिदोन
2764 पूर्वाह्न में, मिद्यानियों ने इस्राएलियों पर अत्याचार किया, जिन्होंने तब तक कनान पर कब्जा कर लिया था । मिद्यानियों ने इस प्रभुत्व को सात वर्षों तक बनाए रखा, जब तक कि न्यायाधीश गिदोन ने तीन सौ की सेना के साथ एक संयुक्त मिद्यानियों- और मोआबी सेना को पराजित नहीं किया।
वंशज
बाइबिल मिद्यानियों
अरब इतिहासकार और भूगोलवेत्ता, याकूत अल-हमवी, हमें बताते हैं कि अरब की मिद्यानी जनजातियाँ अरबी की हाविल भाषा बोलती थीं , और वह इस तथ्य की भी पुष्टि करते हैं कि मिद्यान इब्राहीम का पुत्र था । मिद्यान की जनजातियाँ मिस्र और अन्य स्रोतों से भी जानी जाती हैं। उदाहरण के लिए, टॉलेमी ने उनकी नाम मोदियाना के रूप में दर्ज किया, जबकि सिनाई प्रायद्वीप के छोर के विपरीत प्राचीन पूर्व-इस्लामिक अरब शहर मद्यान को आज मगहिर शुऐब ("शुऐब की गुफा") के रूप में जाना जाता है।
कुर्द
इब्राहीम द्वारा भेजे जाने के बाद , मिद्यान के वंशज पर्वत श्रृंखला के उत्तर और दक्षिण दोनों काकेशस के क्षेत्र में बस गए:
मित्तानी देश की राजधानी का नाम वसुखानी (धन की खान) था।
इस वंश के वैवाहिक सम्बन्ध मिस्र से थे। एक धारणा यह है कि इनके माध्यम से भारत का बाबुल, मिस्र और यूनान पर गहरा प्रभाव पडा।
- कीर्त्य Kirta 1500 BC-1490 BC
- सत्वर्ण 1 :Shuttarna I, son of Kirta 1490 BC-1470 BC
- वरतर्ण- Barattarna, P/Barat(t)ama 1470 BC-1450 BC
- Parshatatar, (may be identical with Barattarna) 1450 BC-1440 BC
- Shaushtatar (son of Parsha(ta) tar) 1440 BC-1410 BC
- आर्ततम 1 Artatama I 1410 BC-1400 BC
- सत्वर्ण 2 Shuttarna II 1400 BC-1385 BC
- अर्थसुमेढ़ Artashumara 1385 BC-1380 BC
- तुष्यरथ अथवा दशरथ en:Tushratta 1380 BC-1350 BC
- सत्वर्ण 3 Shuttarna III 1350 BC, son of an usurper Artatama II
- मतिवाज Shattiwaza or Mattivaza, son of Tushratta 1350 BC-1320 BC
- क्षत्रवर 1 Shattuara I 1320 BC-1300 BC
- वसुक्षत्र Wasashatta, son of Shattuara 1300 BC-1280 BC
- क्षत्रवर 2 Shattuara II, son or nephew of Wasashatta 1280 BC-1270 BC, or maybe the same king as Shattuara I.
मितानी के राज्य
सदी 1500 ई०पू० से 1300 ईसा पूर्व विद्यमान थे।ओल्ड असीरियन साम्राज्य (Yamhad) जमहद मध्य अश्शूर साम्राज्य अपने इतिहास की शुरुआत में वैदिक रूप मितज्ञु की प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी मिस्र थुटमोसाइट्स के तहत थी। हालांकि, हित्ती साम्राज्य की चढ़ाई के साथ, मित्तन्नी और मिस्र ने हित्ति प्रभुत्व के खतरे से अपने पारस्परिक हितों की रक्षा के लिए एक बन्धन बनाया।
14 वीं शताब्दी ईसा पूर्व 14 वीं सदी के दौरान, मितांनी ने अपनी राजधानी वासुखेनी पर केंद्रित निगरानी रखी, जिसका स्थान पुरातत्वविदों द्वारा खबुर नदी के मुख्यालयों पर बताया गया था।
मितन्नी राजवंश ने उत्तरी युफ्रेट्स-तिग्रिस (फरात एवं दजला) क्षेत्र पर सदी के बीच शासन किया।
1475 और सदी 1275 ईसा पूर्व आखिरकार, मित्तानी हित्ती और बाद में अश्शूर (असुर )के हमलों की निन्दा करते थे, और मध्य असीरियन साम्राज्य के एक प्रान्त का दर्जा कम कर दिया गया था।
पाश्चात्य इतिहास विद "मार्गरेट .एस. ड्रावर ने "तुसरत" (दशरथ)-के नाम का अनुवाद 'भयानक रथों के मालिक' के रूप में किया है।
लेकिन यह वास्तव में 'दशरथ रथों का मालिक' या 'दस गुना रथ' हो सकता है
जो दशरथ के नाम की प्रतिध्वनि है।
दशरथ ने दस राजाओं के संघ का नेतृत्व किया। इस नाम में आर्यार्थ जैसे बाद के नामों की प्रतिध्वनि है।
सीता और राम का ऋग्वेद में भी वर्णन है।
_____________________________________
राम नाम के एक असुर (शक्तिशाली राजा) को संदर्भित करता है, लेकिन कोसल का कोई उल्लेख नहीं करता है।
वास्तव में कोसल नाम शायद सुमेरियन माइथॉलॉजी में "खास-ला" के रूप में था ।
और सुमेरियन अभिलेखों के मार-कासे (बार-कासे) के अनुरूप हो सकता है।👇
"refers to an Asura (powerful king) named Rama but makes no mention of Kosala.♨
In fact the name Kosala was probably Khas-la and may correspond to Mar-Khase (Bar-Kahse) of the Sumerian records.
कई प्राचीन संस्कृतियों में मिथकों में साम्य उनकी प्राचीन एकरूपता का सूचक हैं।
प्रस्तुत लेख मनु के जीवन की प्रधान घटना बाढ़ की कहानी का विश्लेषण करना ही है। परन्तु ये सभी पात्र पौराणिक हैं अत: इनकी ऐतिहासिक सिद्ध के लिए इनका अन्य संस्कृतियों से उद्धरण अपेक्षित है।
👇👇👇👇
2-सुमेरियन संस्कृति में 'मनु'का वर्णन जीवसिद्ध के रूप में-
महान बाढ़ आई और यह अथक थी और मछली जो विष्णु की मत्स्य अवतार थी, ने मानवता को विलुप्त होने से बचाया।
ज़ीसुद्र सुमेर का एक अच्छा राजा था और देव एनकी ने उसे चेतावनी दी कि शेष देवताओं ने मानव जाति को नष्ट करने का दृढ़ संकल्प किया है ।
उसने एक बड़ी नाव बनाने के लिए ज़ीसुद्र को बताया। बाढ़ आई और मानवता बच गई-
ज़िसुद्रा ( ओल्ड बेबीलोनियन : 𒍣𒌓𒋤𒁺 zi-ud-su₃-ra₂ , नियो-असीरियन : 𒍣𒋤𒁕 zi-sud-da , [1] ग्रीक : Ξίσουθρος , अनुवाद। Xísouthros ) शूरुपक (c. 2900 ईसा पूर्व) में सूचीबद्ध है। 62 सुमेरियन राजा महान बाढ़ से पहले सुमेर के अंतिम राजा के रूप में सूची की पुनरावृत्ति । बाद में उन्हें सुमेरियन सृजन मिथक के नायक के रूप में दर्ज किया गया और बेरोसस के लेखन में ज़िसुथ्रोस के रूप में प्रकट होता है। [ उद्धरण वांछित ]
| ज़िसुद्र 𒍣𒌓𒋤𒁺 | |
|---|---|
| शूरुपक के राजा सुमेर के राजा | |
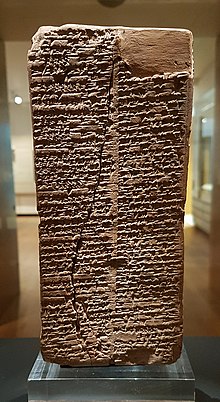 सुमेरियन राजा सूची, 1800 ईसा पूर्व, लार्सा, इराक | |
| एंटीडिल्वियन राजा | |
| शासन | सी। 2900 ईसा पूर्व |
| पूर्वज | उबर टूटू |
| उत्तराधिकारी | कीश का जलप्रलय जुशूर |
| मृत | अमर |
| राजवंश | पुराना |
| पिता | उबारा-तुतु (अक्कडियन परम्परा) |
ज़ीसुद्र कई पौराणिक पात्रों में से एक है जो निकट पूर्वी बाढ़ मिथकों के नायक हैं, जिनमें अत्रहासिस , उत्तानपश्चिम और बाइबिल नूह शामिल हैं। हालांकि प्रत्येक कहानी अपनी विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करती है, कहानी के कई प्रमुख तत्व दो, तीन या सभी चार संस्करणों के लिए आम हैं।
"साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य-
"शूरुपक के राजा जीसूद्र
सुमेरियन राजा सूची में, ज़्यूसुद्र, या शूरुपक के ज़िन-सुड्डू को एक महान बाढ़ से पहले सुमेर के अंतिम राजा के पुत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। [2] उन्हें दस सार्स (3,600 वर्ष की अवधि) के लिए राजा और गुडुग पुजारी दोनों के रूप में शासन करने के रूप में दर्ज किया गया है , [3] हालांकि यह आंकड़ा शायद दस वर्षों के लिए एक प्रतिवादी त्रुटि है। [4] इस संस्करण में, ज़िसुद्र को अपने पिता उबरा-टूटू से शासन विरासत में मिला , [5] जिन्होंने दस सार्स तक शासन किया । [6]
ज़ियसुद्र के उल्लेख के बाद की पंक्तियाँ पढ़ती हैं:
फिर बाढ़ बह गई। जब जल-प्रलय समाप्त हो गया, और राज्य स्वर्ग से उतर गया, तब राज्य कीश में था। [7]
नदी की बाढ़ के तुरंत बाद प्रारंभिक राजवंशीय काल में किश शहर का विकास शूरुपक (आधुनिक टेल फारा ), उरुक, किश और अन्य स्थानों पर तलछटी स्तर द्वारा पुरातात्विक रूप से प्रमाणित किया गया था , जिनमें से सभी को रेडियोकार्बन दिनांकित किया गया है। 2900 ईसा पूर्व। [8] जेमडेट नस्र अवधि (सी.ए. 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व) से पॉलीक्रोम मिट्टी के बर्तन , जो प्रारंभिक राजवंश I काल से तुरंत पहले थे, सीधे शूरुपक बाढ़ स्तर के नीचे खोजे गए थे। [8] [9] मैक्स मल्लोवन ने लिखा है कि "हम वेल्ड ब्लंडेल प्रिज्म [अर्थात् डब्ल्यूबी-62] से जानते हैं कि बाढ़ के समय, सुमेरियन नूह,शूरुपक शहर का राजा था, जहां उसे आसन्न आपदा की चेतावनी मिली थी। एक के रूप में उसकी भूमिका उद्धारकर्ता गिलगमेश महाकाव्य में अपने समकक्ष उत्तानपश्चिम को सौंपे गए से सहमत हैं। ... पुरालेख संबंधी और पुरातात्विक खोज दोनों ही इस बात पर विश्वास करने के लिए अच्छा आधार देते हैं कि ज़िसुद्र एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर का एक प्रागैतिहासिक शासक था, जिसके स्थल की पहचान की गई है। [10]
यह कि ज़िसुद्र शूरुपक का एक राजा था, गिलगमेश XI टैबलेट द्वारा समर्थित है, जो उत्तानपश्चिम ( सुमेरियन नाम ज़िसुद्रा का अक्कादियन अनुवाद) का संदर्भ 23 पंक्ति में "मैन ऑफ़ शूरुपक" के साथ देता है। [11
सुमेरियन बाढ़ मिथक-
ज़ियसुद्रा की कहानी सुमेरियन में लिखी गई एक एकल खंडित गोली से जानी जाती है, जिसकी लिपि 17 वीं शताब्दी ईसा पूर्व ( ओल्ड बेबीलोनियन साम्राज्य ) के अनुसार है, और 1914 में अर्नो पोएबेल द्वारा प्रकाशित की गई थी। [12] पहला भाग मनुष्य और जानवरों के निर्माण और पहले शहरों एरिडु , बाद-तिबिरा , लारक , सिप्पार और शूरुपक की स्थापना से संबंधित है । टैबलेट में लापता खंड के बाद, हम सीखते हैं कि देवताओं ने मानव जाति को नष्ट करने के लिए बाढ़ भेजने का फैसला किया है। भगवान एनकी(ताजे पानी के अंडरवर्ल्ड समुद्र के स्वामी और बेबीलोनियन देवता ईए के सुमेरियन समकक्ष) एक बड़ी नाव बनाने के लिए शूरुपक के शासक ज़िसुद्रा को चेतावनी देते हैं; नाव के लिए दिशाओं का वर्णन करने वाला मार्ग भी खो गया है। जब टैबलेट फिर से शुरू होता है, तो यह बाढ़ का वर्णन कर रहा होता है। एक भयानक तूफान सात दिनों तक चला, "विशाल नाव को महान जल पर उछाला गया था," तब उत्तु (सूर्य) प्रकट होता है और ज़िसुद्र एक खिड़की खोलता है, खुद को आगे बढ़ाता है, और एक बैल और एक भेड़ की बलि देता है। एक और विराम के बाद, पाठ फिर से शुरू होता है, बाढ़ स्पष्ट रूप से खत्म हो जाती है, और ज़ीसुद्र खुद को एन (स्काई) और एनिल (लॉर्डब्रेथ) के सामने झुका रहा है, जो उसे "अनन्त सांस" देते हैं और उसे दिलमुन में रहने के लिए ले जाते हैं । कविता का शेष भाग खो गया है। [13][ विफल सत्यापन ]
ज़ियसुद्रा का महाकाव्य 258-261 पंक्तियों में एक तत्व जोड़ता है जो अन्य संस्करणों में नहीं मिलता है, कि नदी की बाढ़ के बाद [14] "राजा ज़िसुद्र ... उन्होंने कुर दिलमुन में निवास किया , वह स्थान जहां सूरज उगता है"। सुमेरियन शब्द "कुर" एक अस्पष्ट शब्द है। शमूएल नूह क्रैमर का कहना है कि "इसका प्राथमिक अर्थ 'पहाड़' है, इस तथ्य से प्रमाणित है कि इसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चिन्ह वास्तव में पहाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाला एक चित्रलेख है। पहाड़ी देशों के बाद से 'पहाड़' के अर्थ से 'पहाड़' विकसित हुआ है। सीमावर्ती सुमेर अपने लोगों के लिए एक निरंतर खतरा थे। कुर का अर्थ सामान्य रूप से 'भूमि' भी था। [13] अंतिम वाक्य का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है "पार करने के पहाड़ में, दिलमुन का पहाड़,
एक सुमेरियन दस्तावेज़ जिसे क्रेमर द्वारा लगभग 2600 ईसा पूर्व के शूरुपक के निर्देश के रूप में जाना जाता है, बाद के संस्करण में ज़िसुद्र को संदर्भित करता है। क्रेमर ने कहा "तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक ज़ियसुद्र साहित्यिक परंपरा में एक सम्मानित व्यक्ति बन गए थे" [15]
ज़िसुथ्रोस -
ज़िसुथ्रोस (Ξίσουθρος) सुमेरियन ज़ियसुद्रा का यूनानीकरण है, जिसे बेरोसस के लेखन से जाना जाता है , जो बाबुल में बेल का एक पुजारी था , जिस पर अलेक्जेंडर पॉलीहिस्टर मेसोपोटामिया की जानकारी के लिए बहुत अधिक निर्भर था। बाढ़ मिथक के इस संस्करण की दिलचस्प विशेषताओं में, सुमेरियन देवता एन्की की ग्रीक देवता क्रोनस , ज़ीउस के पिता के साथ व्याख्या के माध्यम से पहचान है ; और दावा है कि ज़िसुथ्रोस द्वारा निर्मित ईख की नाव कम से कम बेरोसस के दिन तक, अर्मेनिया के "कोरसीरियन पर्वत" में बची रही. ज़िसुथ्रोस को एक राजा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो एक आर्डेट्स का पुत्र था, और उसने 18 सारोई पर शासन किया था । एक सरोस ( अक्कडियन में शार ) 3600 के लिए खड़ा है और इसलिए 18 सरोई का अनुवाद 64,800 वर्षों के रूप में किया गया था। एक सरोई या सरोस एक ज्योतिषीय शब्द है जिसे 29.5 दिनों के 222 चंद्र महीनों या 17.93 सौर वर्षों के बराबर 18.5 चंद्र वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है।
अन्य स्रोत-
ज़ियसुद्र का उल्लेख अन्य प्राचीन साहित्य में भी किया गया है, जिसमें द डेथ ऑफ़ गिलगमेश [16] और द पोएम ऑफ़ अर्ली रूलर्स , [17] और द इंस्ट्रक्शंस ऑफ़ शूरुपक का एक बाद का संस्करण शामिल है । [18]
मेसोपोटामिया के धर्म में ज़ीसुद्रा , भगवान द्वारा भेजी गई बाढ़ के उत्तरजीवी के रूप में बाइबिल के नूह के मोटे तौर पर प्रतिरूप । जब देवताओं ने मानवता को बाढ़ से नष्ट करने का फैसला किया था, तो भगवान एन्की (अक्कादियन ईए ), जो डिक्री से सहमत नहीं था , ने इसे ज़ीसुद्रा को प्रकट किया, जो अपनी विनम्रता और आज्ञाकारिता के लिए जाना जाता है। एनकी की आज्ञा के अनुसार ज़्यूसुद्र ने किया और एक विशाल नाव का निर्माण किया, जिसमें वह सफलतापूर्वक बाढ़ से बाहर निकला। बाद में, उसने खुद को देवताओं अन ( अनु ) और एनिल (बेल) के सामने दंडवत किया, और एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए एक इनाम के रूप में, ज़िसुद्र को अमरता दी गई । उत्तानपश्चिम देखें ।
बाढ़ मिथक
बाढ़ मिथक , जिसे बाढ़ मिथक भी कहा जाता है, कई पौराणिक कथाओं में से कोई भी जिसमें बाढ़ आम तौर पर अवज्ञाकारी मूल आबादी को नष्ट कर देती है। एक महान बाढ़ (जलप्रलय) के मिथक यूरेशिया और अमेरिका में फैले हुए हैं । बाढ़, कुछ अपवादों के साथ, पानी द्वारा एक प्रायश्चित है, जिसके बाद एक नए प्रकार की दुनिया का निर्माण होता है।
बाइबिल में वर्णित बाढ़ों का मिथक-
जलप्रलय का बाइबिल विवरण (उत्पत्ति 6:11–9:19) विशेषताएंबाढ़ कहानी के नायक के रूप में नूह । अपने खाते में, नूह को कुलपति के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने निर्दोष धर्मपरायणता के कारण, अपने दुष्ट समकालीनों के जलप्रलय में नाश होने के बाद मानव जाति को बनाए रखने के लिए परमेश्वर द्वारा चुना गया था। एक धर्मी व्यक्ति, नूह ने "प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह पाया" (उत्पत्ति 6:8)। इस प्रकार, जब परमेश्वर ने पृथ्वी के भ्रष्टाचार को देखा और इसे नष्ट करने का निश्चय किया, तो उसने नूह को आसन्न आपदा की दिव्य चेतावनी दी और उसे और उसके परिवार को बचाने का वादा करते हुए उसके साथ एक वाचा बाँधी। नूह को एक निर्माण करने का निर्देश दिया गया था सन्दूक , और परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार उसने सन्दूक में दुनिया की सभी प्रजातियों के जानवरों के नर और मादा नमूने लिए, जिससे स्टॉक की भरपाई की जा सकती थी। नतीजतन, इस कथा के अनुसार, पूरी जीवित मानव जाति नूह के तीन पुत्रों और उनकी पत्नियों के वंशज थे।
नूह के वीरतापूर्ण उत्तरजीविता के बाद, अरारत पर्वत पर सुरक्षित रूप से उतरने के बाद बाढ़ का धार्मिक अर्थ व्यक्त किया गया। फिर उसने एक वेदी का निर्माण किया जिस पर उसने भगवान को जले हुए बलिदान चढ़ाए, जिसने फिर खुद को एक समझौते के लिए बाध्य किया कि वह मानवता के खाते में पृथ्वी को फिर कभी श्राप न दे। तब परमेश्वर ने इस वाचा में अपने वादे की दृश्य गारंटी के रूप में आकाश में एक मेघ-धनुष स्थापित किया । परमेश्वर ने सृष्टि के समय दी गई अपनी आज्ञाओं को भी नवीनीकृत किया लेकिन दो परिवर्तनों के साथ: मानव जाति अब जानवरों को मार सकती थी और मांस खा सकती थी, और हत्या के लिए मनुष्यों को दंड दिया जाएगा। मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं की मूर्त समानताओं के बावजूदऔर बाइबिल की बाढ़, बाइबिल की कहानी का एक अनूठा हिब्रू परिप्रेक्ष्य है। बेबीलोनियन कहानियों में बाढ़ का विनाश देवताओं के बीच असहमति का परिणाम था, जबकि उत्पत्ति में यह मानव इतिहास के नैतिक भ्रष्टाचार का परिणाम था। मेसोपोटामिया के संस्करणों का आदिम बहुदेववाद बाइबिल की कहानी में एक धर्मी ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और परोपकार की पुष्टि में बदल गया है।
मेसोपोटामिया बाढ़ मिथक
के अनुसार एरिडु जेनेसिस , एक प्राचीन सुमेरियन धार्मिक महाकाव्य, देवताओं ने मिट्टी से मानव जाति को जमीन पर खेती करने, भेड़-बकरियों की देखभाल करने और देवताओं की पूजा को बनाए रखने के लिए तैयार किया। शहर जल्द ही बन गए, लेकिन, किसी कारण से, देवताओं ने बाढ़ से मानव जाति को नष्ट करने का फैसला किया। एन्की ( अक्कडियन : ईए), जो डिक्री से सहमत नहीं था, ने इसे प्रकट किया ज़िसुद्र , एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी विनम्रता और आज्ञाकारिता के लिए जाना जाता है। एनकी की आज्ञा के अनुसार ज़्यूसुद्र ने किया और एक विशाल नाव का निर्माण किया, जिसमें वह सफलतापूर्वक बाढ़ से बाहर निकला। बाद में, उसने खुद को देवताओं एन (अनु) और एनिल के सामने झुकाया, और एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए एक इनाम के रूप में, ज़िसुद्र को अमरत्व दिया गया।
संबंधित बेबीलोनियन में गिलगमेश महाकाव्य , उत्तानपश्चिम और उनकी पत्नी पौराणिक बाढ़ के उत्तरजीवी हैं, जिन्होंने अपने द्वारा निर्मित महान नाव में मानव और पशु जीवन को संरक्षित किया है। इस जोड़े को एक सन्दूक बनाने के दैवीय निर्देश को मानने के लिए एक इनाम के रूप में भगवान एनिल द्वारा देवता घोषित किया गया था।
एक अन्य मेसोपोटामिया मिथक की कहानी है अतरहासिस , एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे खुद को बचाने के लिए एक जहाज बनाने के लिए देवताओं में से एक द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद बाढ़ से बचाया गया था। यह कहानी खंडित ओल्ड बेबीलोनियन और असीरियन संस्करणों में संरक्षित है।
इन बेबीलोनियन पौराणिक कथाओं में बाढ़ की बाइबिल की कहानी के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और सन्दूक के निर्माण और प्रावधान, इसके प्लवनशीलता, और रेवेन और कबूतर के प्रेषण के साथ-साथ मानव द्वारा निभाई गई भूमिका जैसी विशेषताओं का स्रोत हैं। बाइबिल खाते में नायक।
अन्य बाढ़ मिथक
ग्रीक पौराणिक कथाओं में,प्रोमेथियस (मानव जाति का निर्माता) का पुत्र ड्यूकालियन , नूह के समकक्ष है। जब देवताओं के राजा ज़्यूस ने बाढ़ से पूरी मानवता को नष्ट करने का संकल्प लिया, तो ड्यूकालियन ने एक सन्दूक का निर्माण किया, जिसमें एक संस्करण के अनुसार, वह और उसकी पत्नी बाढ़ से बाहर निकले और माउंट पर्नासस पर उतरे ।
भारतीय बाढ़ पौराणिक कथाओं के अनुसार, आदमीमनु महान बाढ़ का एकमात्र उत्तरजीवी था , जो पहले आदमी नूह और आदम के हिब्रू बाइबिल के आंकड़ों की विशेषताओं को मिलाता था । शतपथ ब्राह्मण याद करते हैं कि कैसे मनु को एक मछली ने चेतावनी दी थी, जिस पर उसने दया की थी, कि एक बाढ़ पूरी मानवता को नष्ट कर देगी। इसलिए उसने मछली की सलाह के अनुसार एक नाव बनाई। जब बाढ़ आई, तो उसने इस नाव को मछली के सींग से बांध दिया और सुरक्षित रूप से एक पहाड़ की चोटी पर आराम करने के स्थान पर ले जाया गया। जब बाढ़ कम हुई, तो एकमात्र जीवित मानव मनु ने जल में मक्खन और खट्टे दूध की आहुति डालते हुए एक यज्ञ किया। एक वर्ष के बाद, जल से एक स्त्री का जन्म हुआ जिसने स्वयं को "मनु की पुत्री" घोषित किया। ये दोनों तब पृथ्वी को फिर से भरने के लिए एक नई मानव जाति के पूर्वज बन गए । महाभारत ("भारत राजवंश के महान महाकाव्य") में, मछली की पहचान भगवान ब्रह्मा के साथ की गई है , जबकि पुराणों ("प्राचीन विद्या") में यह हैमत्स्य , भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार ।
एज़्टेक का मानना था कि वर्तमान ब्रह्मांड से पहले चार संसार मौजूद थे। वे संसार, या "सूर्य", विपत्तियों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, और प्रत्येक सूर्य के अंत में मानवजाति को पूरी तरह से मिटा दिया गया था। चौथा सूर्य, नहुई-अटल, "चार-जल", 52 वर्षों तक चली एक विशाल बाढ़ में समाप्त हुआ। केवल एक पुरुष और एक महिला बच गए, एक विशाल सरू में शरण ली, लेकिन बाद में उन्हें कुत्तों में बदल दिया गया।
एनसाइक्लोपीनूह
इस विषय का संक्षिप्त सारांश पढ़ें
नूह , बाइबिल के नायक, नोए की वर्तनी भी है उत्पत्ति के पुराने नियम की किताब में बाढ़ की कहानी , दाख की बारी की खेती के प्रवर्तक, और, शेम, हाम और जेफेथ के पिता के रूप में, एक सेमिटिक वंशावली रेखा के प्रतिनिधि प्रमुख। कम से कम तीन बाइबिल स्रोत परंपराओं का एक संश्लेषण, नूह एक धर्मी व्यक्ति की छवि है जिसे एक पक्ष बनाया गया है इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के साथ वाचा , जिसमें आपदा के विरुद्ध प्रकृति की भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित है।
नूह उत्पत्ति 5:29 में लेमेक के पुत्र के रूप में और आदम के वंश में नौवें स्थान पर प्रकट होता है। जलप्रलय की कहानी (उत्पत्ति 6:11-9:19) में, उसे कुलपति के रूप में दर्शाया गया है, जिसे उसकी निष्कलंक धर्मपरायणता के कारण, उसके दुष्ट समकालीनों के जलप्रलय में नष्ट हो जाने के बाद मानव जाति को बनाए रखने के लिए परमेश्वर द्वारा चुना गया था। एक धर्मी व्यक्ति, नूह ने "प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह पाया" (उत्पत्ति 6:8)। इस प्रकार, जब परमेश्वर ने पृथ्वी के भ्रष्टाचार को देखा और इसे नष्ट करने का निश्चय किया, तो उसने नूह को आसन्न आपदा की दिव्य चेतावनी दी और उसे और उसके परिवार को बचाने का वादा करते हुए उसके साथ एक वाचा बाँधी । नूह को एक निर्माण करने का निर्देश दिया गया था सन्दूक , और परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार उसने सन्दूक में दुनिया की सभी प्रजातियों के जानवरों के नर और मादा नमूने लिए, जिससे स्टॉक की भरपाई की जा सकती थी। नतीजतन, इस कथा के अनुसार, पूरी जीवित मानव जाति नूह के तीन पुत्रों के वंशज थे। ऐसी वंशावली एक सार्वभौमिक ढाँचे को स्थापित करती है जिसके भीतर इज़राइल के विश्वास के पिता के रूप में इब्राहीम की बाद की भूमिका अपने उचित आयामों को ग्रहण कर सकती है।
बाढ़ की कहानी का इनसे गहरा नाता है सर्वनाश बाढ़ की बेबीलोनियन परंपराएँ जिसमेंउत्तानपश्चिम नूह के अनुरूप भूमिका निभाता है। ये पौराणिक कथाएँ बाइबिल की बाढ़ की कहानी की ऐसी विशेषताओं का स्रोत हैं जैसे कि सन्दूक का निर्माण और प्रावधान, उसका तैरना, और पानी का घटाव, साथ ही साथ मानव नायक द्वारा निभाई गई भूमिका। टैबलेट संख्या (XI)गिलगमेश महाकाव्य उत्तानपश्चिम का परिचय देता है, जो नूह की तरह, एक सन्दूक बनाने के लिए दिव्य निर्देश को ध्यान में रखते हुए लौकिक विनाश से बच गया।
The religious meaning of the Flood is conveyed after Noah’s heroic survival. He then built an altar on which he offered burnt sacrifices to God, who then bound himself to a pact never again to curse the earth on man’s account. God then set a rainbow in the sky as a visible guarantee of his promise in this covenant. God also renewed his commands given at creation but with two changes: man could now kill animals and eat meat, and the murder of a man would be punished by men.
Despite the tangible similarities of the Mesopotamian and biblical myths of the flood, the biblical story has a unique Hebraic perspective. In the Babylonian story the destruction of the flood was the result of a disagreement among the gods; in Genesis it resulted from the moral corruption of human history. The primitive polytheism of the Mesopotamian versions is transformed in the biblical story into an affirmation of the omnipotence and benevolence of the one righteous God. Again, following their survival, Utnapishtim and his wife are admitted to the circle of the immortal gods; but Noah and his family are commanded to undertake the renewal of history.
उत्पत्ति 9:20-27 में नूह से संबंधित कथा एक अलग चक्र से संबंधित है, जो जलप्रलय की कहानी से संबंधित नहीं लगती है। उत्तरार्द्ध में, नूह के पुत्र विवाहित हैं और उनकी पत्नियाँ उनके साथ सन्दूक में हैं; लेकिन इस आख्यान में वे अविवाहित प्रतीत होंगे, और न ही नूह की बेशर्म नशे की लत बाढ़ की कहानी के पवित्र नायक के चरित्र के साथ मेल खाती है। उत्पत्ति 9:20-27 में तीन अलग-अलग विषयों का पता लगाया जा सकता है: पहला, यह परिच्छेद कृषि की शुरुआत का वर्णन करता है, और विशेष रूप सेबेल , नूह के लिए; दूसरा, यह नूह के तीन पुत्रों के व्यक्तियों में प्रदान करने का प्रयास करता है,शेम,हाम, और जेफेथ, मानव जाति की तीन जातियों के पूर्वज और उनके ऐतिहासिक संबंधों के लिए कुछ हद तक खाते में; और तीसरा, कनान की अपनी निंदा के द्वारा , यह बाद में इस्राएलियों की विजय और उनके अधीनता के लिए एक परोक्ष औचित्य प्रदान करता है। कनानी - नूह के नशे में धुत होने और उसके पुत्र हाम का अनादर करने के परिणामस्वरूप नूह ने हाम के पुत्र कनान को श्राप दिया। यह घटना फ़िलिस्तीन के जातीय और सामाजिक विभाजन का प्रतीक हो सकती है: इज़राइली (शेम की रेखा से) कनान की पूर्व-इज़राइली आबादी से अलग हो जाएंगे (जो कि व्यभिचारी के रूप में चित्रित किया गया है), जो इब्रानियों के अधीन रहेंगे।
पेन्टाट्यूक के संकलन से पहले नूह की प्रतीकात्मक आकृति प्राचीन इस्राएल में जानी जाती थी । यहेजकेल (14:14, 20) उसके बारे में उस धर्मी व्यक्ति के आदर्श के रूप में बात करता है , जो इस्राएलियों के बीच अकेले, परमेश्वर के प्रतिशोध से बचेगा । नए नियम में, ल्यूक (3:36) के अनुसार सुसमाचार की वंशावली में नूह का उल्लेख किया गया है जो कि चित्रित करता है आदम से यीशु का वंश। यीशु जलप्रलय की कहानी का भी उपयोग करते हैं जो पुरुषों की एक सांसारिक पीढ़ी पर "नूह के दिनों में" बपतिस्मा के उदाहरण के रूप में आई थी, और नूह को अपने समय के पुरुषों के लिए पश्चाताप के उपदेशक के रूप में चित्रित किया गया है, जो स्वयं में एक प्रमुख विषय है यहूदी एपोक्रिफ़ल और रैबिनिकल लेखन।
जबकि मिथकों की रूपरेखा एक अतीत की अवधि से या अपने स्वयं के अलावा किसी अन्य समाज से आम तौर पर काफी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, उन मिथकों को पहचानना जो अपने समय और समाज में प्रभावी हैं हमेशा मुश्किल होता है। यह शायद ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि एक मिथक का अधिकार खुद को साबित करने से नहीं बल्कि खुद को पेश करने से होता है। इस अर्थ में एक मिथक का अधिकार वास्तव में "बिना कहे चला जाता है," और मिथक को विस्तार से केवल तभी रेखांकित किया जा सकता है जब उसका अधिकार अब निर्विवाद नहीं है, लेकिन किसी अन्य, अधिक व्यापक मिथक द्वारा किसी तरह से खारिज या दूर कर दिया गया है।
मिथ शब्द ग्रीक मिथोस से निकला है , जिसमें "शब्द", "कहने" और "कहानी," से लेकर "कथा" तक कई अर्थ हैं; मिथकों की निर्विवाद वैधता की तुलना लोगो से की जा सकती है , जिस शब्द की वैधता या सच्चाई को तर्क और प्रदर्शित किया जा सकता है। क्योंकि मिथक सबूत के प्रयास के बिना शानदार घटनाओं का वर्णन करते हैं, कभी-कभी यह माना जाता है कि वे बिना किसी वास्तविक आधार वाली कहानियां हैं, और यह शब्द झूठ या सबसे अच्छा गलत धारणा का पर्याय बन गया है। हालांकि, धर्म के अध्ययन में , मिथकों और कहानियों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है जो केवल असत्य हैं।
इस लेख के पहले भाग में ज्ञान की आधुनिक शाखाओं द्वारा प्रस्तावित विषय के विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए प्रकृति, अध्ययन, कार्यों, सांस्कृतिक प्रभाव और मिथकों के प्रकारों पर चर्चा की गई है। दूसरे भाग में, मिथक में जानवरों और पौधों की भूमिका के विशेष विषय की कुछ विस्तार से जांच की जाती है। विशिष्ट संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं को ग्रीक धर्म , रोमन धर्म और जर्मनिक धर्म के लेखों में शामिल किया गया है ।
मिथक की प्रकृति, कार्य और प्रकार
मिथक हर समाज में मौजूद है। वास्तव में, यह मानव संस्कृति का एक बुनियादी घटक प्रतीत होगा । क्योंकि विविधता इतनी महान है, मिथकों की प्रकृति के बारे में सामान्यीकरण करना मुश्किल है। लेकिन यह स्पष्ट है कि उनकी सामान्य विशेषताओं और उनके विवरण में लोगों के मिथक लोगों की आत्म-छवि को प्रतिबिंबित, अभिव्यक्त और अन्वेषण करते हैं। इस प्रकार मिथक का अध्ययन व्यक्तिगत समाजों और समग्र रूप से मानव संस्कृति दोनों के अध्ययन में केंद्रीय महत्व रखता है।
सैमेटिक संस्कृतियों में प्राप्त मिथकों के अनुसार
नूह (मनु:)को एक बड़ी नाव बनाने और नाव पर सभी जानवरों की एक जोड़ी लेने की चेतावनी दी गई थी। नाव को अरारात पर्वत जाना था ।
और उसके शीर्ष पर लंगर डालना था जो बाढ़ में बह गया था।
इन तीन प्राचीन संस्कृतियों में महान बाढ़ के बारे में बहुत समान कहानियाँ हैं।
बाइबिल के अनुसार इज़राइल में इस तरह की बड़ी बाढ़ का कारण कोई महान नदियाँ नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि
इब्रानियों ने उर के इब्राहीम के लिए अपनी उत्पत्ति का पता लगाया जो मेसोपोटामिया में है।
भारतीय इतिहास में यही इब्राहीम ब्रह्मा है।
जबकि टिगरिस (दजला)और यूफ्रेट्स (फरात)बाढ़ और अक्सर बदलते प्रवेश में, उनकी बाढ़ उतनी बड़े पैमाने पर नहीं होती है।
एक दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी क्रिया "Meander "का अर्थ है, जिसका उद्देश्य लक्ष्यहीनता से एक तुर्की नदी के नाम से आता है।
जो अपने परिवेश को बदलने के लिए कुख्यात है।
सिंधु और गंगा बाढ़ आती हैं लेकिन मनु द्वारा वर्णित प्रलय जैसा कुछ भी नहीं है।
महान जलप्रलय 5000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ जब भूमध्य सागर काला सागर में टूट गया।
इसने यूक्रेन, अनातोलिया, सीरिया और मेसोपोटामिया को विभिन्न दिशाओं में (littoral) निवासियों के प्रवास का नेतृत्व किया।
ये लोग अपने साथ बाढ़ और उसके मिथक की अमिट स्मृति को ले गए।
अक्कादियों ने कहानी को आगे बढ़ाया क्योंकि उनके लिए सुमेरियन वही थे जो लैटिन यूरोपीय थे।
सभी अकाडियन शास्त्रियों को सुमेरियन, एक मृत भाषा सीखना था, जैसे कि सभी शिक्षित यूरोपीय मध्य युग में लैटिन सीखते हैं।
ईसाइयों ने मिथक को शामिल किया क्योंकि वे पुराने नियम को अवशोषित करते थे क्योंकि उनके भगवान जन्म से यहूदी थे।
बाद में उत्पन्न हुए धर्मों ने मिथक को शामिल नहीं किया। जोरास्ट्रियनवाद जो कि भारतीय वैदिक सन्दर्भों में साम्य के साथ दुनियाँ के रंगमञ्च पर उपस्थित होता है; ने मिथक को छोड़ दिया।
अर्थात् पारसी धर्म ग्रन्थ अवेस्ता में जल प्रलय के स्थान पर यम -प्रलय ( हिम -प्रलय ) का वर्णन है
जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। इसी तरह इस्लाम जो यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और कुछ स्थानीय अरब रीति-रिवाजों का मिश्रण है, जो मिथक को छोड़ देता है। सभी मनु के जल प्रलय के मिथकों में विश्वास करते हैं ।
____________________________________
सुमेरियन और भारतीयों के बीच एक और आम मिथक है सात ऋषियों का है।
सुमेरियों का मानना था कि उनका ज्ञान और सभ्यता सात ऋषियों से उत्पन्न हुई थी। हिंदुओं में सप्त ऋषियों का मिथक है जो इन्द्र से अधिक शक्तिशाली थे।
यह सुमेरियन कैलेंडर से है कि हमारे पास अभी भी सात दिन का सप्ताह है।
उनके पास एक दशमलव प्रणाली भी नहीं थी जिसे भारत ने शून्य के साथ आविष्कार किया था। उनकी गिनती का आधार दस के बजाय साठ था ।
और इसीलिए हमारे पास अभी भी साठ सेकंड से एक मिनट, साठ मिनट से एक घंटे और एक सर्कल में 360 डिग्री है।
सीरिया में अनदेखी मितन्नी राजधानी को वासु-खन्नी अर्थात समृद्ध -पृथ्वी का नाम दिया गया था।
मनु ने अयोध्या को बसाया यह तथ्य वाल्मीकि रामायण में वर्णित है।
वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है, "अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या"
अथर्ववेद १०/२/३१ में वर्णित है।
वास्तव में यह सारा सूक्त ही अयोध्या पुरी के निर्माण के लिए है।
नौ द्वारों वाला हमारा यह शरीर ही अयोध्या पुरी बन सकता है।
अयोध्या का समानार्थक शब्द "अवध" है ।
"मध्य-एशिया (तुर्की) में मनु की अवधारणा-
प्राचीन काल में एशिया - माइनर ---(छोटा एशिया), जिसका ऐतिहासिक नाम -करण अनातोलयियो के रूप में भी हुआ है ।
यूनानी इतिहास कारों विशेषत: होरेडॉटस् ने अनातोलयियो के लिए एशिया माइनर शब्द का प्रयोग किया है ।
जिसे आधुनिक काल में तुर्किस्तान अथवा टर्की नाम से भी जानते हैं ।
यहाँ की पार्श्व -वर्ती संस्कृतियों में मनु की प्रसिद्धि उन सांस्कृतिक-अनुयायीयों ने अपने पूर्व-पुरुष { Pro -Genitor } के रूप में स्वीकृत की है ।
मनु को पूर्व- पुरुष मानने वाली जन-जातियाँ प्राय: भारोपीय वर्ग की भाषाओं का सम्भाषण करती रहीं हैं ।
वस्तुत: भाषाऐं सैमेटिक वर्ग की हो अथवा हैमेटिक वर्ग की अथवा भारोपीय , सभी भाषाओं मे समानता का कहीं न कहीं सूत्र अवश्य है।
जैसा कि मिश्र की संस्कृति में मिश्र का प्रथम पुरुष जो देवों का का भी प्रतिनिधि था , वह था "मेनेस्" (Menes)अथवा मेनिस् (Menis) इस संज्ञा से अभिहित था ।
मेनिस ई०पू० 3150 के समकक्ष मिश्र का प्रथम शासक और मेंम्फिस (Memphis) नगर में जिसका निवास था
"मेंम्फिस "प्राचीन मिश्र का महत्वपूर्ण नगर जो नील नदी की घाटी में आबाद है ।
तथा यहीं का पार्श्ववर्ती देश फ्रीजिया (Phrygia)के मिथकों में भी मनु की जल--प्रलय का वर्णन मिऑन (Meon)के रूप में है ।
मिऑन अथवा माइनॉस का वर्णन ग्रीक पुरातन कथाओं में क्रीट के प्रथम राजा के रूप में है । जो ज्यूस तथा यूरोपा का पुत्र है ।
और यहीं एशिया- माइनर के पश्चिमीय समीपवर्ती लीडिया( Lydia) देश वासी भी इसी मिअॉन (Meon) रूप में मनु को अपना पूर्व पुरुष मानते थे।
इसी मनु के द्वारा बसाए जाने के कारण लीडिया देश का प्राचीन नाम मेऑनिया "Maionia" भी था ।
ग्रीक साहित्य में विशेषत: होमर के काव्य में "मनु" को (Knossos) क्षेत्र का का राजा बताया गया है ।
ग्रीक पौराणिक कथाओं में मिनोस कौन था ?
ग्रीक पौराणिक कथाओं में मिनोस क्रेते द्वीप के राजा और शासक थे। उन्हें ज़्यूस और यूरोपा का पुत्र माना जाता था । किंवदंतियों के भीतर, मिनोस को कई उपलब्धियों का श्रेय दिया जाता है, जिसमें पोसिडॉन की इच्छा के माध्यम से सिंहासन प्राप्त करना और एजियन सागर के कई द्वीपों का उपनिवेश करना शामिल है। उन्हें कानूनों का एक सफल कोड बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। मिनोस ग्रीक पौराणिक कथाओं की कई कहानियों में एक शक्तिशाली राजा के रूप में एक चरित्र के रूप में प्रकट होता है जो न्याय और कभी-कभी अत्याचार के साथ शक्ति रखता है। ग्रीक किंवदंतियों के अलावा, विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि मिनोस कांस्य युग के शासकों को दी गई एक शाही उपाधि हो सकती है।
"कनान देश की कैन्नानाइटी(Canaanite ) संस्कृति में बाल -मिऑन के रूप में भारतीयों के बल और मनु (Baal- meon) और यम्म (Yamm) देव के रूप मे वैदिक देव यम से साम्य संयोग नहीं अपितु संस्कृतियों की एकरूपता की द्योतक है ।
यम और मनु दौनों को सजातिय रूप में सूर्य की सन्तानें बताया है।
_________________________________________
विश्व संस्कृतियों में यम का वर्णन --- यहाँ भी कनानी संस्कृतियों में भारतीय पुराणों के समान यम का उल्लेख यथाक्रम नदी ,समुद्र ,पर्वत तथा न्याय के अधिष्ठात्री देवता के रूप में हुआ है।
कनान प्रदेश से ही कालान्तरण में सैमेटिक हिब्रु परम्पराओं का विकास हुआ था ।
स्वयम् कनान शब्द भारोपीय है , केन्नाइटी भाषा में कनान शब्द का अर्थ होता है मैदान अथवा जड्•गल यूरोपीय कोलों अथवा कैल्टों की भाषा पुरानी फ्रॉन्च में कनकन (Cancan)आज भी जड्.गल को कहते हैं ।
और संस्कृत भाषा में कानन =जंगल सर्वविदित ही है। परन्तु कुछ बाइबिल की कथाओं के अनुसार कनान एक पूर्व पुरुष था --जो हेम (Ham)की परम्पराओं में एनॉस का पुत्र था।
जब कैल्ट जन जाति का प्रव्रजन (Migration) बाल्टिक सागर से भू- मध्य रेखीय क्षेत्रों में हुआ।
तब मैसॉपोटामिया की संस्कृतियों में कैल्डिया के रूप में इनका विलय हुआ ।
तब यहाँ जीव सिद्ध ( जियोसुद्द )अथवा नूह के रूप में मनु की किश्ती और प्रलय की कथाओं की रचना हुयी ।
और तो क्या ? यूरोप का प्रवेश -द्वार कहे जाने वाले ईज़िया तथा क्रीट ( Crete ) की संस्कृतियों में मनु आयॉनिया लोगों के आदि पुरुष माइनॉस् (Minos)के रूप में प्रतिष्ठित हए।
भारतीय संस्कृति की पौराणिक कथाऐं इन्हीं घटनाओं ले अनुप्रेरित हैं।
_________________________________________
भारतीय पुराणों में मनु और श्रृद्धा का सम्बन्ध वस्तुत: मन के विचार (मनन ) और हृदय की आस्तिक भावना (श्रृद्धा ) के मानवीय-करण (personification) रूप है ।
शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ में मनु को श्रृद्धा-देव
(श्रृाद्ध -देव) कह कर सम्बोधित किया है।
तथा बारहवीं सदी में रचित श्रीमद्भागवत् पुराण में वैवस्वत् मनु तथा श्रृद्धा से ही मानवीय सृष्टि का प्रारम्भ माना गया है। 👇
सतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ में " मनवे वै प्रात: "वाक्यांश से घटना का उल्लेख आठवें अध्याय में मिलता है।
सतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ में मनु को श्रृद्धा-देव कह कर सम्बोधित किया है।👇
--श्रृद्धा देवी वै मनु (काण्ड-१--प्रदण्डिका १) श्रीमद्भागवत् पुराण में वैवस्वत् मनु और श्रृद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारम्भ माना गया है--
👇
"ततो मनु: श्राद्धदेव: संज्ञायामास भारत श्रृद्धायां जनयामास दशपुत्रानुस आत्मवान"(9/1/11)
छन्दोग्य उपनिषद में मनु और श्रृद्धा की विचार और भावना रूपक व्याख्या भी मिलती है।
"यदा वै श्रृद्धधाति अथ मनुते नाSश्रृद्धधन् मनुते " __________________________________________
जब मनु के साथ प्रलय की घटना घटित हुई तत्पश्चात् नवीन सृष्टि- काल में :– असुर (असीरियन) पुरोहितों की प्रेरणा से ही मनु ने पशु-बलि दी थी।
" किल आत्आकुलीइति ह असुर ब्रह्मावासतु:।
तौ हो चतु: श्रृद्धादेवो वै मनु: आवं नु वेदावेति।
तौ हा गत्यो चतु:मनो वाजयाव तु इति।।
असुर लोग वस्तुत: मैसॉपोटमिया के अन्तर्गत असीरिया के निवासी थे।
सुमेर भी इसी का एक अवयव है ।
अत: मनु और असुरों की सहवर्तीयता प्रबल प्रमाण है मनु का सुमेरियन होना ।
बाइबिल के अनुसार असीरियन लोग यहूदीयों के सहवर्ती सैमेटिक शाखा के थे।
सतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ में मनु की वर्णित कथा हिब्रू बाइबिल में यथावत है --- देखें एक समानता !
👇👇👇👇
"हिब्रू बाइबिल में नूह का वर्णन:-
👇
बाइबिल उत्पत्ति खण्ड (Genesis)- "नूह ने यहोवा (ईश्वर) कहने पर एक वेदी बनायी ;
और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ की वेदी पर होम-बलि चढ़ाई।(उत्पत्ति-8:20) ।👇
____________________________________
" And Noah builded an alter unto the Lord Jehovah and took of the every clean beast, and of every clean fowl or birds, and offered ( he sacrificed ) burnt offerings on the alter
_________________________________________
Genesis-8:20 in English translation... -------------------------------------------------------------------
हृद् तथा श्रृद् शब्द वैदिक भाषा में मूलत: एक रूप में ही हैं ; रोम की सांस्कृतिक भाषा लैटिन आदि में क्रेडॉ "credo" का अर्थ :--- मैं विश्वास करता हूँ ।
तथा क्रिया रूप में credere---to believe लैटिन क्रिया credere--- का सम्बन्ध भारोपीय धातु
"Kerd-dhe" ---to believe से है ।
साहित्यिक रूप इसका अर्थ "हृदय में धारण करना –(to put On's heart-- पुरानी आयरिश भाषा में क्रेटिम cretim रूप --- वेल्स भाषा में (credu ) और संस्कृत भाषा में श्रृद्धा(Srad-dha)---faith,
इस शब्द के द्वारा सांस्कृतिक प्राक्कालीन एक रूपता को वर्णित किया है ।
__________________________________________
श्रृद्धा का अर्थ :–Confidence, Devotion आदि हार्दिक भावों से है ।
प्राचीन भारोपीय (Indo-European) रूप कर्ड (kerd)--हृदय है ।
ग्रीक भाषा में श्रृद्धा का रूप "Kardia" तथा लैटिन में "Cor " है ।
आरमेनियन रूप ---"Sirt" पुरातन आयरिश भाषा में--- "cride" वेल्स भाषा में ---"craidda" हिट्टी में--"kir" लिथुअॉनियन में--"sirdis" रसियन में --- "serdce" पुरानी अंग्रेज़ी --- "heorte". जर्मन में --"herz" गॉथिक में --hairto " heart" ब्रिटॉन में---- kreiz "middle" स्लेवॉनिक में ---sreda--"middle ..
यूनानी ग्रन्थ "इलियड तथा ऑडेसी "महा काव्य में प्राचीनत्तम भाषायी साम्य तो है ही देवसूचीयों मेंभी साम्य है ।
आश्चर्य इस बात का है कि ..आयॉनियन भाषा का शब्द माइनॉस् तथा वैदिक शब्द मनु: की व्युत्पत्तियाँ (Etymologies)भी समान हैं।
जो कि माइनॉस् और मनु की एकरूपता(तादात्म्य) की सबसे बड़ी प्रमाणिकता है।
क्रीट (crete) माइथॉलॉजी में माइनॉस् का विस्तृत विवेचन है, जिसका अंग्रेजी रूपान्तरण प्रस्तुत है ।👇
------------------------------------------------------------- .. Minos and his brother Rhadamanthys
जिसे भारतीय पुराणों में रथमन्तः कहा है ।
And sarpedon wereRaised in the Royal palace of Cnossus-... Minos Marrieged pasiphae- जिसे भारतीय पुराणों में प्रस्वीः प्रसव करने वाली कहा है !
शतरूपा भी इसी का नाम था यही प्रस्वीः या पैसिफी सूर्य- देव हैलिअॉस् (Helios) की पुत्री थी।
क्यों कि यम और यमी भाई बहिन ही थे ।
जिन्हें मिश्र की संस्कृतियों में पति-पत्नी के रूप में भी वर्णित किया है ।
Pasiphae is the Doughter of the sun god (helios ) हैलीअॉस् के विषय में एक तथ्य और स्पष्ट कर दें कि यूनानीयों का यही हैलीअॉस् मैसोपॉटामियाँ की पूर्व सैमेटिक भाषाओं ---हिब्रू आरमेनियाँ तथा अरब़ी आदि में "ऐल " (El) के रूप में है।
इसी शब्द का हिब्रू भाषा में बहुवचन रूप ऐलॉहिम Elohim )है ।
इसी से अरब़ी में " अल् --इलाह के रूप में अल्लाह शब्द का विकास हुआ है।
विश्व संस्कृतियों में सूर्य ही प्रत्यक्ष सृष्टि का कारण है
अत: यही प्रथम देव है ।
भारतीय वैदिक साहित्य में " अरि " शब्द का प्राचीनत्तम अर्थ "ईश्वर" है ।
वेद में अरि शब्द के अर्थ हैं ईश्वर तथा घर "और लौकिक संस्कृत में अरि शब्द केवल शत्रु के अर्थ में रूढ़ हो गया
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १३६ वें सूक्त का ५वाँ श्लोक "अष्टौ अरि धायसो गा:
पूर्ण सूक्त इस प्रकार है ।👇
पूर्वामनु प्रयतिमा ददे वस्त्रीन्युक्ताँ अष्टवरि धायसो गा: । सुबन्धवो ये विश्वा इव व्रा अनस्वन्त: श्रव एेषन्त पज्रा: ऋ०2/126/5/
कुछ भाषा -विद् मानते हैं कि ग्रीक भाषा के हेलिअॉस् (Helios)का सम्बन्ध भारोपीय धातु स्वेल (sawel ) से प्रस्तावित करते हैं।
अवेस्ता ए जेन्द़ में हवर (hvar )-- सूर्य , प्रकाश तथा स्वर्ग लिथुऑनियन सॉले (Saule ) गॉथिक-- सॉइल (sauil) वेल्स ---हॉल (haul) पुरानी कॉर्निश-- हिऑल (heuul) आदि शब्दों का रूप साम्य स्पष्ट है ।
परन्तु यह भाषायी प्रवृत्ति ही है कि संस्कृत भाषा में अर् धातु "हृ "धातु के रूप में पृथक विकसित हुयी।
वैदिक "अरि" का रूप लौकिक संस्कृत भाषा में "हरि" हो कर ईश्वरीय अर्थ को तो प्रकट करता है
परन्तु इरि रूप में शत्रु का अर्थ रूढ़ हो जाता है ।
कैन्नानाइटी संस्कृति में यम "एल" का पुत्र है।
और भारतीय पुराणों में सूर्य अथवा विवस्वत् का पुत्र.. इसी लिए भी हेलिऑस् ही हरिस् अथवा अरि: का रूपान्तरण है ।👇
अरि से हरि और हरि से सूर्य का भी विकास सम्भवत है जैसे वीर: शब्द सम्प्रसारित होकर आर्य रूप में विकसित हो जाता है।
____________________________________
जिसमें अज् धातु का संयोजन है:–अज् धातु अर् (ऋ) धातु का ही विकास क्रम है जैसे वीर्य शब्द से बीज शब्द विकसित हुआ ।संस्कृत साहित्य में सूर्य को समय का चक्र (अरि) कह कर वर्णित किया गया है।
."वैदिक सूक्तों में अरिधामश् शब्द का अर्थ अरे: ईश्वरस्य धामश् लोकं इति अरिधामश् रूप में है।
----------------------------------------------------------
वास्तव में पैसिफी और माइनॉस् दौनों के पिता सूर्य ही थे ।
ऐसी प्राचीन सांस्कृतिक मान्यताऐं थी ।
ओ३म् (अमॉन्) रब़ तथा ऐल जिससे अल्लाह शब्द का विकास हुआ प्राचीनत्तम संस्कृतियों में केवल सूर्य के ही वाचक थे ।
आज अल्लाह शब्द को लेकर मुफ़्ती और मौलाना लोग फ़तवा जारी करते हैं और कहते हैं कि यह एक इस्लामीय अरब़ी शब्द है।
--जो गैर इस्लामीय के लिए हराम है ।
परन्तु यह अल्लाह वैदिक अरि का असीरियन रूप है । मनु के सन्दर्भ में ये बातें इस लिए स्पष्ट करनी पड़ी हैं कि क्योंकि अधिकतर संस्कृतियों में मनु को मानवों का आदि तथा सूर्य का ही पुत्र माना गया है।
यम और मनु को भारतीय पुराणों में सूर्य (अरि) का पुत्र माना गया है।
क्रीट पुराणों में इन्द्र को (Andregeos) के रूप में मनु का ही छोटा भाई और हैलीअॉस् (Helios) का पुत्र कहा है।
इधर चतुर्थ सहस्राब्दी ई०पू० मैसॉपोटामियाँ दजला- और फ़रात का मध्य भाग अर्थात् आधुनिक ईराक की प्राचीन संस्कृति में मेनिस् (Menis)अथवा मेैन (men) के रूप में एक समुद्र का अधिष्ठात्री देवता है।
यहीं से मेनिस का उदय फ्रीजिया की संस्कृति में हुआ था । यहीं की सुमेरीयन सभ्यता में यही मनुस् अथवा नूह के रूप में उदय हुआ, जिसका हिब्रू परम्पराओं नूह के रूप वर्णन में भारतीय आर्यों के मनु के समान है।
मनु की नौका और नूह की क़िश्ती
दोनों प्रसिद्ध हैं।
👇👇👇👇
"जर्मनिक संस्कृतियों में मनु: (मैनुस)Mannus का आख्यान-👇
____________________________________
Mannus, according to the Roman writer Tacitus, was a figure in the creation myths of the Germanic tribes. Tacitus is the only source of these myths.Tacitus wrote that Mannus was the son of Tuisto and the progenitor of the three Germanic tribes Ingaevones, Herminones and Istvaeones. In discussing the German tribes Tacitus wrote:I n ancient lays, their only type of historical tradition, they celebrate Tuisto, a god brought forth from the earth.They attribute to him a son, Mannus, the source and founder of their people, and to Mannus three sons, from whose names those nearest the Ocean are called Ingvaeones, those in the middle Herminones, and the rest Istvaeones. Some people, inasmuch as antiquity gives free rein to speculation, maintain that there were more sons born from the god and hence more tribal designations—Marsi, Gambrivii, Suebi, and Vandilii—and that those names are genuine and ancient. (Germania, chapter 2)
Several authors consider the name Mannus in Tacitus's work to stem from an Indo-European root; see Indo-European cosmogony § Linguistic evidence.
The Latinized name Mannus is evidently of some relation to Proto-Germanic *Mannaz, "man".
Mannus again became popular in literature in the 16th century, after works published by Annius de Viterbo and Johannes Aventinus purported to list him as a primeval king over Germany and Sarmatia.
In the 19th century, F. Nork wrote that the names of the three sons of Mannus can be extrapolated as Ingui, Irmin, and Istaev or Iscio. A few scholars like Ralph T. H. Griffith have expressed a connection between Mannus and the names of other ancient founder-kings, such as Minos of Greek mythology, and Manu of Hindu tradition.
Guido von List incorporated the myth of Mannus and his sons into his occult beliefs which were later adopted into Nazi occult beliefs.
अनुवाद:-
मन्नुस, रोमन लेखक टैसिटस के अनुसार, जर्मनिक जनजातियों के उत्पत्ति मिथकों में एक व्यक्ति था। रोमन इतिहासकार टैसिटस इन मिथकों का एकमात्र स्रोत है।
टैसिटस ने लिखा है कि मन्नस ( Mannus)ट्यूइस्टो ( _त्वष्टा) का पुत्र था और ज्सने तीन जर्मनिक जनजातियों १-इंगेवोन्स, २-हर्मिनोन्स और ३-इस्तवाइओन्स के पूर्वज रूप में स्वयं को व्याख्यायित किया।
जर्मन जनजातियों पर चर्चा करते हुए टैकिटस ने लिखा: कि
प्राचीन काल में, उनकी एकमात्र प्रकार की ऐतिहासिक परंपरा में, जर्मन लोग ट्यूइस्टो का जश्न (उत्सव)मनाते हैं, जो कि पृथ्वी से लाए गए देवता हैं।
वे उसके लिए एक पुत्र, मन्नुस, उनके लोगों के स्रोत और संस्थापक, और मन्नू के तीन पुत्रों को श्रेय देते हैं, जिनके नाम से महासागर के निकटतम लोगों को (इंगवीओन्स ) कहा जाता है, जो मध्य हर्मिनोन्स में हैं, और बाकी इस्तवाईओन्स हैं। कुछ लोग, चूंकि इनकी पुरातनता अटकलों पर पूरी तरह से लगाम लगाती है, यह बनाए रखती है और विश्वास है कि देव से और अधिक पुत्र पैदा हुए थे और इसलिए अधिक आदिवासी पदनाम-मार्सी, गम्ब्रिवी, सुएबी, और वंदिली-आदि हैं और ये नाम वास्तविक और प्राचीन हैं। (जर्मनिया, अध्याय 2)
कई लेखक टैसिटस के काम में मन्नस नाम को एक इंडो-यूरोपियन मूल से उत्पन्न मानते हैं;
लैटिनकृत नाम मन्नस स्पष्ट रूप से प्रोटो-जर्मनिक * मन्नज, "आदमी" से कुछ संबंध रखता है।
मेनुस फिर से 16 वीं शताब्दी में साहित्य में लोकप्रिय हो गया, एनियस डी विटर्बो और जोहान्स एवेंटिनस द्वारा प्रकाशित कार्यों के बाद उन्हें जर्मनी और सरमाटिया पर एक आदिम राजा के रूप में जिसे सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया।
19 वीं सदी में एफनोर्क ने लिखा है कि "मानुस के तीन बेटों के नाम इंगुई, इरमिन और इस्तैव या इस्सियो के रूप में निकाले जा सकते हैं। कुछ विद्वान जैसे 'राल्फ टी.एचग्रिफ़िथ" ने मानस और अन्य प्राचीन संस्थापक-राजाओं के नामों के बीच एक संबंध व्यक्त किया है, जैसे ग्रीक पौराणिक कथाओं के मिनोस और भारतीय परंपरा के मनु में है।
गुइडो वॉन लिस्ट" ने मन्नस और उसके बेटों के मिथक को अपने मनोगत विश्वासों में शामिल किया, जिन्हें बाद में नाज़ीयों ने मनोगत विश्वासों में अपनाया गया।
References
[1]Publishers, Struik; Stanton, Janet Parker, Alice Mills, Julie (2007-11-02). Mythology: Myths, Legends and Fantasies. Struik. pp. 234–. ISBN 9781770074538. Archived from the original on 2014-07-04. Retrieved 6 April 2014.
[2]The Phonology/paraphonology Interface and the Sounds of German Across Time, p.64, Irmengard Rauch, Peter Lang, 2008
[3]Tales of the Barbarians: Ethnography and Empire in the Roman West, p. 40, Greg Woolf, John Wiley & Sons, 01-Dec-2010
[4]"Word and Power in Mediaeval Bulgaria", p. 167. By Ivan Biliarsky, Brill, 2011
[5]Mitra-Varuna: An Essay on Two Indo-European Representations, p. 87, by Georges Dumézil, Zone, 1988. The question remains whether one can phonetically link this Latin mani- "(dead) man" the *manu- which, apart from the Sanskrit Manu (both the name and the common noun for "man"), has given, in particular, the Germanic Mannus (-nn- from *-nw- regularly), mythical ancestor of the Germans (...), the Gothic manna "man" ... and the Slavic monžǐ."
[6]"man | Origin and meaning of man by Online Etymology Dictionary". www.etymonline.com. Archived from the original on 2020-08-14. Retrieved 2020-09-28.
[7]Germany and the Holy Roman Empire: Volume I: Maximilian I to the Peace of Westphalia, 1493-1648, p.110, Joachim Whaley, Oxford University Press, 2012
[8]Historian in an age of crisis: the life and work of Johannes Aventinus, 1477-1534, p. 121 Gerald Strauss, Harvard University Press, 1963
[9]William J. Jones, 1999, "Perceptions in the Place of German in the Family of Languages" in Images of Language: Six Essays on German Attitudes, p9 ff.
[10]Populäre Mythologie, oder Götterlehre aller Völker, p. 112, F. Nork, Scheible, Rieger & Sattler (1845)
[11]"A Classical Dictionary of India: Illustrative of the Mythology, Philosophy, Literature, Antiquities, Arts, Manners, Customs &c. of the Hindus", p. 383, by John Garrett, Higginbotham and Company (1873)
[12]़Goodrick-Clarke, Nicholas (1992). The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology. NYU Press. pp. 56–. ISBN 9780814730607. Archived from the original on 4 July 2014. Retrieved 6 April 2014.
Grimm, Jacob (1835). Deutsche Mythologie (German Mythology); From English released version Grimm's Teutonic Mythology (1888); Available online by Northvegr © 2004-2007: Chapter 15, page 2 Archived 2012-01-14 at the Wayback Machine File retrieved 12-08-2011.
Tacitus. Germania (1st Century AD). (in Latin...
जर्मन वर्ग की प्राचीन सांस्कृतिक भाषों में क्रमशः यमॉ Yemo- (Twice) -जुँड़वा यमल तथा मेन्नुस Mannus- मनन (Munan ) का वर्णन करने वाला एक रूपता आधार है ।
अर्थात् विचार शक्ति का अधिष्ठाता मनु है ।
और उन मनन "Munan" में संयम का रूप यम है ।
फ्राँस भाषा में यम शब्द (Jumeau )के रूप में है । रोमन इतिहास कारों में "टेकट्टीक्स" (Tacitus) जर्मन जाति से सम्बद्ध इतिहास पुस्तक "जर्मनिका " में लिखता हैं।
" अपने प्राचीन गाथा - गीतों में वे ट्युष्टो अर्थात् ऐसा ईश्वर जो पृथ्वी से निकल कर आता है।
मैनुस् उसी का पुत्र है वही जन-जातिों का पिता और संस्थापक है।
जर्मनिक जन-जातियाँ उसके लिए उत्सव मनाती हैं । मैनुस् के तीन पुत्रों को वह नियत करते हैं ।
जिनके पश्चात मैन (Men)नाम से बहुत से लोगों को पुकारा जाता है ।
( टेकट्टीक्स (Tacitus).. जर्मनिका अध्याय (2)
100 ईस्वी सन् में लिखित ग्रन्थ.... --------------------------------------------------------------
यम शब्द रोमन संस्कृति में (Gemellus ) के रूप में है
जो लैटिन शब्द (Jeminus) का संक्षिप्त रूप है।
रोमन मिथकों के मूल-पाठ (Text )में मेन्नुस् (Mannus) ट्युष्टो (Tuisto )का पुत्र तथा जर्मन आर्य जातियों के पूर्व पुरुष के रूप में वर्णित है ।👇
-- A. roman text(dated) ee98) tells that Mannus the Son of Tvisto Was the Ancestor of German Tribe or Germanic people "
इधर जर्मन आर्यों के प्राचीन मिथकों "प्रॉज़एड्डा आदि में उद्धरण है :–👇
__________________________________________
" Mannus progenitor of German tribe son of tvisto in some Reference identified as Mannus "
उद्धरण अंश (प्रॉज- एड्डा ) वस्तुतः ट्युष्टो ही भारतीय आर्यों का देव त्वष्टा है।
,जिसे विश्व कर्मा कहा है जिसे मिश्र की पुरा कथाओं में "तिहॉती" ,जर्मन भाषा में प्रचलित डच (Dutch )का मूल रूप "त्वष्टा" शब्द है ।
गॉथिक शब्द (Thiuda )के रूप में भी "त्वष्टा" शब्द है प्राचीन उच्च जर्मन में यह शब्द (Diutisc )तथा जर्मन में (Teuton )है ।
और मिश्र की संस्कृति में (tehoti) के रूप में वर्णित है।
जर्मन पुराणों में भारतीयों के समान यम और मनु सजातीय थे ।
भारतीय संस्कृति में मनु: और यम: दोनों ही विवस्वान् (सूर्य) की सन्तान थे ।
इसी लिए इन्हें वैवस्वत् कहा गया यह बात जर्मनिक जन-जाति में भी प्रसिद्ध थी।
The Germanic languages have lnformation About both ...Ymir ------------------------------------------------------------ यमीर ( यम) and (Mannus) मेनुस् Cognate of Yemo and Manu"..मेन्नुस् मूलक मेन "Man" शब्द भी डच भाषा का है ।
जिसका रूप जर्मन तथा ऐंग्लो - सेक्शन भाषा में मान्न "Mann" रूप है ।
प्रारम्भ में जर्मन लोग "मनुस्" का वंशज होने के कारण स्वयं को मान्न कहते थे।
मनु का उल्लेख ऋग्वेद काल से ही मानव -सृष्टि के आदि प्रवर्तक एवम् समग्र मानव जाति के आदि- पिता के रूप में मान्य हो गया था।
__________________________________________
वैदिक सन्दर्भों मे प्रारम्भिक चरण में मनु तथा यम का अस्तित्व अभिन्न था कालान्तरण में मनु को जीवित मनुष्यों का तथा यम को मृत मनुष्यों के लोक का आदि पुरुष माना गया ... _____________________________________ जिससे यूरोपीय भाषा परिवार में मैन (Man) शब्द आया ।
मैने प्रायः उन्हीं तथ्यों का पिष्ट- पेषण भी किया है जो मेरे विचार बलाघात का लक्ष्य है।
और मुझे अभिप्रेय भी ..
जर्मन माइथॉलॉजी में यह तथ्य प्रायः प्रतिध्वनित होता रहता है ।👇 ------------------------------------------------------------
"The ancient Germanic tribes believeb that they had acmmon origin all of them Regarding as their fore father "mannus" the son of god "tuisco" mannus was supposed to have and three sons from whom had sprung the istaevones the lngavones" ------------------------------------------------------------------
हम पूर्व में इस बात को कह चुके हैं , कि क्रीट मिथकों में माइनॉस् (Minos )ज्युस तथा यूरोपा की प्रथम सन्तान है । 👇
यूनानीयों का ज्यूस ही वैदिक संहिताओं में (द्यौस् )के रूप में वर्णित है विदित हो कि यूरोप महाद्वीप की संज्ञा का आधार यही यूरोपा शब्द ही है।
.यहाँ एक तथ्य विद्वानों से निवेदित है कि मिथकों में वर्णित घटनाऐं और पात्र प्राचीन होने के कारण परम्परागत रूप से सम्वहन होते होते अपने मूल रूप से प्रक्षिप्त (बदली हुई ) हो जाती है ; परन्तु उनमें वर्णित पात्र और घटनाओं का अस्तित्व अवश्य होता है ।
किसी न किसी रूप में मनु के विषय में यूरेशिया की बहुत सी संस्कृतियाँ वर्णन करती हैं । ---------------------------------------------------------------
.🐋🐬🐳🐋🏊🏄🐟.....
पाश्चात्य पुरातत्व वेत्ता - डॉ० लियो नार्ड वूली ने पूर्ण प्रमाणित पद्धति से सिद्ध किया है ।
कि एशिया माइनर के पार्श्ववर्ती स्थलों का जब उत्खनन करवाया , तब ज्ञात हुआ कि जल -प्रलय की विश्व -प्रसिद्ध घटना सुमेरिया और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में हुई थी।
सुमेरियन जल - प्रलय के नायक सातवें मनु वैवस्वत् थे जल प्रलय के समय मत्स्य अवतार विष्णु रूप में भगवान् ने इसी मनु की रक्षा की थी ...इस घटना का एशिया-माइनर की असीरी संस्कृति (असुरों की संस्कृति ) की पुरा कथाओं में उल्लेख है कि मनु ही जल- प्रलय के नायक थे ।
विष्णु और मनु के आख्यान सुमेरियन संस्कृति से उद्धृत किए भारत में आगत देव संस्कृति से अनुयायीयों ने 👇
"विष्णु देवता का जन्म सुमेरियन
पुरातन कथाओं में"
82 INDO-SUMERIAN SEALS DECIPHERED
-------------------------------------------------------------------
sentation on ancient Sumerian and Hitto-Phoenician sacred seals and on Ancient Briton monuments,
see our former work,
1 of which the results therein announced are now con- firmed and established by the evidence of these Indo- Sumerian seals.
________________________________________
This Sumerian " Fish " title for the Sun-god on this and the other amulet seals, as " Fish of the Setting Sun (S'u- kha) " is of the utmost critical importance for establishing the Sumerian origin of the Indo-Aryans..
and the Aryan character of the Sumerian language,
as it discloses for the first time the origin and hither to unknown real meaning of the Vedic name for the Sun-god " Vishnu," and of his represen-tative as a Fish-man, as well as the Sumerian origin of the English word " Fish," the Gothic " Fisk " and Latin " Piscis."
The first " incarnation " of the Sun-god Vishnu in Indian mythology is represented as a Fish-man (see Fig. 19)
and in substantially the same form as the Sumerian Fish-man personification of the Sun-god of the Waters in the Sumerian seals.
Now the Sumerians of Mesopotamia called the Setting Sun " The Fish (KM) "
2- a fact which has not hitherto been remarked or recognized.
And this Sumerian title of " Fish " for the Sun is explained in the bilingual
Sumero-Akkadian glossaries by the actual word occurring in this and the other Indo-Sumerian amulets,
namely S'u-khd, with the addition of " man = (na),
_________________________________________
3 by word-signs which read literally " The Winged Fish-man " ; * thus co-relating the Winged or soaring Sun with the Fish personification of the supposed " returning or resurrecting " Sun in " the waters under the earth."
This solar title of "
The Winged Fish " is further given the synonym of "The turning Bii-i-es's which latter name 1 W.P.O.B., 247 f., 251, 308. 2 B.. 8638. 3 lb., and 1586. 4 S'u=" wing," B.W., 311. 5 Gar-bi-i-i-es' (B., 7244) ; gar=" turn " (B., 11984) ; es' (B., 2551).
SUMER ORIGIN OF VISHNU IN NAME AND FORM 83
is evidently a variant spelling of the Sumerian Pi-es' or Pish for " Great Fish " with the pictograph word-sign of Fig, 19. — Sumerian Sun-Fish as Indian Sun-god Vishnu. From an eighteen th-centuiy Indian image (after Moor's Hindoo Pantheon).
Note the Sun-Cross pendant on his necklace. He is given four arms to carry his emblems : la) Disc of the Fiery Wheel {weapon) of the Sun, (M Club or Stone-mace (Gada or Kaumo-daki)
1 of the Sky-god Vanma, (c) Conch-shell (S'ank-ha), trumpet of the Sea-Serpent demon, 1 (d) Lotus (Pad ma) as Sun- flower.* i. Significantly this word " Kaumo-daki " seems to be the Sumerian Qum, " to kill or crush to pieces " (B., 4173 ; B.W.. 193) and Dak or Daggu " a cut stone " (B., 5221, 5233). a. " Protector of the S'ankha (or Conch) " is the title of the first and greatest Sea- Serpent king in Buddhist myth, see my List of Naga (or Sea-Serpent) Kings in Jour. Roy. Asiat. Soc, Jan, 1894. 3. On the Lotus as symbol of heavenly birth, see my W.B.T., 338, 381, 388.
________________________________________
84 INDO-SUMERIAN SEALS DECIPHERED Fish joined to sign " great." 1 This now discloses the Sumerian origin not only of the " Vish " in Vish-nu, but also of the English '* Fish," Latin " Piscis," etc.— the labials B, P, F and V being freely interchangeable in the Aryan family of languages.
The affix nu in " Vish-nu " is obviously the Sumerian Nu title of the aqueous form of the Sun-god S'amas and of his father-god la or In-duru इन्द्र: (Indra) as " God of the Deep." ' It literally defines them as " The lying down, reclining or bedded " (god)
3 or " drawer or pourer out of water." ' It thus explains the common Indian representation of Vishnu as reclining upon the Serpent of the Deep amidst the Waters, and also seems to disclose the Sumerian origin of the Ancient Egyptian name Nu for the " God of the Deep."
5 Thus the name
" Vish-nu " is seen to be the equivalent of the Sumerian Pisk-nu,(पिस्क- नु ) and to mean "Pisk-nu,(पिस्क- नु ) and to mean " The reclining Great Fish (-god) of the Waters " ; and it will doubtless be found in that full form in Sumerian when searched for. And it would seem that this early " Fish " epithet of Vishnu for his " first incarnation " continued to be applied by the Indian Brahmans to that Sun-god even in his later "
incarnations " as the "striding" Sun-god in the heavens.
____________________________________
Indeed the Sumerian root Pish or Pis for " Great Fish " still survives in Sanskrit as Fts-ara विसार: " fish." " This name thus affords another of the many instances which I 1 On sign T.D., 139; B.W., 303. The sign is called " Increased Fish " {Kua-gunu, i.e., Khd-ganu, B., 6925), in which significantly the Sumerian grammatical term gunu meaning " increased " as applied to combined signs, is radically identical with the Sanskrit grammatical term gut.a ( = " multi- plied or auxiliary," M.W.D., 357) which is applied to the increased elements in bases forming diphthongs, and thus disclosing also the identity of Sanskrit and Sumerian grammatical terminology.
* M., 6741, 6759 ; B., 8988. s B., 8990-1, 8997. 4 lb., 8993. 5 This Nu is probably a contraction for Nun, or " Great Fish," a title of the god la (or Induru) इन्द्ररु of the Deep (B., 2627). Its Akkad synonym of Naku, as "drawer or pourer out of Water," appears cognate with the Anu(n)-«aAi, or " Spirits of the Deep," and with the Sanskrit Ndga or " Sea-Serpent." • M.W.D., 1000. The affix ara is presumably the Sanskrit affix ra, added to roots to form substantives, just as in Sumerian the affix ra is similarly added (cp., L.S.G., 81).
____________________________________
SUMER ORIGIN OF POSEIDON
85 have found of the Sumerian origin of Aryan words, and in particular in the Sanskrit and English.
This Fish-man form of the Sumerian Sun-god of the Waters of the Deep,
Piesh, Pish or Pis (or Vish-nu),
also appears to disclose the unknown origin of the name of the Greek Sea-god "
____________________________________
संख्या 82 वीं इण्डो-सुमेरियन निद्रा (सील )में प्राचीन सुमेरियन और हिट्टो फॉनिशियन पवित्र मुद्राओं पर( और प्राचीन ब्रिटान स्मारकों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।
जिनमें से मौहर संख्या (1) में से परिणाम घोषित किए गए हैं ।
अब इन इंडो-सुमेरियन सीलों के प्रमाण के आधार पर पुष्टि की गई है कि इस सुमेरियन "मछली देव" पर सूर्य-देवता का आरोपण है।
और अन्य ताबीज मुद्राओं के लिए शीर्षक, "स्थापित सूर्य (सु-ख़ाह) की मछली" के रूप में इंडो-आर्यों की सुमेरियन मूल की स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साम्य है ।
और सुमेरियन भाषा के आर्यन चरित्र के रूप में, यह सूर्य-देवता "विष्णु" के लिए वैदिक नाम की उत्पत्ति और अब तक अज्ञात मछली अर्थ के रूप में प्रकट करता है और मत्स्य -मानव के रूप में उनकी प्रतिनिधि के समान साथ ही अंग्रेजी शब्द "फिश" के सुमेरियन मूल, गॉथिक "फिसक" और लैटिन "पिसिस पर भी प्रकाश डालता है ।
____________________________________
भारतीय पौराणिक कथाओं में सूर्य-देव विष्णु का पहला "अवतार" मत्स्य -नर के रूप में दर्शाया गया है।
, और अत्यधिक सीमा तक उसी तरह के रूप में जैसे सुमेरियन मछली-नर के रूप में सूर्य का देवता के रूप में चित्रण सुमेरियन मुद्राओं पर (अब मेसोपोटामिया )के सुमेरियन मुद्राओं पर उत्कीर्ण है।
और सूर्य के लिए "मछली" के इस सुमेरियन शीर्षक को द्विभाषी सुमेरो-अक्कादियन शब्दावलियों में वास्तविक शब्द और अर्थ इस प्रकार के अन्य इंडो-सुमेरियन ताबीज पर व्याख्यायित है ।
"मत्स्य मानव ।
____________________________________
पिस्क-नु" शब्द को पंखधारी मछली-मानव " आदि अर्थों के रूप पढ़ते हैं। इस प्रकार पंखों या बढ़ते सूर्य को "पृथ्वी के नीचे के पानी में" लौटने या पुनर्जीवित करने वाले सूर्य के मछली के संलयन के साथ सह-संबंधित कथाओं का सृजन सुमेरियन संस्कृति में होगया था ।
--जो कालान्तरण में भारतीय पुराणों में मिथक रूप में अभिव्यक्त हुई ।
"द विंगेड फिश" के इस सौर शीर्षक को "biis"को फिश" का समानार्थ दिया गया है।
____________________________________
सूर्य और विष्णु भारतीय मिथकों में समानार्थक अथवा पर्याय वाची रहे हैं।
"विष्-नु " में प्रत्यय "नु" स्पष्ट रूप से सूर्य-देवता के जलीय रूप और उनके पिता-देवता इन-दुरु (इन्द्र) के "देवता के रूप में सुमेरियन आदम का शीर्षक है।
यह इस प्रकार विष्णु के सामान्य भारतीय प्रतिनिधित्व को जल के बीच दीप के नाग पर पुन: और यह भी लगता है कि "दीप के देवता" के लिए प्राचीन मिस्र के नाम आतम के सुमेरियन मूल का खुलासा किया गया है।
इस प्रकार "विष्णु" नाम सुमेरियन "पिस्क-नु "के बराबर माना जाता है।
और " जल की बड़ी फिश (-गोड) को करना; और और यह निश्चित रूप से सुमेरियन में उस पूर्ण रूप में पाए जाने पर खोजा जाएगा।
और ऐसा प्रतीत होता है कि "अवतार" के लिए विष्णु के इस बड़ी "मछली" का उपदेश भारतीय ब्राह्मणों ने अपने बाद के "अवतारों" में भी विष्णु-देवता को स्वर्ग में सूर्य-देवता के रूप में लागू किया है।वास्तव में "महान मछली" के लिए सुमेरियन मूल पीश या पीस शब्द अभी भी संस्कृत में एफ्स-ऐरा "मछली" के रूप में जीवित है।जो वैदिक मत्स्यवाची शब्द "विसार" से साम्य है "यह नाम इस प्रकार कई उदाहरणों में से एक है जिसे मैं दीप, पीश, पीश या पीस (या वाश-नु) के जल के सुमेरियन सूर्य-देवता का यह नाम है ।
मिश्रु "MISHARU" - The Sumerian god of law and justice, brother of Kittu.
भारतीय पुराणों में मधु और कैटव का वध विष्णु-देवता करते है ।
मत्स्यः से लिए वैदिक सन्दर्भों में एक शब्द पिसार
भारोपीय मूल की धातु से प्रोटो-जर्मनिक में फिस्कज़(पुरानी सैक्सोन, पुरानी फ्रिसिज़, पुरानी उच्च जर्मन फ़िश, पुरानी नोर्स फिस्कर। मध्य डच विस्सी, डच, जर्मनी, फ़िश्च, गॉथिक फिसक का स्रोत) से पुरानी अंग्रेजी मछलियां "मछली"
pisk- "एक मछली।
*pisk-
Proto-Indo-European root meaning
"a fish."It forms all or part of: fish; fishnet; grampus; piscatory; Pisces; piscine; porpoise.It is the hypothetical source of/evidence for its existence is provided by:Latin piscis (source of Italian pesce)
French poisson, Spanish pez, Welsh pysgodyn, Breton pesk); Old Irish iasc; Old English fisc, Old Norse fiskr, Gothic fisks.
1-Latin piscis,
2-Irish íasc/iasc,
3-Gothic fisks,
4-Old Norse fiskr,
5-English fisc/fish,
6-German fisc/Fisch,
7-Russian пескарь (peskarʹ),
8-Polish piskorz,
9-Welsh pysgodyn,
10-Sankrit visar
11Albanian peshk
__________________________________________
This important reference is researched by Yadav Yogesh Kumar 'Rohi'. Thus, no gentleman should not add to its break!
भारतीय ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अपने इष्ट को वलि समर्पण हेतु मनुः ने असीरियन द्रविड पुरोहितों का आह्वान किया था "" असुरः ब्राह्मण इति आहूत " -------------------------------------------------------------
मानव संज्ञा का आधार प्रथम स्वायंभुव मनु थे ।
उधर नार्वे की पुरा कथाओं में मनु की प्रतिष्ठा मेनुस (Mannus )के रूप में है।
जे जर्मनिक जन-जातियाँ के आदिम रूप हैं।
पश्चिमीय एशिया की हिब्रू जन-जाति के धर्म ग्रन्थ ऑल्ड-टेक्सटामेण्ट(पुरानी बाइबिल ) जैनेसिस्(उत्पत्ति) खण्ड के पृष्ठ संख्या 82 पर वर्णित है ""👇
कि नूह (मनुः) ने ईश्वर के लिए एक वेदी बनायीऔर उसमें पशु पक्षीयों को लेकर यज्ञ- अग्नि में उनकी बलि दी इन्हीं कथाओं का वाचन ईसाई तथा इस्लामीय ग्रन्थों में किया गया है।
मनु के सन्दर्भ में ये कुछ प्रमाणिक तथ्य थे ••••••••
"श्रीकृष्णेतिहासम्"
महाबलिपुरम्-और कृष्ण-
- कन्नन का उल्लेख:प्राचीन तमिल साहित्य में कृष्ण को 'कन्नन' नाम से जाना जाता है, जो संस्कृत कृष्ण का ही प्राकृत रूप है।
- कहानियों का अस्तित्व:संगम ग्रंथों जैसे अगनानुरु में रास लीला का उल्लेख मिलता है, जो दर्शाता है कि कृष्ण से जुड़ी अंतरंग स्मृतियाँ यादवों द्वारा सँजोई गई थीं।
- वाहन और ध्वज:तमिल कवियों ने कृष्ण के वाहनों और ध्वजों का भी वर्णन किया है, जो धार्मिक और साहित्यिक ज्ञान के प्रति उनके झुकाव को दर्शाता है।
- शिलप्पादिकारम:इस महाकाव्य में कृष्ण के हल्लोन (बलराम) की प्रशंसा की गई है।
- आंडाल की भक्ति:तमिल की प्रसिद्ध वैष्णव कवयित्री आंडाल ने कृष्ण के वियोग में तिरुप्पावै और नाच्चिचार तिरूमोलि जैसे पद लिखे, जिनमें कृष्ण के प्रति उनकी गहन भक्ति और प्रेम व्यक्त किया गया है। वह कृष्ण को अपना पति मानती थीं और उनके साथ रासलीला की कल्पना करती थीं।
- कृष्ण के विभिन्न रूप:कृष्ण को ग्वाला, पालक और देव के रूप में चित्रित किया गया है, जोTamil भूमि के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
तमिल की सबसे प्राचीन कृति 'थोलकप्पियम' में स्वयं संस्कृत के शब्द हैं, तो फिर तमिल, संस्कृत से पुरानी भाषा कैसे हो सकती है?
तमिलज़ के पास 690 ईसा पूर्व से लिखित लिपि थी (सालुवांकुप्पम मुरुगन मंदिर के पत्थर पर तमिलज़ी शिलालेख) जबकि संस्कृत की 600 ईस्वी तक कोई लिपि नहीं थी। थोलकाप्पियम का समय 300 ईसा पूर्व है।
350 ईसा पूर्व से अधिक पुराने कीलझाडी बर्तनों के टुकड़ों में तमिलझी लिपि अंकित है।
आदिचनल्लूर (650 ईसा पूर्व), कोर्राई (500 ईसा पूर्व), पोरुन्थल (450 ईसा पूर्व), अझगनकुलम, कोडुमनाल (350 ईसा पूर्व) में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, एक ढलाईखाना और कुछ सोने के टुकड़े मिले थे और उनकी आयु कार्बन डेटिंग द्वारा निर्धारित की गई थी। उपरोक्त उत्खनन कीलझाड़ी साक्ष्यों से भी पुराने पाए गए हैं।
ओडिशा के राजगीर और दौलागिरी की चट्टानों में पाए गए अशोक के ब्राह्मी शिलालेख (प्रकृति) 262 से 232 ईसा पूर्व के हैं। मैंने 2014 और 2015 में इन जगहों का दौरा किया है। अशोक के शिलालेख में उल्लेख है कि दक्षिण के शासक - करिकाल चोलझान, पांड्य और चेर राजा - उनके समकालीन थे। इसमें यह भी उल्लेख है कि दक्षिण में एक अलग लिपि का प्रयोग होता था। तमिलज़ी में, शिलालेख आम लोगों के लिए कुम्हारों द्वारा बनाए गए थे, जबकि अशोक के शिलालेख शासकों के लिए शिक्षित लोगों द्वारा बनाए गए थे। यह उन दोनों क्षेत्रों में साक्षरता दर के स्तर को दर्शाता है।
तमिल भाषा में ऋषि अगस्त्य/अकथियार द्वारा रचित अकथियम था, जिसका उल्लेख तोल्काप्पियार ने अपने तोल्काप्पियम में किया है, जो 360 ईसा पूर्व से लेकर आज तक का पहला उपलब्ध लिखित तमिल व्याकरण है।
उस व्याकरण में, थोलकाप्पियार ने सोल अथिकाराम लिखा था, जहां उन्होंने शब्दों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था - ईयारचोल (प्राकृतिक थमिलज़ शब्द), वडासोल (संस्कृत, पाली, प्रकृति के शब्द), थिरिसोल (कविता और साहित्य में प्रयुक्त शब्द) और .थिसाई चोल (केंद्रीय थमिलज़खम के आसपास के 12 क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियाँ)। ).
उन्होंने तमिल भाषा में वडासोल लिखने के नियमों का उल्लेख किया था।
तिरुक्कुरल में (तिरुवल्लुवर द्वारा 34 ईसा पूर्व लिखा गया) 24 तमिल शब्द थे। तो थिरुक्कुरल में, जिसमें 14000 से अधिक शब्द हैं, 24 वडासोल हैं
बाद में 200 ई. तक तीसरे तमिल संगम ग्रंथों में हमें 45 वडासोल मिलते हैं।
बाद के ग्रंथों में 6वीं शताब्दी ई. तक 242 वडासोल और थिरिसोल थे।
13वीं शताब्दी के बाद वडसोल का प्रचलन और अधिक बढ़ने लगा। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में मणिप्रवलम नामक एक और शैली अस्तित्व में आई। इस प्रकार, वडसोल का प्रतिनिधित्व करने के लिए 16वीं शताब्दी में नए अक्षर - ஷ (श), ஸ (सा), ஹ (ह), க்ஷ (क्ष), और ஸ்ரீ (श्री) जोड़े गए।
1895 में, मराईमलाई आदिकल की पुत्री और एक तमिल शिक्षिका श्रीमती नीलाम्बिका /நீலாம்பிகை அம்மையார் ने तमिल में वडसोल की एक सूची संकलित की। इसे 1898 में शैव तमिलज़ पाथुकाप्पु कलझकम (कीमत 3 आना) द्वारा "वडसोल - तमिलज़ अकारथी" शीर्षक के तहत एक संग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसमें 25 पृष्ठ हैं - जिसमें प्रस्तावना और सामग्री के लिए पृष्ठ शामिल हैं। मैंने इसे 3 साल पहले (2020) पढ़ा था। इसमें 23 पृष्ठों में वडसोल है। इसमें प्रति पृष्ठ 2 कॉलम और प्रति कॉलम 40 शब्द हैं। इसलिए पृष्ठ 3 से 24 तक प्रति पृष्ठ 80 शब्द हैं। 25वें पृष्ठ (जो कि अंतिम पृष्ठ है) में बाएं कॉलम में 40 शब्द हैं, जबकि दाएं कॉलम में 33 शब्द हैं।
तो 44 कॉलम में तमिलज़ में वडासोल की कुल संख्या 1760 + 73 = 1833 शब्द हैं।
1896 में किए गए शोध के अनुसार तमिल भाषा में 3.8 लाख शब्द थे (12 शब्दकोश उपलब्ध हैं)।
इस प्रकार, 3.8 लाख तमिल शब्दों में से 1833 शब्दों (वडासोल) का प्रतिशत 0.5% से भी कम है। इसलिए, तमिल भाषा के 99.5% अपने मूल शब्द हैं।
भारत की सभी भाषाओं में से तमिल भाषा में वडासोल - अर्थात संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं से लिए गए शब्दों की संख्या सबसे कम है।
तमिल भाषा ने भी संस्कृत को कई शब्द दिए हैं, जो इस प्रश्न में शामिल नहीं हैं।
संपादन 1
तमिल भाषा स्वयं को पृथ्वी की सबसे प्राचीन भाषा होने का दावा नहीं करती।
हालाँकि, यह न केवल सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, बल्कि सबसे पुरानी जीवित शास्त्रीय भाषा भी है।
महाबलिपुरम् (Mahabalipuram) या मामल्लपुरम् (Mamallapuram) भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टु ज़िले में स्थित एक प्राचीन नगर (शहर) है।
यह मंदिरों का शहर राज्य की राजधानी, चेन्नई, से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी से तटस्थ है।
चेन्नई का पुराना नाम मद्रास (Madras) है, जिसे 1996 में तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर बदलकर चेन्नई कर दिया था।
यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर-तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सातवीं शताब्दी में यह शहर पल्लव( पाल ) राजाओं की राजधानी था।
द्रविड वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ पर पत्थरों को काट कर मन्दिर बनाया गया। पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित थे।
महाबलीपुरम का रथ मंदिर
यह स्थान सबसे विशाल नक्काशी के लिए लोकप्रिय है। यह 27 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है। इस व्हेल मछली के पीठ के आकार की विशाल शिलाखंड पर ईश्वर, मानव, पशुओं और पक्षियों की आकृतियां उकेरी गई हैं।
अर्जुन्स् पेनेन्स को मात्र महाबलिपुरम या तमिलनाडु की गौरव ही नहीं बल्कि देश का गौरव माना जाता है।
समुद्र-तट का मन्दिर (शोर टेम्पल)
महाबलिपुरम के तट मन्दिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में माना जाता है जिसका संबंध आठवीं शताब्दी से है।
यह मंदिर द्रविड वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यहां तीन मंदिर हैं। बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है जिसके दोनों तरफ से शिव मंदिर हैं। मंदिर से टकराती सागर की लहरें एक अनोखा दृश्य उपस्थित करती हैं। इसे महाबलीपुरम् का रथ मंदिर भी कहते है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था।
प्रांरभ में इस शहर को "मामल्लपुरम" कहा जाता था।
रथ-
महाबलिपुरम के लोकप्रिय रथ दक्षिणी सिर पर स्थित हैं। महाभारत के पांच पांडवों के नाम पर इन रथों को पांडव रथ कहा जाता है। पांच में से चार रथों को एकल चट्टान पर उकेरा गया है। द्रौपदी और अर्जुन रथ वर्ग के आकार का है जबकि भीम रथ रेखीय आकार में है। धर्मराज रथ सबसे ऊंचा है। इसमे दौपदी के पांच रथमंदिर हुए। क्योंकि उसके पांच पति थे। इस लिए उसके पांच रथमंदिर हुए।
कृष्ण मण्डपम्-
यह मंदिर महाबलिपुरम के प्रारंभिक पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिरों में एक है। मंदिर की दीवारों पर ग्रामीण जीवन की झलक देखी जा सकती है। एक चित्र में भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाए तथा बाँसुरी बजाते हुए दिखाया गया है।
गुफाएँ-
वराह गुफा विष्णु के वराह और वामन अवतार के लिए प्रसिद्ध है। साथ की पल्लव के चार मननशील द्वारपालों के पैनल लिए भी वराह गुफा चर्चित है। सातवीं शताब्दी की महिसासुर मर्दिनी गुफा भी पैनल पर नक्काशियों के लिए खासी लोकप्रिय है।
मूर्ति संग्रहालय-
राजा स्ट्रीट के पूर्व में स्थित इस संग्रहालय में स्थानीय कलाकारों की 3000 से अधिक मूर्तियां देखी जा सकती हैं। संग्रहालय में रखी मूर्तियां पीतल, रोड़ी, लकड़ी और सीमेन्ट की बनी हैं।
मुट्टुकाडु-
यह स्थान महाबलिपुरम् से 21 किलोमीटर की दूरी पर है जो वाटर स्पोट्र्स के लिए लोकप्रिय है। यहां नौकायन, केनोइंग, कायकिंग और विंडसर्फिग जसी जलक्रीड़ाओं का आनंद लिया जा सकता है।
कोवलोंग-
महाबलिपुरम से 19 किलोमीटर दूर कोवलोंग का खूबसूरत बीच रिजॉर्ट स्थित है। इस शांत फिशिंग विलेज में एक किले के अवशेष देखे जा सकते हैं। यहां तैराकी, विंडसफिइर्ग और वाटर स्पोट्र्स की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं।
महाबलिपुरम् नृत्य पर्व-
यह नृत्य पर्व सामान्यत: जनवरी या फरवरी माह में मनाया जाता है। भारत के जाने माने नृत्यकार शोर मंदिर के निकट अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। पर्व में बजने वाले वाद्ययंत्रों का संगीत और समुद्र की लहरों का प्राकृतिक संगीत की एक अनोखी आभा यहां देखने को मिलती है।
- वायु मार्ग-
महाबलिपुरम से 60 किलोमीटर दूर स्थित चैन्नई निकटतम एयरपोर्ट है।
भारत के सभी प्रमुख शहरों से चैन्नई (मदुरई) के लिए फ्लाइट्स हैं।
- रेल मार्ग
चेन्गलपट्टू महाबलिपुरम का निकटतम रेलवे स्टेशन है जो 29 किलोमीटर की दूरी पर है। चैन्नई और दक्षिण भारत के अनेक शहरों से यहां के लिए रेलगाड़ियों की व्यवस्था है।
- सड़क मार्ग
महाबलिपुरम तमिलनाडु के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा है। राज्य परिवहन निगम की नियमित बसें अनेक शहरों से महाबलिपुरम के लिए जाती हैं।
यह कविता संगम साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है। हालाँकि यह उस तरह की संगम कविता है जो मुझे बहुत सारी तुलनाओं और छिपे अर्थों के साथ पसंद है, लेकिन यह कविता मुझे विशेष रूप से किसी अन्य कारण से रुचिकर लगती है। इस कविता में कृष्ण मिथकों और मुरुगन की कृति थिरुपरनकुंड्रम के दिलचस्प संदर्भ हैं।
आपकी भुजाओं को
सूजे हुए बांस की तरह पतला छोड़कर ,
थलाइवन ने हमें दूर देश में धन संचय करने का महान कार्य
करने के लिए छोड़ दिया है।
सुदूर देश की अपनी यात्रा में
, (उसने देखा)
नर हाथी झुक जाता था और
ऊँचे या पेड़ को तोड़ देता था,
ताकि युवा मादा हाथी कोमल टहनियों को
खा सके , जैसे, "माल जिसने उस पर चलकर पेड़ों को रौंद दिया , ताकि चरवाहे समुदाय की स्नान करने वाली महिलाओं को , पानी से भरी उत्तर की तोलुनाई (यमुना) नदी के विस्तृत फैले हुए रेत के तटों पर ठंडी पत्तियों को पहनने की अनुमति दें ” और वासना से सराबोर गालों पर बसने वाली मधुमक्खियों को भगाएं । (यह देखकर थलाइवन वापस आ जाएंगे).
कवि: मदुरै मारुतन इलानाकन
Translated by me based on Swaminathan Iyer’s and Dr.Kamil Zvelebil’s commentry.
थलाइवन अब दौलत कमाने के लिए थलाइवी छोड़ चुके हैं. इसकी वजह से थलाइवी का हाथ बांस के आकार का पतला होता जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह ठीक से खाना नहीं खा रही है और अपने प्रेमी से अलग होने के कारण बीमार भी है।

इन पंक्तियों का महत्व:
हथिनी ने मादा हाथी के लिए ऊंचे पेड़ों को झुका दिया - थलाइवन ने धन कमाने के लिए थलाइवी छोड़ दी।
वासना से सराबोर गालों पर मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं - थलाइवी प्रेम रोग और प्रेमी से अलगाव से पीड़ित है।
नर हाथी के पीछा करने के कृत्य से थलाइवन को एहसास होगा कि उसे अपने प्रेमी से प्यार की बीमारी को दूर करना होगा और थलाइवी को देखने के लिए वापस लौटना होगा।
मल/कृष्ण अयार लड़कियों के कपड़े छीन रहे हैं - थलाइवन धन की तलाश में थलाइवी की शांति को अपने साथ ले जा रहा है।
अयार लड़कियाँ शर्म की स्थिति में होती हैं जब बलरामन आता है - थलाइवी अलगाव के कारण प्यार से बीमार हो जाती है।
इससे पहले कि लड़कियों पर कोई शर्मिंदगी आ जाए, कृष्णा उन्हें बचा रहे हैं - थलाइवी को उम्मीद है कि थलाइवन वापस आएगा और उसे प्यार की बीमारी से बचाएगा।
Thiruparankundram
यह कविता थिरुपरनकुंद्रम को मुरुगन के शुरुआती पवित्र स्थलों में से एक के रूप में भी प्रमाणित करती है (संगम में उल्लिखित दूसरा स्थान सेंथी-थिरुसेन्थुर है। कोपियस चंदन के पेड़ों के साथ ऊंचे पर्वत (नेटुवराई) का उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में अनुतुवन ने गाया था, जिसे 'कूल' परनकुंरम कहा जाता है। और जो "बड़े गुस्से वाले मुरुकन का निवास स्थान है, जिसके पास चमकीले पत्ते जैसे लंबे भाले थे, जिसने करन के शरीर को दो टुकड़ों में काट दिया था"।
नल्लंतुवनार
अनुतुवन एक साथी कवि नल्लंतुवनार (250-400 ईस्वी के बीच किसी भी समय) थे, जिन्होंने परिपादल कविता 8 में थिरुपरनकुंड्रम के बारे में गाया था (गीत में थिरुपरनकुंड्रम का विस्तृत वर्णन है - मैंने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है!)। उन्हें संगम युग के उत्तरार्ध के प्रतिभाशाली कवियों में से एक माना जाता है। वह अकाम 43, नरिनाई 88, पारिपातल 6, कलिथोकाई 118-150 के लेखक हैं और शायद कलिथोकाई संकलन के संकलनकर्ता भी रहे हैं। कवि यहाँ सम्मान करते हैं उन्होंने अपनी कविता में थिरपरनकुंड्रम कहा, जिसे अनुतुवन ने गाया था।
यमुना में कृष्ण और गोपिकाओं का सबसे पहला उल्लेख ???
निम्नलिखित पंक्तियों का अनुवाद डॉ. कामिल ज़्वेलेबिल द्वारा किया गया है।
नर हाथी अपनी मादा के खाने के लिए कोमल टहनियों को नष्ट कर देता है, उसकी तुलना "माल" से की जाती है, जो कपड़े पहनने के लिए पेड़ों की शाखाओं (यानी कुरुंतमारम, कन्नन द्वारा काटा गया जंगली चूना) पर चलते हुए रौंदता (चलता, कूदता, मिटिट्टु) बनाता है। पानी से भरी तोलुनाई नदी के दूर-दूर तक फैले रेत वाले चौड़े घाट के [किनारों पर] ग्वालों (अंतर) समुदाय की युवा महिलाओं (मकलिर) को ठंडक मिलती है।
और डॉ. ज़्वेलेबिल के अनुसार, किंवदंती का यह संस्करण किसी भी संस्कृत स्रोत को ज्ञात नहीं है। सबसे पहला संस्कृत स्रोत या तो भागवतपुराण या विष्णुपुराण प्रतीत होता है। इसलिए ऐसा लगता है कि मटुरै मरुतानिलनकन की यह अकाम 59 कविता भारत में कृष्ण की आकृति और यमुना नदी के तट पर चरवाहों का उल्लेख करने वाली सबसे पुरानी कविता प्रतीत होती है।



यमुना में कृष्ण, बलराम और ग्वाल-बालों की पूरी आकृति का उल्लेख चिंतामणि 209 में निम्नलिखित श्लोक में किया गया है ( ற்றுட்
போனிற வளையி னார்க்குக் குருந்தவ னொசித "
यह एक अच्छा विचार है ।”
इस कविता पर प्रोफेसर जॉर्ज एल. हार्ट की राय नीचे दी गई है (अकाम 59)
अकाम 59 में वर्णन किया गया है कि "एक हाथी जो ऊंचे पेड़ों को झुकाता है ताकि उसका साथी खा सके, जैसे कृष्ण [मल}, जो उन पर पैर रखकर [शाखाओं] को नीचे झुकाता है [मिटि-चढ़ने के बाद?] ताकि चौड़ी रेतीली रेत पर चरवाहे लड़कियाँ तोलुनाई[यमुना] के तट पर उत्तर अच्छे कपड़े बना सकता है और पहन सकता है।” यह भारतीय साहित्य में कृष्ण और गोपियों की कहानी के सबसे शुरुआती संदर्भों में से एक है; यह हरिवंश के समकालीन या उससे थोड़ा बाद का होना चाहिए। किसी भी घटना में, इतनी प्रारंभिक तिथि में तमिल में इसकी उपस्थिति इंगित करती है कि यह भारत के कई हिस्सों में पहले से ही अच्छी तरह से जाना जाता होगा। नायक द्वारा अपनी प्रेमिका को पोशाक (तलाई) बनाने के लिए पत्ते भेंट करने का विषय तमिल की एक विशेषता है। भगवान कृष्ण और रोवर यमुना दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नाम तमिल शब्द हैं; मल, "काला वाला"; टोलुनाई, संभवतः टोलू मूल से, "पूजा करना", उत्तर भारत में किसी स्थान के लिए शुद्ध तमिल नाम का सर्वेक्षण की गई कविताओं में एकमात्र उदाहरण है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, शुरुआत से ही, तमिलों ने उत्तर भारत के देवताओं और पौराणिक शख्सियतों पर अपनी काव्य परंपराएं लागू कीं और सबसे पहले उन्होंने नए देवताओं की भूमिकाओं पर जोर दिया, जो उनके लिए केंद्रीय और सबसे डराने वाला कार्य था। जीवन, पुरुष और महिलाओं के बीच प्यार ”।










कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें